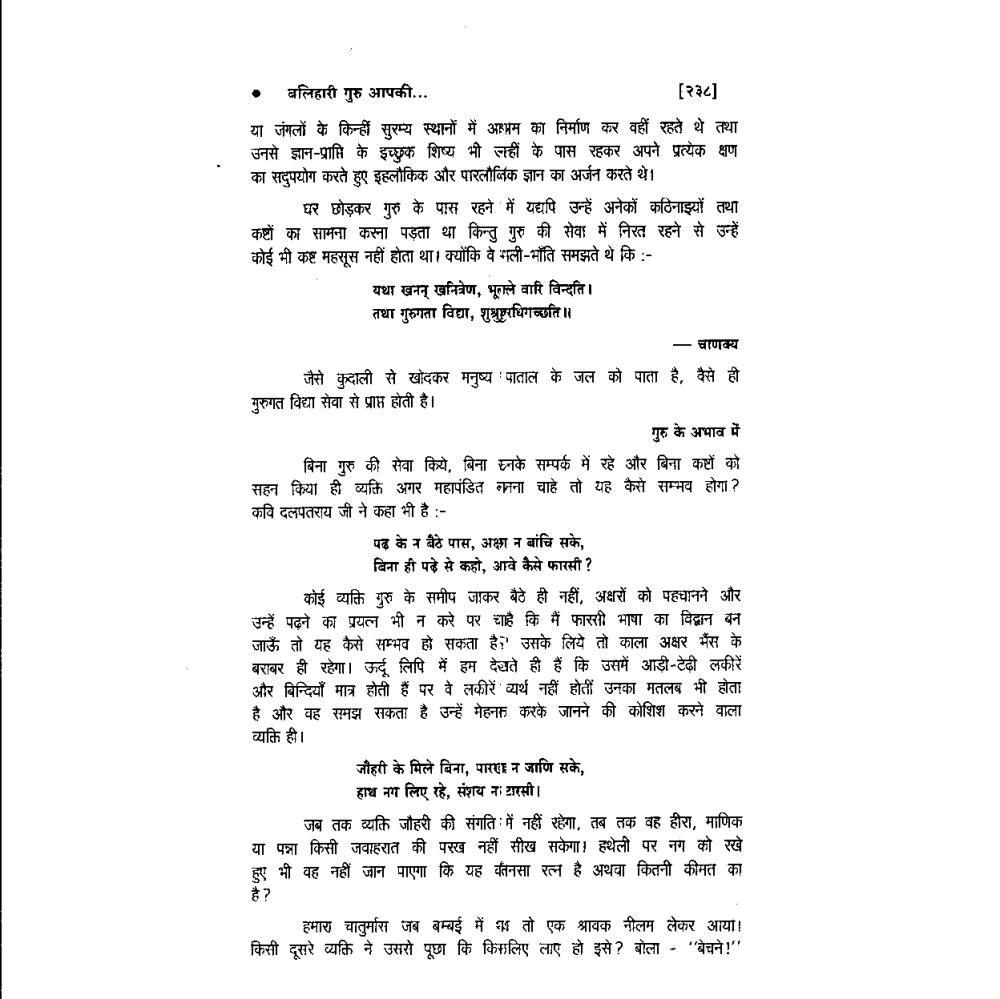________________
• बलिहारी गुरु आपकी....
[२३८]
या जंगलों के किन्हीं सुरम्य स्थानों में आश्रम का निर्माण कर वहीं रहते थे तथा उनसे ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक शिष्य भी नहीं के पास रहकर अपने प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करते हुए इहलौकिक और पारलौलिक ज्ञान का अर्जन करते थे।
घर छोड़कर गुरु के पास रहने में यद्यपि उन्हें अनेकों कठिनाइयों तथा कष्टों का सामना करना पड़ता था किन्तु गुरु की सेवा में निरत रहने से उन्हें कोई भी कष्ट महसूस नहीं होता था। क्योंकि वे गली-भाँति समझते थे कि :
यथा खनन् खनित्रेण भूलले वारि विन्दति । तथा गुरुगता विद्या, शुश्रुष्ठुरधिगच्छति ॥
चाणक्य
जैसे कुदाली से खोदकर मनुष्य पाताल के जल को पाता है, वैसे ही गुरुगत विद्या सेवा से प्राप्त होती है।
बिना गुरु की सेवा किये बिना उनके सम्पर्क में रहे सहन किया ही व्यक्ति अगर महापंडित बनना चाहे तो यह कवि दलपतराय जी ने कहा भी है:
पढ़ के न बैठे पास, अक्षा न बांचि सके, बिना ही पढ़े से कहो, आवे कैसे फारसी ?
गुरु के अभाव में
और बिना कष्टों को कैसे सम्भव होगा ?
कोई व्यक्ति गुरु के समीप
जाकर बैठे ही नहीं, अक्षरों को पहचानने और उन्हें पढ़ने का प्रयत्न भी न करे पर चाहै कि मैं फारसी भाषा का विद्वान बन जाऊँ तो यह कैसे सम्भव हो सकता है उसके लिये तो काला अक्षर भैंस के बराबर ही रहेगा। ऊर्दू लिपि में हम देखते ही हैं कि उसमें आड़ी-टेढ़ी लकीरें और बिन्दियाँ मात्र होती हैं पर वे लकीरें व्यर्थ नहीं होतीं उनका मतलब भी होता है और वह समझ सकता है उन्हें मेहनक करके जानने की कोशिश करने वाला व्यक्ति ही ।
जौहरी के मिले बिना, पारा न जाणि सके, हाथ नग लिए रहे, संशय न टारसी।
जब तक व्यक्ति जौहरी की संगति में नहीं रहेगा, तब तक वह हीरा, माणिक
या पन्ना किसी जवाहरात की परख नहीं सीख सकेगा। हथेली पर नग को रखे
हुए भी वह नहीं जान पाएगा कि यह वर्तनसा रत्न है अथवा कितनी कीमत का
है ?
हमारा चातुर्मास जब बम्बई में शव तो एक श्रावक नीलम लेकर आया । किसी दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा कि किसलिए लाए हो इसे ? बोला - "बेचने !"