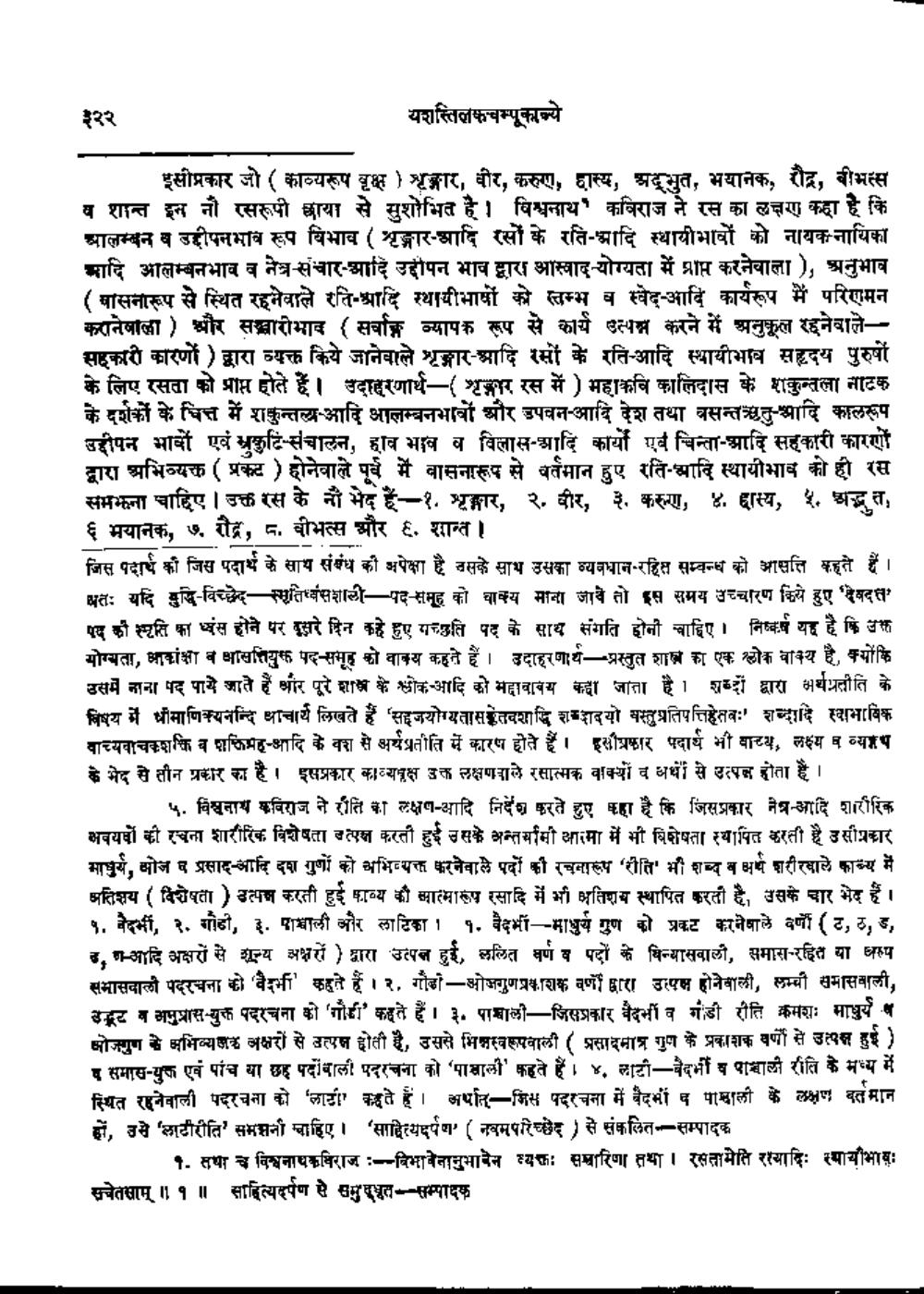________________
३२२
यशस्तिलफचम्पूकान्ये
इसीप्रकार जो ( काव्यरूप वृक्ष ) शृङ्गार, वीर, करुण, हास्य, अद्भुत, भयानक, रौद्र, वीभत्स व शान्त इन नौ रसरूपी छाया से सुशोभित है। विश्वनाथ' कविराज ने रस का लक्षण कहा है कि आलम्बन व उद्दीपनभाव रूप विभाव (शृङ्गार-श्रादि रसों के रति-श्रादि स्थायीभावों को नायक नायिका मादि आलम्बनभाव व नेत्र संचार-आदि उद्दीपन भाव द्वारा आस्वाद-योग्यता में प्राप्त करनेवाला), अनुभाव (पासनारूप से स्थित रहनेवाले रति-आदि स्थायीभाषों को स्तम्भ व स्वेद-आदि कार्यरूप में परिणमन करानेवाला) और सवारीभाव { सर्वात व्यापक रूप से कार्य उत्पन्न करने में अनुकूल रहनेवालेसहकारी कारणों ) द्वारा व्यक्त किये जानेवाले शृङ्गार-आदि रसों के रति-आदि स्थायीभाव सहृदय पुरुषों के लिए रसता को प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ-( शृङ्गार रस में ) महाकवि कालिदास के शकुन्तला नाटक के दर्शकों के चित्त में शकुन्तला-आदि आलम्बनभावों और उपवन-आदि देश तथा बसन्तऋतु-आदि कालरूप उद्दीपन भावों एवं भ्रुकुटि संचालन, हाव भाव व विलास-आदि कार्यों एवं चिन्ता-आदि सहकारी कारणों द्वारा अभिव्यक्त (प्रकट) होनेवाले पूर्व में वासनारूप से वर्तमान हुए रति-श्रादि स्थायीभाव को ही रस समझना चाहिए । उक्त रस के नौ भेद है-१. शृङ्गार, २. वीर, ३. करुण, ४. हास्य, ५. अद्भुत, ६ भयानक, ५. रौद्र, ८. बीभत्स और ६. शान्त। जिस पदार्थ को जिस पदार्थ के साथ संबंध की अपेक्षा है उसके साथ उसका व्यवधान-रहित सम्बन्ध को आसत्ति कहते हैं। षतः यदि बुद्धि-विच्छेद-स्मृतिध्वंसशाली-पद-समूह को वाक्य माना जाये तो इस समय उच्चारण किये हुए 'देवदत्त' पद की स्मृति का ध्वंस होने पर दूसरे दिन कहे हुए गच्छति पद के साथ संगति होनी चाहिए। निष्कर्ष यह है कि उस योग्यता, आकांक्षा व भासतियुक्त पद-समह को वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ-प्रस्तत शास्त्र का एक श्लोक वाक्य है. क्योंकि उसमें नाना पद पाये जाते हैं और पूरे शास्त्र के श्लोक-आदि को महावाक्य कहा जाता है। शब्दों द्वारा अर्थप्रतीति के विषय में धीमाणिक्यनन्दि आचार्य लिखते हैं 'सहजयोग्यतासचेतवशादि शम्दादयो यस्तुप्रतिपत्तिहेतवः' शब्दादि स्वाभाविक वाच्यवाचकशक्ति व शख्मिह-आदि के वश से अर्थप्रतीति में कारण होते हैं। इसौत्रकार पदार्थ भी वाच्य, लक्ष्य छ व्याप के भेद से तीन प्रकार का है। इसप्रकार काव्यक्ष उक्त लक्षणाले रसात्मक वाक्यों व अधों से उत्पन होता है ।
५. विश्वनाथ कविराज ने रीति का लक्षण-आदि निर्देश करते हुए कहा है कि जिस प्रकार नेत्र-आदि शारीरिक भवयों की रचना शारीरिक विशेषता उत्पन्न करती हुई उसके अन्तर्यामी आत्मा में भी विशेषता स्थापित करती है उसीप्रकार माधुर्य, मोज प प्रसाद-आदि दश गुणों को अभिव्यक्त करनेवाले पदों की रचनारूप 'रीति' भी शब्द व अर्थ शारीरथाले काव्य में अतिशय ( विशेषता) उत्पन्न करती हुई काव्य को स्मात्मारूप रसादि में भी अतिशय स्थापित करती है, उसके चार भेद है। ९. वैदी, २. गोडी, ३. पाश्वाली और लाटिका । १. वैदी-माधुर्य गुण को प्रकट करनेवाले वर्णी ( ट, ठ, ड, ड, आदि अक्षरों से शून्य अक्षरों) द्वारा उत्पन्न हुई, ललित वर्ण व पदों के विन्यासवाली, समास-रहित या वरुप सभासदाली पदरचना को 'वैदर्भी' कहते है। २, गोडी-ओजगुणप्रकाशक व Eru उत्पम होनेवाली. लम्बी समासवाली, उद्भट व अनुप्रास-युक्त पदरचना को 'गौडी' कहते हैं। ३. पाश्चाली—जिसप्रकार वैदी व गंडी रीति क्रमशः माधुर्य व मोगुण के अभिव्यजक अक्षरों से उत्पन्न होती है, उससे भिन्नस्वरूपवाली ( प्रसादमात्र गुण के प्रकाशक वर्गों से उत्पन्न हुई) व समास-युक्त एवं पांच या छह पदोबाली पदरचना को 'पावाली' कहते हैं। ४. लाटी-बैदी व पाश्चाली रीति के मध्य में स्थित रहनेवाली पदरचना को 'लाटी' कहते हैं। अर्थात्-मिस पदरचना में वैदी व पाचाली के लक्षण वर्तमान हों, उसे 'लाटीरीति' समझनी चाहिए। 'साहित्यदर्पण ( नवमपरिच्छेद ) से संकलित--सम्पादक
१. सथा व विश्वनाथकविराज :-बिभावेनानुभावेन व्यक्तः सम्बारिणा तथा । रसत्तामेति रस्यादिः स्मायोभायः स्चेतसाम् ॥ १ ॥ साहित्यदर्पण से समुभूत--सम्पादक