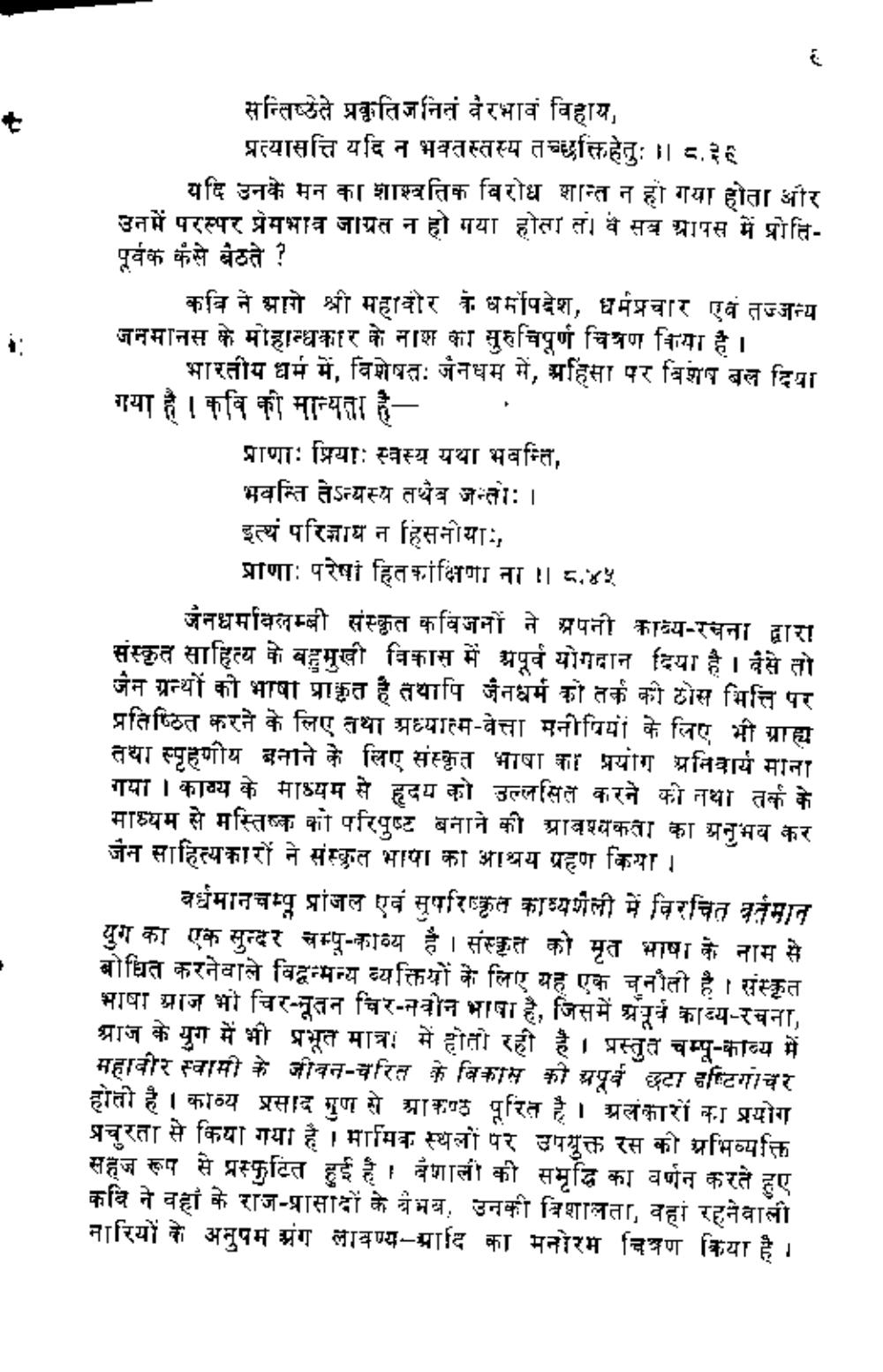________________
सन्तिष्ठेते प्रकृतिजनितं वैरभावं विहाय,
प्रत्यासत्ति यदि न भवतस्तस्य तच्छक्तिहेतुः ।। ८.३६ यदि उनके मन का शाश्वतिक विरोध शान्त न हो गया होता और उनमें परस्पर प्रेमभाव जाग्रत न हो मया होता तो वे सब पापस में प्रोतिपूर्वक कसे बैठते ?
कवि ने भागे श्री महावीर के धर्मोपदेश, धर्मप्रचार एवं तज्जन्य जनमानस के मोहान्धकार के नाश का सुरुचिपूर्ण चित्रण किया है।
भारतीय धर्म में, विशेषतः जनधम में, अहिंसा पर विशेष बल दिया गया है ! कवि की मान्यता है
प्राणाः प्रियाः स्वस्य यथा भवन्ति, भवन्ति तेऽन्यस्य तथैव जन्तोः । इत्थं परिज्ञाय न हिसनीयाः,
प्राणाः परेषां हितकांक्षिणा ना ।। ८.४५ जैनधर्मावलम्बी संस्कृत कविजनों ने अपनी काव्य-रचना द्वारा संस्कृत साहित्य के बहुमुखी विकास में अपूर्व योगदान दिया है । वैसे तो जैन ग्रन्थों की भाषा प्राकृत है तथापि जैनधर्म को तर्क की ठोस भित्ति पर प्रतिष्ठित करने के लिए तथा अध्यात्म-वेत्ता मनीषियों के लिए भी ग्राह्य तथा स्पृहणीय बनाने के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग अनिवार्य माना गया। काव्य के माध्यम से हृदय को उल्लसिल करने की नथा तर्क के माध्यम से मस्तिष्क को परिपुष्ट बनाने की अावश्यकता का अनुभव कर जैन साहित्यकारों ने संस्कृत भाषा का आश्रय ग्रहण किया।
वर्धमानचम्पु प्रांजल एवं सुपरिष्कृत काभ्यशैली में विरचित वर्तमान युग का एक सुन्दर चम्पु-काव्य है । संस्कृत को मृत भाषा के नाम से बोधित करनेवाले विद्वन्मन्य व्यक्तियों के लिए यह एक चुनौती है। संस्कृत भाषा आज भी चिर-नूतन चिर-नवीन भाषा है, जिसमें अपूर्व काव्य-रचना, आज के युग में भी प्रभूत मात्रा में होती रही है। प्रस्तुत चम्पू-काव्य में महावीर स्वामी के जीवन-चरित के विकास की अपर्व छटा दृष्टिगोचर होती है । काव्य प्रसाद गुण से प्राकण्ठ पूरित है। अलंकारों का प्रयोग प्रचुरता से किया गया है । मार्मिक स्थलों पर उपयुक्त रस को अभिव्यक्ति सहज रूप से प्रस्फुटित हुई है। वैशाली की समृद्धि का वर्णन करते हुए कवि ने वहाँ के राज-प्रासादों के बैभव, उनकी विशालता, वहां रहनेवाली नारियों के अनुपम अंग लावण्य-ग्रादि का मनोरम चित्रण किया है।