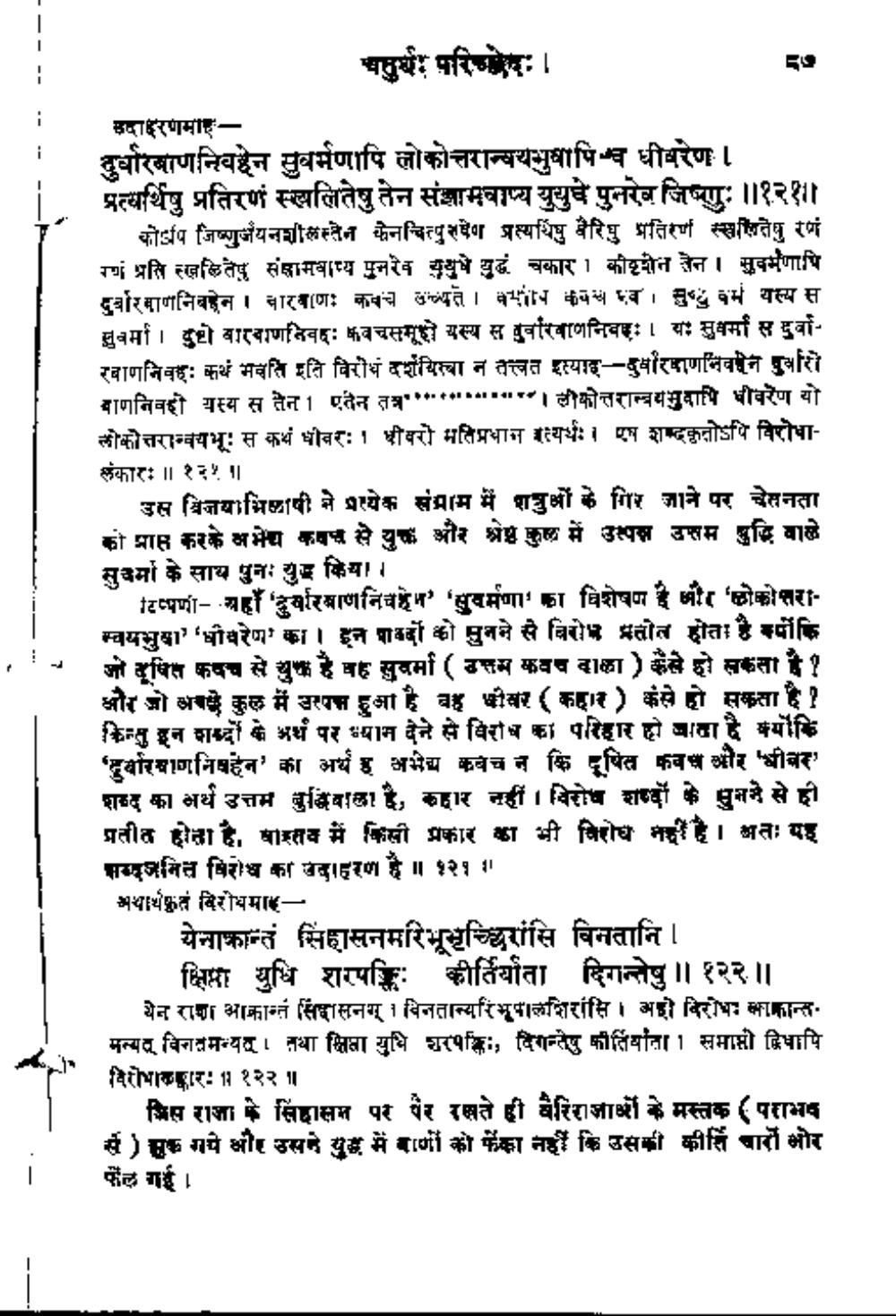________________
¦
i
चतुर्थः परिच्छेदः ।
उदाहरणमाह
दुर्वारवाण निवदेन सुवर्मणापि लोकोत्तरान्वयभुवापि श्व धीवरेण । प्रत्यर्थिषु प्रतिरणं स्खलितेषु तेन संज्ञामवाप्य युयुधे पुनरेव जिष्णुः ॥१२१॥
-
६७
कोप जिष्णुर्जयनशीलस्तेन केनचित्पुरुषेण प्रत्यर्थिषु वैरिधु प्रतिरर्ण स्खलितेषु रणं यं प्रति स्खलितेषु संज्ञामवाध्य पुनरेव युयुषे युद्धं चकार । कीदृशेन तेन । सुवर्मेणापि दुबरमाणनिबन । चारवाणः कवच उच्यते व सुकर्म यस्य स सुवर्मा। दुधे बारवाणनिवधः कवचसमूहो यस्य स रवाणनिवहः । यः सुधर्मा सदुर्वा - रवाणनिवहः कथं भवति इति विरोध दर्शयित्वा न तत्त्वत इत्याह- दुर्गारानिवदेन दुर्गारो बाणवि यस्य स तेन एतेन तत्र । लोकोत्तरान्त्रयमुदापि धीवरेण यो लोकोत्तरान्वयभूः स कथं धीवरः । दीवरों मतिप्रधान इत्यर्थः । एष शब्दकृतोऽपि विरोधालंकारः ।। १२५ ।।
उस विजयाभिलाषी ने प्रत्येक संग्राम में शत्रुओं के गिर जाने पर चेतनता को प्राप्त करके अभेय कवच से युक्त और श्रेष्ठ कुछ में उत्पन्न उत्तम बुद्धि वाले सुत्रों के साथ पुनः युद्ध किया ।
टिप्पणी- यहाँ 'दुरषाणनिचग' 'सुवर्मणा' का विशेषण है और 'छोकोतरास्वयभुषा' 'धीरे' का। इन प्रावदों को सुनने से विरोध प्रतीत होता है क्योंकि जो दूषित कवच से युक्त है वह सुवर्मा ( उत्तम कवच वाला ) कैसे हो सकता है ? और जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है वह छोवर ( कहार ) कैसे हो सकता है ? किन्तु इन शब्दों के अर्थ पर ध्यान देने से विरोध का परिहार हो जाता है क्योंकि 'दुराणनिषन' का अर्थ इ अभेद्य कवच न कि दूषित कवच और 'वीच' शब्द का अर्थ उत्तम बुद्धिवाला है, कहार नहीं । विरोध शब्दों के सुनने से ही प्रतीत होता है, बाद में किसी प्रकार का भी विशेष नहीं है। अतः यह जति विशेष का उदाहरण है ।। १२१ ।।
यथार्थ विरोधमा
येनाक्रान्तं सिंहासनमरिभूधिरांसि विनतानि ।
क्षित युधि शरपङ्किः कीर्तिर्यता दिगन्तेषु ।। १२२ ।। नराशा आकान्तं सिंहासनम् । विनतान्यरिभूपालशिरांसि । अहो विरोधः काकान्समन्यत् विगतमन्यत् । तथा क्षिप्ता युधि शरपक्तिः, दिगन्तेषु कीर्तियांता समाप्ती द्विधापि विरोधाङ्कारः ॥ १२२ ॥
जिस राजा के सिंहासन पर पैर रखते ही वैरिराजाओं के मस्तक ( पराभव से) झुक गये और उसने युद्ध में बाणों को फेंका नहीं कि उसकी कीर्ति चारों ओर फैल गई।