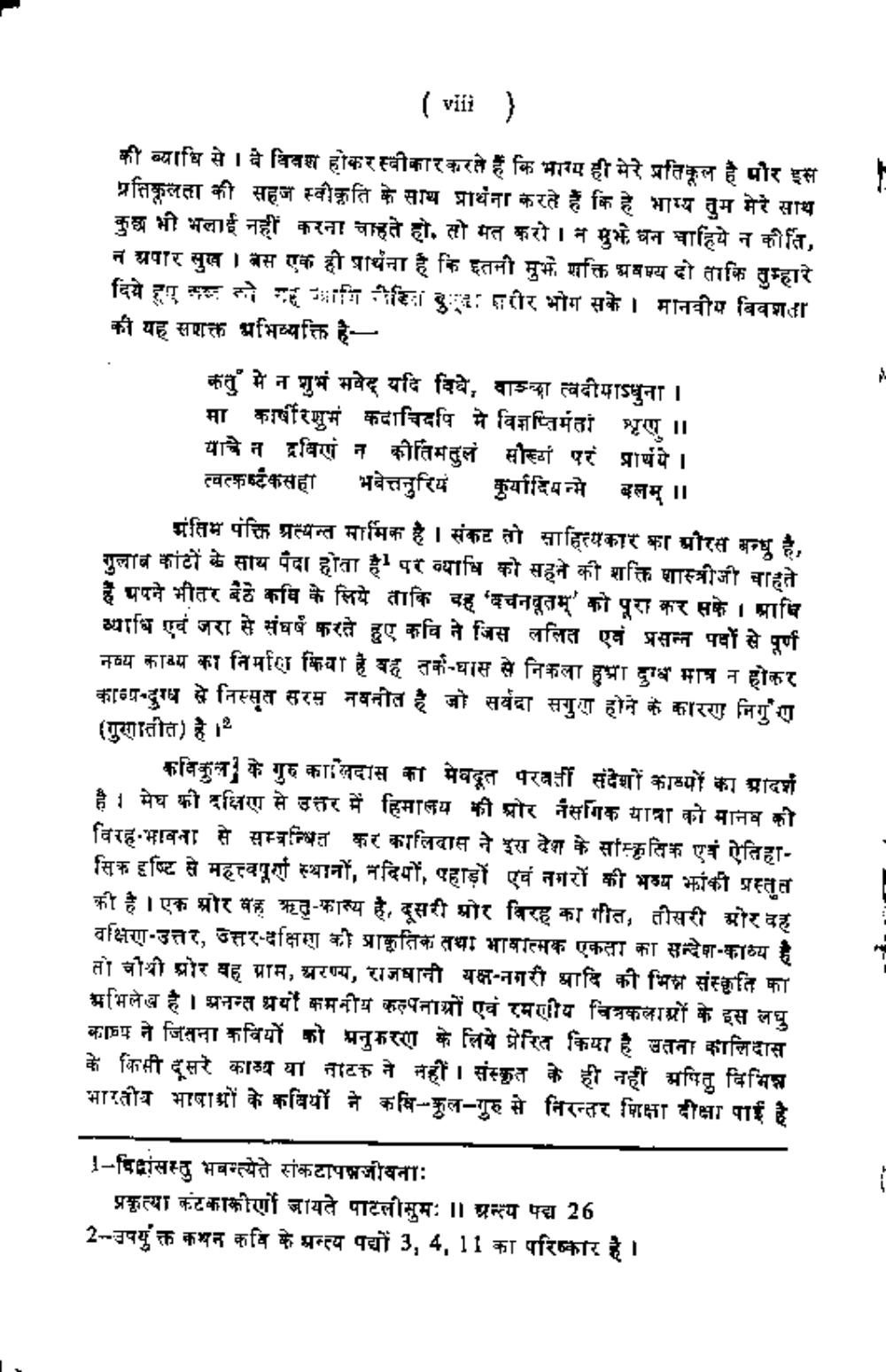________________
की ब्याधि से । वे विवश होकर स्वीकार करते हैं कि भाग्य ही मेरे प्रतिकूल है पौर इस प्रतिकुलता की सहज स्वीकृति के साथ प्रार्थना करते हैं कि हे भाम्य तुम मेरे साथ कुछ भी भलाई नहीं करना चाहते हो. सो मत करो । न मुझे धन चाहिये न कीर्ति, न अपार सुख । बस एक ही प्रार्थना है कि इतनी मुझे शक्ति अवश्य दो ताकि तुम्हारे दिये हा सन लो महागि नीति बुहारीर भोग सके। मानवीय विवशता की यह सशक्त अभिव्यक्ति है
कत मे न शुभं भवेद् यदि विधे, वाश्या त्वदीयाऽधुना । मा कार्षीरसुमं कदाचिदपि मे विज्ञप्तिमतां शृण ।। याचे न द्रविणं न कीतिमतुलं सौस्ठा पर प्रार्थये ।
त्वत्कष्टकसहा भवेत्तनुरियं कुर्यादियन्मे बलम् ।।
मंतिम पंक्ति प्रत्यन्त मार्मिक है । संकट तो साहित्यकार का औरस बन्धु है, गुलाब कांटों के साथ पैदा होता है। पर क्याधि को सहने की शक्ति शास्त्रीजी चाहते है अपने भीतर बैठे कवि के लिये ताकि वह 'वचनबूतम्' को पूरा कर सके । प्राधि ध्याधि एवं जरा से संघर्ष करते हुए कवि ने जिस ललित एवं प्रसन्न पदों से पूर्ण नध्य काव्य का निर्माण किया है वह तर्क-घास से निकला हुमा दुग्ध मात्र न होकर काम्प्रदुग्ध से निस्सृत सरस नवनीत है जो सर्वदा सगुण होने के कारण निर्गुण (गुणातीत) है।
कविकुल के गुरु कालिदास का मेवदूत परवर्ती संदेशों काठमों का प्रादर्श है । मेघ की दक्षिण से उत्तर में हिमालय की प्रोर नैसगिक यात्रा को मानष की विरह भावना से सम्बन्धित कर कालिदास ने इस देश के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों, नदियों, पहाड़ों एवं नगरों की भव्य झांकी प्रस्तुत की है । एक अोर वह ऋतु-कान्य है, दूसरी पोर विरह का गीत, तीसरी ओर वह वक्षिण-उत्तर, उत्तर-दक्षिा की प्राकृतिक तथा भावात्मक एकता का सन्देश-काव्य है तो चौथी प्रोर वह ग्राम, अरण्य, राजधानी यक्ष-नगरी प्रादि की भिन्न संस्कृति का अभिलेख है । अनन्त अर्यो कमनीय कल्पनाओं एवं रमणीय चित्रकलाओं के इस लघु काध्य ने जितना कवियों को अनुकरण के लिये प्रेरित किया है खतना कालिदास के किसी दूसरे काव्य या नाटक ने नहीं । संस्कृत के ही नहीं अपितु विभिन्न भारतीय भाषाओं के कवियों ने कषि-कुल-गुरु से निरन्तर शिक्षा दीक्षा पाई है
-विधांसस्तु भवन्त्येते संकटापनजीवना:
प्रकृत्या कंटकाकीर्णो जायते पाटलीसुमः ।। अन्त्य पद्य 26 2-उपयुक्त कथन कवि के अन्त्य पद्यों 3, 4, 11 का परिष्कार है।