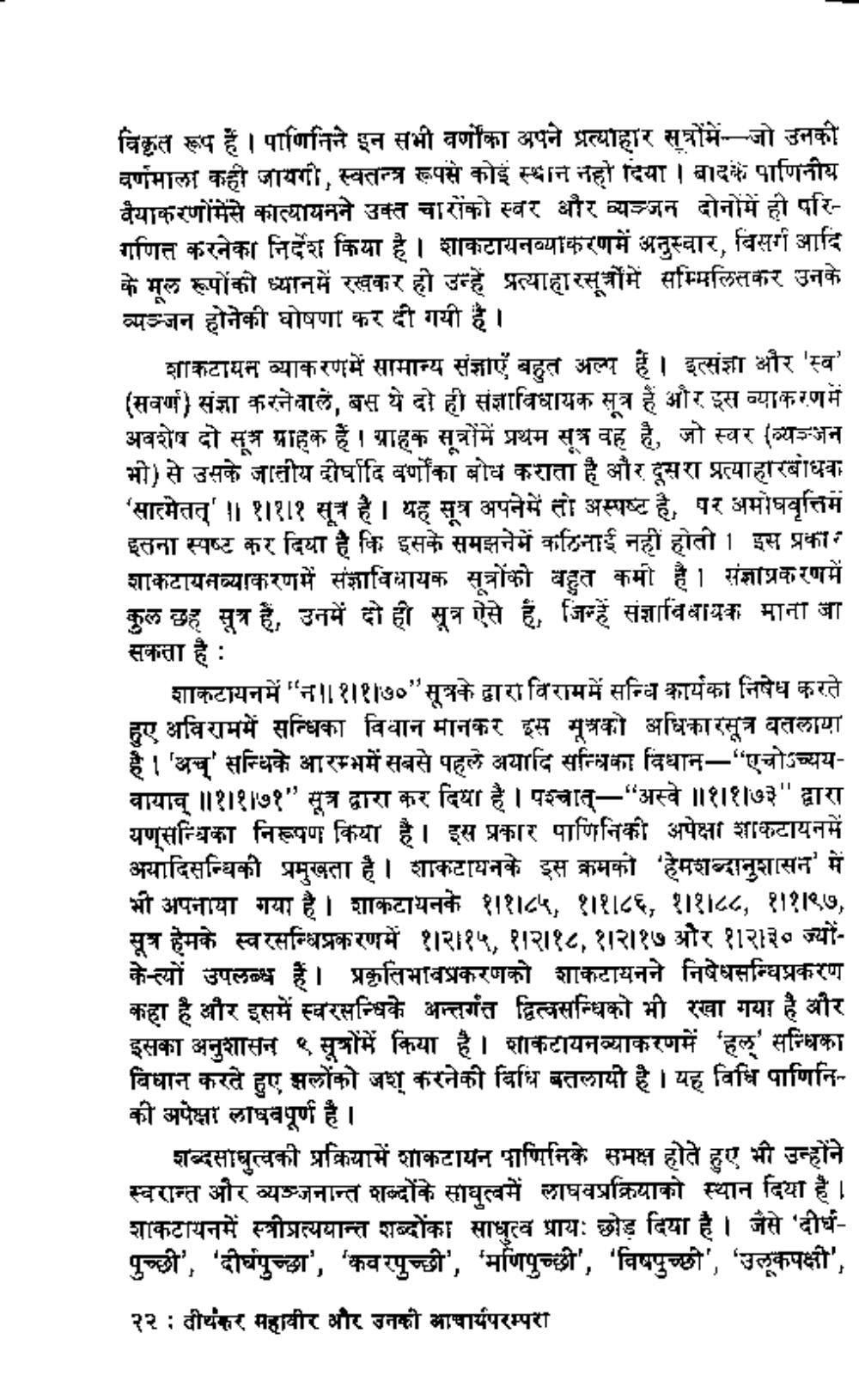________________
विकृत रूप हैं । पाणिनिने इन सभी वर्गोका अपने प्रत्याहार स्त्रोंमें जो उनकी वर्णमाला कही जायगी, स्वतन्त्र रूपसे कोई स्थान नहीं दिया। बादक पाणिनीय वैयाकरणोंमेंसे कात्यायनने उक्त चारोंको स्वर और व्यञ्जन दोनोंमें ही परिगणित करनेका निर्देश किया है। शाकटायनव्याकरणमें अनुस्वार, बिसर्ग आदि के मल रूपोंको ध्यान में रखकर ही उन्हें प्रत्याहारसूत्रोंमें सम्मिलिसकर उनके व्यञ्जन होनेकी घोषणा कर दी गयी है।
शाकटायन' व्याकरण में सामान्य संज्ञाएं बहुत अल्प हैं। इत्संज्ञा और 'स्व' (सवर्ण) संज्ञा करनेवाले, बस ये दो ही संज्ञाविधायक सत्र हैं और इस व्याकरणमें अवशेष दो सूत्र ग्राहक हैं । ग्राहक सूत्रोंमें प्रथम सूत्र वह है, जो स्वर (व्यञ्जन भी) से उसके जातीय दीर्घादि वर्गों का बोध कराता है और दूसरा प्रत्याहारबोधवः 'सात्मेतत् ॥ १।१।१ सूत्र है । यह सूत्र अपने में तो अस्पष्ट है, पर अमोघवृत्तिम इतना स्पष्ट कर दिया है कि इसके समझनेमें कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार शाकटायनव्याकरणमें संज्ञाविधायक सूत्रोंको बहुत कमी है। संज्ञाप्रकरणमें कुल छह सूत्र हैं, उनमें दो ही सूत्र ऐसे हैं, जिन्हें संज्ञाविधायक माना जा सकता है:
शाकटायनमें "न||१११७०" सूत्रके द्वारा विराममें सन्धि कार्यका निषेध करते हुए अविराममें सन्धिका विधान मानकर इस मूत्रको अधिकारसूत्र बतलाया है । 'अच्' सन्धिके आरम्भमें सबसे पहले अयादि सन्धिका विधान-“एचोऽच्ययवाया ॥१।११७१" सूत्र द्वारा कर दिया है । पश्चात्-"अस्वे ॥१३१७३द्वारा यणसन्धिका निरूपण किया है। इस प्रकार पाणिनिकी अपेक्षा साकटायनमें अयादिसन्धिको प्रमुखता है । शाकटायनके इस क्रमको 'हेमशब्दानुशासन' में भी अपनाया गया है। शाकटायनके १२११८५, १३१४८६, १।१८८, १११३९७, सूत्र हेमके स्वरसन्धिप्रकरणमें ||१५, शरा१८,११२।१७ और शरा३० ज्योंके-त्यों उपलब्ध हैं। प्रकृतिभावप्रकरणको शाकटायनने निषेधसन्धिप्रकरण कहा है और इसमें स्वरसन्धिके अन्तर्गत द्वित्वसन्धिको भी रखा गया है और इसका अनुशासन ९ सूओंमें किया है। शाकटायनव्याकरणमें 'हल सन्धिका विधान करते हुए सलोंको जश करनेकी विधि बतलायी है । यह विधि पाणिनिकी अपेक्षा लाघवपूर्ण है। ___ शब्दसाधुत्वकी प्रक्रियामें शाकटायन पाणिनिके समक्ष होते हुए भी उन्होंने स्वरान्त और व्यञ्जनान्त शब्दोंके साधुत्वमें लाघवप्रक्रियाको स्थान दिया है। शाकटायनमें स्त्रीप्रत्ययान्त शब्दोंका साधत्व प्रायः छोड़ दिया है। जैसे 'दीर्घपुच्छी', 'दीर्घपुच्छा', 'कवरपुच्छो', 'मणिपुच्छी', 'विषपुच्छो', 'उलूकपक्षी', २२ : दीर्थकर महावीर और उनकी आचार्यपरम्परा