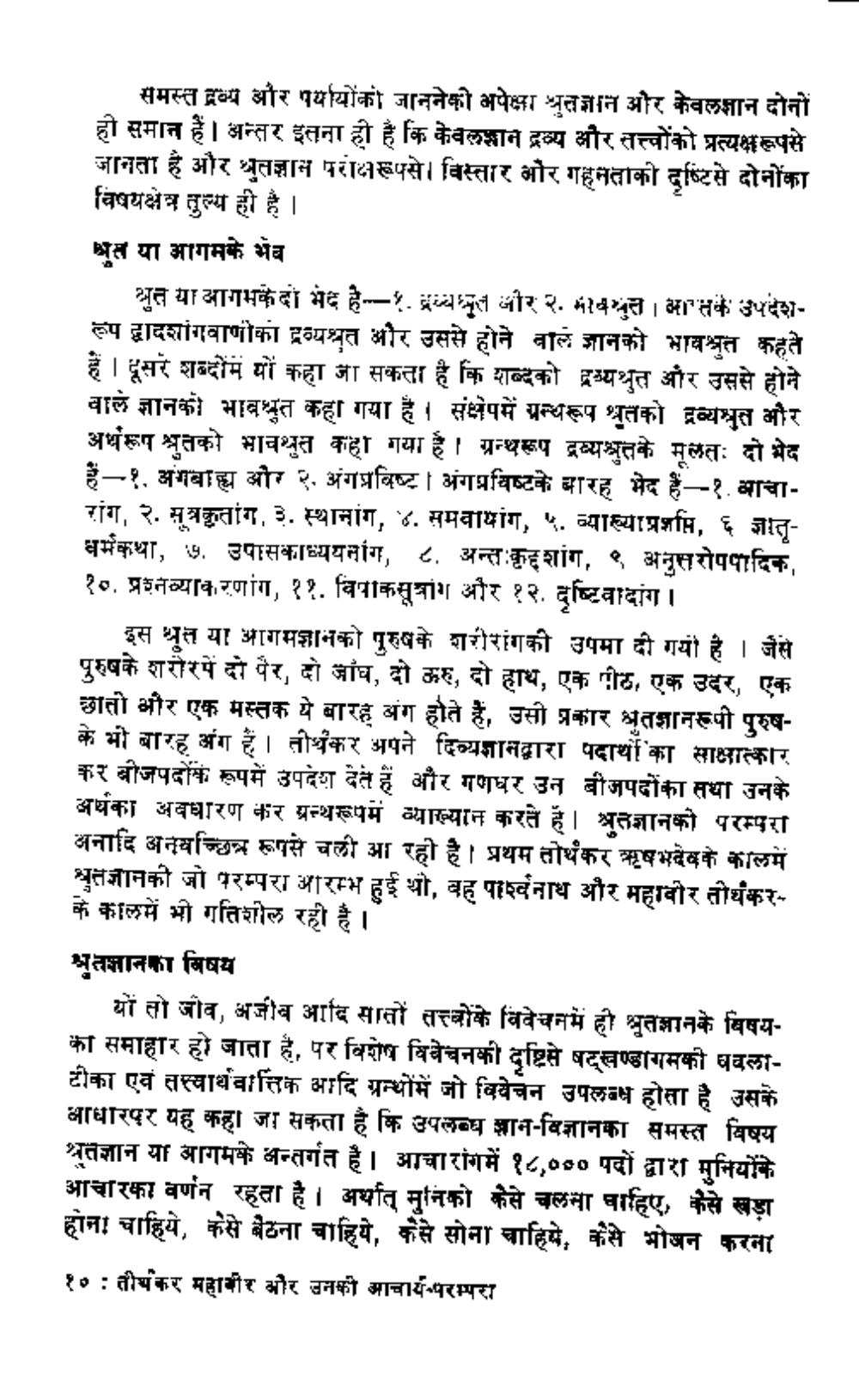________________
समस्त द्रव्य और पर्यायोंको जाननेको अपेक्षा श्रुतज्ञान और केवलज्ञान दोनों ही समान हैं । अन्तर इतना ही है कि केवलज्ञान द्रव्य और तत्त्वों को प्रत्यक्षरूपसे जानता है और श्रुतज्ञान परोक्षरूपसे । विस्तार और गहनताकी दृष्टिसे दोनोंका विषयक्षेत्र तुल्य ही है |
या आगमके ब
जर २ मा
तया आगमके दो भेद है-- १. आग्तके उपदेशरूप द्वादशांगवाणीका द्रव्यश्रुत और उससे होने वाले ज्ञानको भावश्रुत कहते हैं । दूसरे शब्दों यों कहा जा सकता है कि शब्दको द्रव्यभुत और उससे होने वाले ज्ञानको भावश्रुत कहा गया है। संक्षेपमें ग्रन्थरूप श्रुतको द्रव्यश्रुत भौर अर्थरूप श्रुतको भावभूत कहा गया है। ग्रन्थरूप द्रव्यश्रुतके मूलतः दो भेद हैं - १. अंगबाह्य और २. अंगप्रविष्ट । अंगप्रविष्टके बारह भेद हैं-- १. आचा रांग, २. सूत्रकृतांग, ३. स्थानांग, ४. समवायांग, ५. व्याख्याप्रज्ञप्ति, ६ ज्ञातुधर्मकथा, ७ उपासकाध्ययनांग, ८. अन्तःकृद्दशांग ९ अनुतरोपपादिक, १०. प्रश्नव्याकरणांग, ११. विपाकसूत्रांग और १२. दृष्टिवादांग ।
P
इस श्रुतया आगमज्ञानको पुरुष के शरीरांगकी उपमा दी गयी है । जैसे पुरुष के शरीर में दो पैर, दो जाँघ, दो ऊरु, दो हाथ, एक पीठ, एक उदर, एक छाती और एक मस्तक ये बारह अंग होते हैं, उसी प्रकार श्रुतज्ञानरूपी पुरुषके भी बारह अंग हैं। तीर्थंकर अपने दिव्यज्ञानद्वारा पदार्थों का साक्षात्कार कर बीजपदक रूपमें उपदेश देते हैं और गणधर उन बीजपदों का तथा उनके अर्थका अवधारण कर ग्रन्थरूपमें व्याख्यान करते है। श्रुतज्ञानको परम्परा अनादि अनवच्छिन्न रूपसे चली आ रही है। प्रथम तोर्थंकर ऋषभदेव के कालमें श्रुतज्ञानकी जो परम्परा आरम्भ हुई थी, बहु पार्श्वनाथ और महावीर तीर्थंकरके कालमें भी गतिशील रही है ।
श्रुतज्ञानका विषय
यों तो जीव, अजीव आदि सातों तत्वोंके विवेचनमें ही श्रुतज्ञान के विषयका समाहार हो जाता है, पर विशेष विवेचनकी दृष्टिसे षट्खण्डागमकी घवलाटीका एवं तस्वार्थवासिक आदि ग्रन्थोंमें जो विवेचन उपलब्ध होता है उसके आधारपर यह कहा जा सकता है कि उपलब्ध ज्ञान-विज्ञानका समस्त विषय श्रुतज्ञान या आगमके अन्तर्गत है । आचारांग में १८,००० पदों द्वारा मुनियोंके आचारका वर्णन रहता है। अर्थात् मुनिको कैसे चलना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिये कैसे बैठना चाहिये, कैसे सोना चाहिये, कैसे भोजन करना
१०: तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य परम्परा