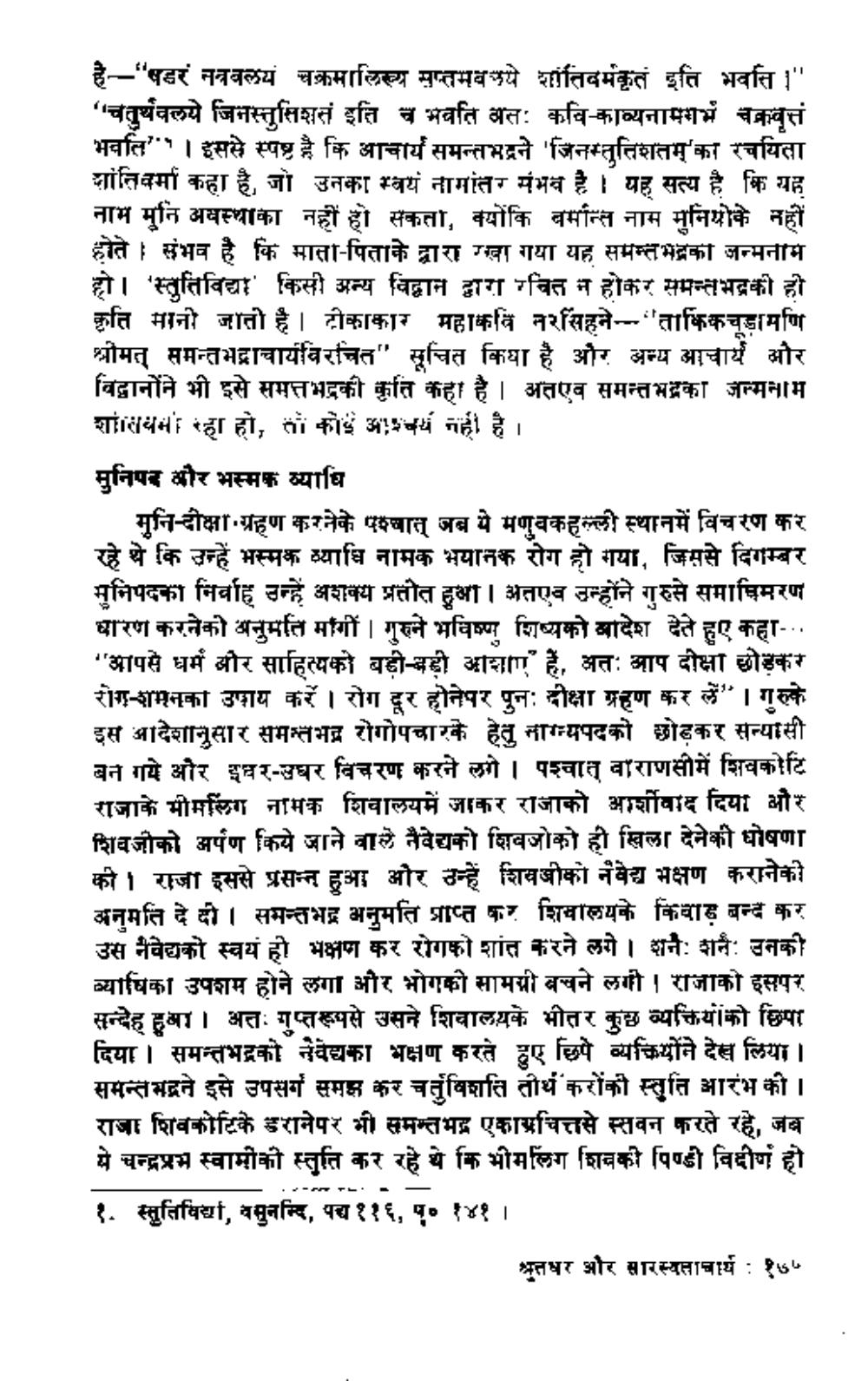________________
है-"पहरं नववलयं चक्रमालिख्य सप्तमवलये शांतिवर्मकृतं इति भवति ।' "चतुर्थवलये जिनस्तुतिशतं इति च भवति अतः कवि-काव्यनामगर्भ चक्रवृत्तं भवति'। इससे स्पष्ट है कि आचार्य समन्तभद्रने 'जिनम्तुतिशतम् का रचयिता शांतिवर्मा कहा है, जो उनका स्वयं नामांतर संभव है। यह सत्य है कि यह नाम मुनि अवस्थाका नहीं हो सकता, क्योंकि वर्मान्त नाम मुनियोके नहीं होते। संभव है कि माता-पिताके द्वारा रखा गया यह समन्तभद्रका जन्मनाम हो। 'स्तुतिविद्या किसी अन्य विद्वान द्वारा रचित न होकर समन्तभद्रकी ही कृति मानी जाती है | टीकाकार महाकवि नरसिंहने-'ताफिकचडामणि श्रीमत् समन्तभद्राचार्यविरचित" सूचित किया है और अभ्य आचार्य और विद्वानोंने भी इसे समत्तभद्रकी कृति कहा है। अतएव समन्तभद्रका जन्मनाम शांसियमा रहा हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है। मुनिपर और भस्मक व्याधि ____ मुनि-दीक्षा ग्रहण करनेके पश्चात् जब ये मणुवकहल्ली स्थानमें विचरण कर रहे थे कि उन्हें भस्मक व्याधि नामक भयानक रोग हो गया, जिससे दिगम्बर मुनिपदका निर्वाह उन्हें अशक्य प्रतीत हुआ। अतएव उन्होंने गुरुसे समाधिमरण धारण करनेको अनुमति मांगी | गुरुने भविष्य शिष्यको बादेश देते हुए कहा-.. "आपसे धर्म और साहित्यको बड़ी-बड़ी आशाएं हैं, अत: आप दीक्षा छोड़कर रोग-शमनका उपाय करें। रोग दूर होनेपर पुन: दीक्षा ग्रहण कर लें | गरुके इस आदेशानुसार समन्तभन्न रोगोपचारके हेतु नान्यपदको छोड़कर सन्यासी बन गये और इधर-उधर विचरण करने लगे। पश्चात् वाराणसीमें शिवकोटि राजाके भीमसिंग नामक शिवालयमें जाकर राजाको आर्शीवाद दिया और शिवजीको अर्पण किये जाने वाले नैवेद्यको शिवजोको ही खिला देनेकी घोषणा की। राजा इससे प्रसन्न हुआ और उन्हें शिवजीको नैवेद्य भक्षण करानेको अनुमति दे दी। समन्तभद्र अनुमति प्राप्त कर शिवालयके किवाड़ बन्द कर उस नैवेद्यको स्वयं ही भक्षण कर रोगको शांत करने लगे। शनैः शनैः उनकी व्याधिका उपशम होने लगा और भोगको सामग्री बचने लगी । राजाको इसपर सन्देह हुआ। अतः गुप्तरूपसे उसने शिवालयके भीतर कुछ व्यक्तियोंको छिपा दिया। समन्तभद्रको नैवेद्यका भक्षण करते हुए छिपे व्यक्तियोंने देख लिया। समन्तभद्रने इसे उपसर्ग समझ कर चर्तुविशति तीर्थ करोंकी स्तुति आरंभ की । राजा शिवकोटिके डरानेपर भी समन्तभद्र एकाग्रचित्तसे स्तवन करते रहे, जब ये चन्द्रप्रभ स्वामीकी स्तुति कर रहे थे कि भीमलिंग शिवकी पिण्डी विदीर्ण हो १. स्तुतिषि, वसुनन्दि, पद्य ११६, पृ. १४१ ।
श्रुतधर और सारस्वताचार्य : १७५