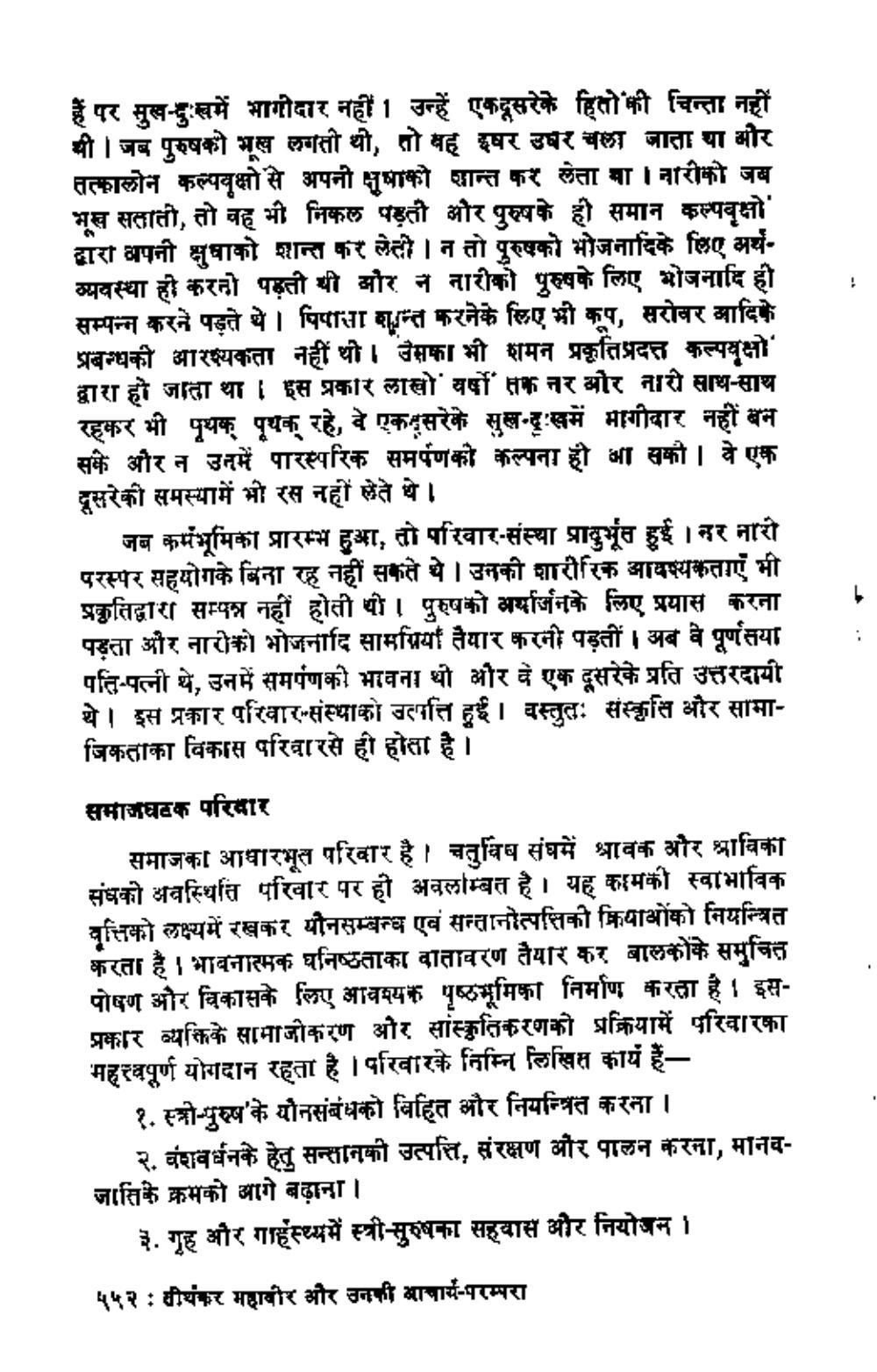________________
हैं पर सुख-दुःखमें भागीदार नहीं। उन्हें एकदूसरेके हितों की चिन्ता नहीं थी । जब पुरुषको भूख लगती थी, तो वह इधर उधर चला जाता था और तत्कालोन कल्पवृक्षो से अपनी क्षुषाको शान्त कर लेता था । नारीको जब भूख सताती, तो वह भी निकल पड़ती और पुरुषके ही समान कल्पवृक्षो' द्वारा अपनी क्षुषाको शन्त कर लेती । न तो पुरुषको भोजनादिके लिए अर्थव्यवस्था ही करनी पड़ती थी और न नारीको पुरुषके लिए भोजनादि ही सम्पन्न करने पड़ते थे। पिपासा शान्त करने के लिए भी कूप, सरोवर आदिके प्रबन्धकी आरश्यकता नहीं थी। जैसका भी शमन प्रकृतिप्रदत्त कल्पवृक्षों द्वारा हो जाता था । इस प्रकार लाखों वर्षों तक नर और नारी साथ-साथ रहकर भी पृथक् पृथक् रहे, वे एकदसरेके सुख-दुःसमें भागीदार नहीं बन सके और न उनमें पारस्परिक समर्पणको कल्पना ही आ सकी। वे एक दूसरेकी समस्या भी रस नहीं लेते थे। __ जब कर्मभूमिका प्रारम्भ हुआ, तो परिवार-संस्था प्रादुर्भूत हुई । नर नारी परस्पर सहयोगके बिना रह नहीं सकते थे। उनकी शारीरिक आवश्यकताएं भी प्रकृतिद्वारा सम्पन्न नहीं होती थी। पुरुषको अर्जिनके लिए प्रयास करना पड़ता और नारीको भोजनादि सामग्नियां तैयार करनी पड़तीं। अब वे पूर्णतया पति-पत्नी थे, उनमें समर्पणको भावना थी और वे एक दूसरेके प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रकार परिवार संस्थाको उत्पत्ति हुई। वस्तुतः संस्कृति और सामाजिकताका विकास परिवारसे ही होता है । समाजघटक परिवार
समाजका आधारभूत परिवार है। चतुर्विष संघमें श्रावक और श्राविका संघको अवस्थिति परिवार पर ही अवलम्बित है। यह कामकी स्वाभाविक वृत्तिको लक्ष्यमें रखकर यौनसम्बन्ध एवं सन्तानोत्पत्तिकी क्रियाओंको नियन्त्रित करता है । भावनात्मक घनिष्ठताका वातावरण तैयार कर बालकोंके समुचित पोषण और विकासके लिए आवश्यक पृष्ठभूमिका निर्माण करता है । इसप्रकार व्यक्तिके सामाजीकरण और सांस्कृतिकरणको प्रक्रियामें परिवारका महत्वपूर्ण योगदान रहता है । परिवारके निम्नि लिखिप्त कार्य हैं
१. स्त्री-पुरुष'के यौनसंबंधको विहित और नियन्त्रित करना ।
२. वंशवर्धनके हेतु सन्तानकी उत्पत्ति, संरक्षण और पालन करना, मानवजातिके क्रमको आगे बढ़ाना।
३. गृह और गार्हस्थ्यमें स्त्री-सुरुषका सहवास और नियोजन । ५५२ : तीर्थकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा