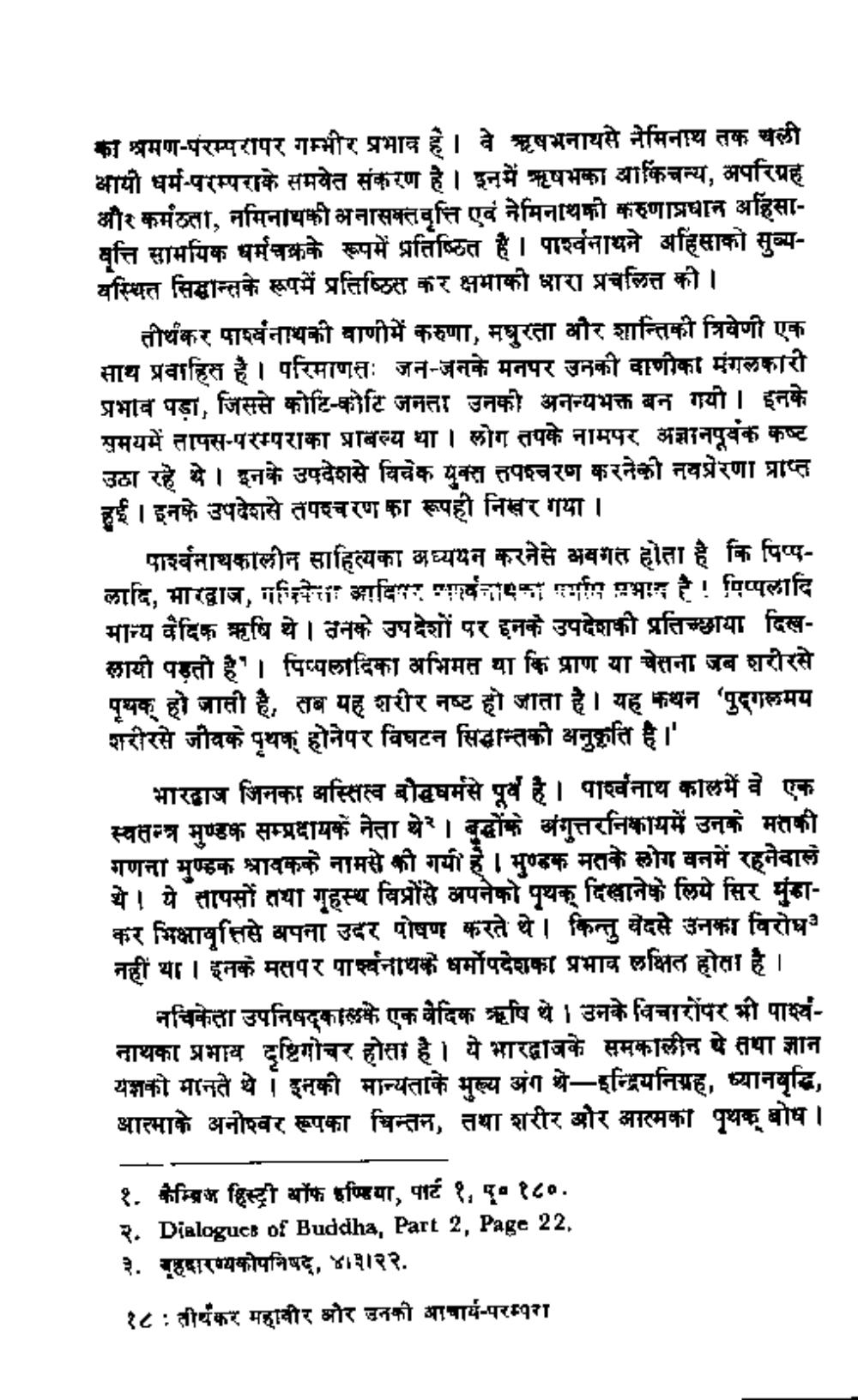________________
का श्रमण परम्परापर गम्भीर प्रभाव है । वे ऋषभनाथसे नेमिनाथ तक चली आय धर्म-परम्परा समवेत संकरण है । इनमें ऋषभका आकिंचन्य, अपरिग्रह और कर्मठता, नमिनाथकी अनासक्त वृत्ति एवं नेमिनाथकी करुणाप्रधान अहिंसावृत्ति सामयिक धर्म चक्र के रूपमें प्रतिष्ठित है । पार्श्वनाथने अहिंसाको सुव्यवस्थित सिद्धान्तके रूपमें प्रतिष्ठित कर क्षमाकी धारा प्रचलित की ।
तीर्थंकर पार्श्वनाथकी वाणीमें करुणा, मधुरता और शान्तिकी त्रिवेणी एक साथ प्रवाहित है । परिमाणतः जन-जनके मनपर उनकी वाणीका मंगलकारी प्रभाव पड़ा, जिससे कोटि-कोटि जनता उनकी अनन्यभक्त बन गयी। इनके समयमें तापस-परम्पराका प्राबल्य था । लोग तपके नामपर अज्ञानपूर्वक कष्ट उठा रहे थे । इनके उपदेशसे विवेक युक्त तपश्चरण करनेकी नवप्रेरणा प्राप्त हुई। इनके उपदेशसे तपश्चरण का रूपही निखर गया ।
पार्श्वनाथकालीन साहित्यका अध्ययन करनेसे अवगत होता है कि पिप्पलादि, भारद्वाज, आदर भाव है। पिप्पलादि मान्य वैदिक ऋषि थे। उनके उपदेशों पर इनके उपदेशकी प्रतिच्छाया दिखलायी पड़ती है । पिप्पलादिका अभिमत था कि प्राण या चेतना जब शरीरसे पृथक हो जाती है, तब यह शरीर नष्ट हो जाता है। यह कथन 'पुद्गलमय शरीरसे जीवके पृथक होनेपर विघटन सिद्धान्तको अनुकृति है ।'
भारद्वाज जिनका अस्तित्व बौद्धधर्मसे पूर्व है। पार्श्वनाथ कालमें वे एक स्वतन्त्र मुण्डक सम्प्रदायकें नेता थे । बुद्धोंके अंगुत्तरनिकायमें उनके मत्तकी गणना मुण्डक श्रावकके नामसे की गयी है । मुण्डक मतके लोग वनमें रहनेवाले थे। ये सापसों तथा गृहस्थ विप्रोंसे अपनेको पृथक् दिखानेके लिये सिर मुंडाकर भिक्षावृत्तिसे अपना उदर पोषण करते थे । किन्तु वेदसे उनका विरोध नहीं था । इनके मसपर पार्श्वनाथ के धर्मोपदेशका प्रभाव लक्षित होता है ।
नचिकेता उपनिषदकालके एक वैदिक ऋषि थे। उनके विचारोंपर भी पाश्यंनाथका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । ये भारद्वाजके समकालीन थे तथा ज्ञान यज्ञको मानते थे । इनकी मान्यता के मुख्य अंग थे – इन्द्रियनिग्रह, ध्यानबृद्धि, आत्मा के अनीश्वर रूपका चिन्तन, तथा शरीर और आत्मका पृथक बोध ।
१. कैम्ब्रिम हिस्ट्री ऑफ इण्डिया पार्ट १ ० १८०.
२. Dialogues of Buddha, Part 2, Page 22, ३. गृहदारण्यकोपनिषद्, ४३२२.
१८ : तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा