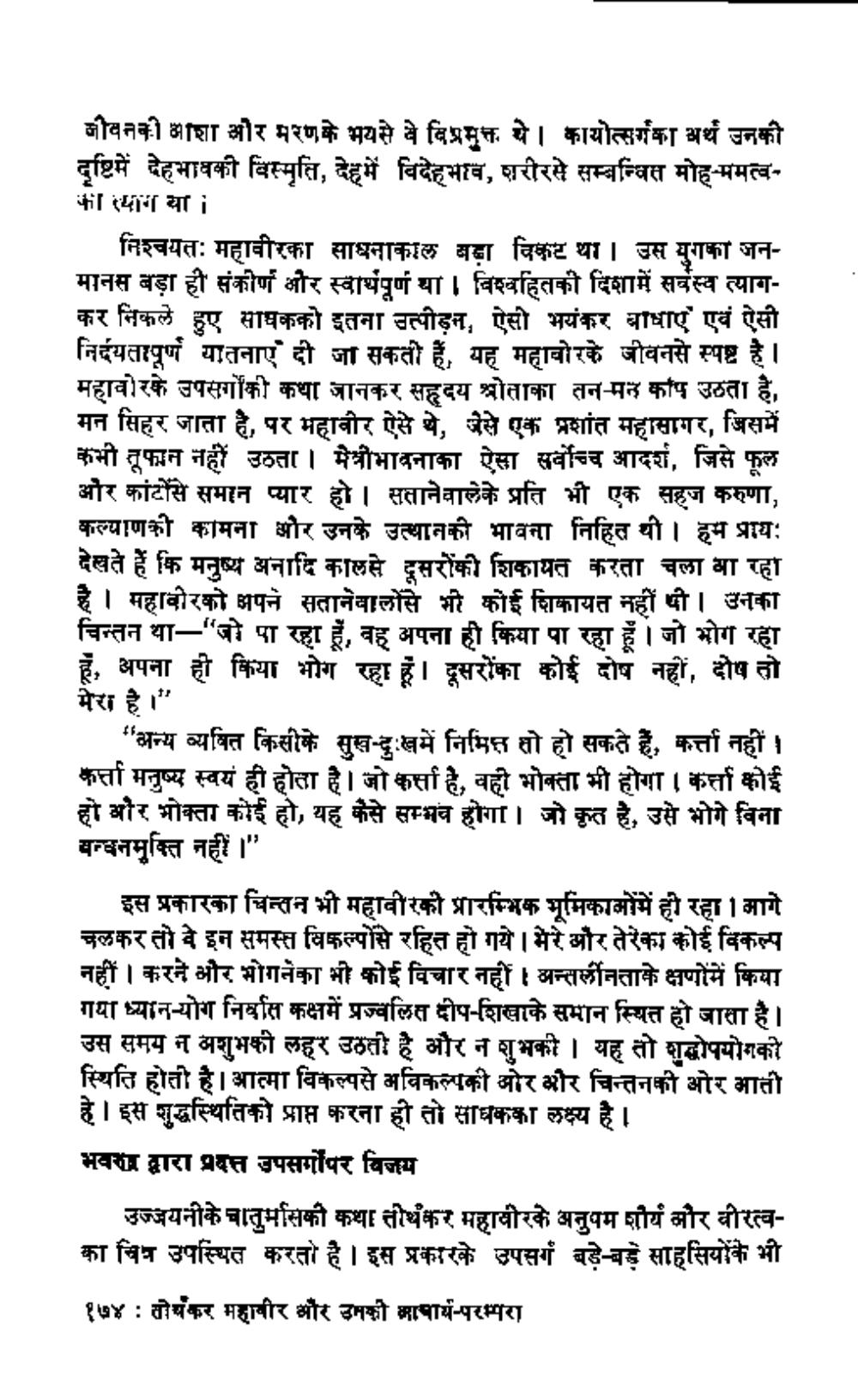________________
जीवनको आशा और मरण के भय से वे विप्रमुक्त थे । कायोत्सर्गका अर्थ उनकी दृष्टिमें देहभावकी विस्मृति, देह में विदेहभाव, शरीर से सम्बन्धित मोह-ममत्व
का त्याग या ।
निश्चयतः महावीरका साधनाकाल बड़ा विकट था । उस युगका जनमानस बड़ा ही संकीर्ण और स्वार्थपूर्ण था । विश्वहितकी दिशा में सर्वस्व त्यागकर निकले हुए साधकको इतना उत्पीड़न, ऐसी भयंकर बाधाएं एवं ऐसी निर्दयतापूर्ण यातनाएं दी जा सकती हैं, यह महाबोरके जीवनसे स्पष्ट है । महावीरके उपसर्गों की कथा जानकर सहृदय श्रोताका तन-मन कांप उठता है, मन सिहर जाता है, पर महावीर ऐसे थे, जैसे एक प्रशांत महासागर, जिसमें कभी तूफान नहीं उठता । मैत्रीभावनाका ऐसा सर्वोच्च आदर्श, जिसे फूल और कांटोंसे समान प्यार हो । सतानेवालेके प्रति भी एक सहज करुणा, कल्याणकी कामना और उनके उत्थानको भावना निहित थी। हम प्रायः देखते हैं कि मनुष्य अनादि कालसे दूसरोंकी शिकायत करता चला भा रहा है । महावीर को अपने सतानेवालोंसे भी कोई शिकायत नहीं थी । उनका चिन्तन था - " जो पा रहा हूँ, वह अपना ही किया पा रहा हूँ। जो भोग रहा हूँ, अपना ही किया भोग रहा हूँ। दूसरोंका कोई दोष नहीं, दोष तो मेरा है ।"
" अन्य व्यक्ति किसीके सुख-दुःख में निमित तो हो सकते हैं, कर्त्ता नहीं । कर्त्ता मनुष्य स्वयं ही होता है। जो कर्ता है, वही भोक्ता भी होगा । कर्ता कोई हो और भोक्ता कोई हो, यह कैसे सम्भव होगा। जो कृत है, उसे भोगे विना बन्धनमुक्ति नहीं ।"
इस प्रकारका चिन्तन भी महावीरको प्रारम्भिक भूमिकामोंमें हो रहा | मागे चलकर तो वे इन समस्त विकल्पोंसे रहित हो गये। मेरे और तेरेका कोई विकल्प नहीं । करने और भोगने का भी कोई विचार नहीं । अन्तलीनताके क्षणोंमें किया गया ध्यान-योग निर्वास कक्षमें प्रज्वलित दीप शिखाके समान स्थित हो जाता है। उस समय न अशुभकी लहर उठती है और न शुभकी । यह तो शुद्धोपयोगको स्थिति होती है। आत्मा विकल्पसे अविकल्पकी ओर और चिन्तनकी ओर भाती है । इस शुद्धस्थितिको प्राप्त करना हो तो साधकका लक्ष्य है।
भवरा द्वारा प्रदत्त उपसगवर विजय
उज्जयनीके चातुर्मासकी कथा तीर्थंकर महावीरके अनुपम शौर्य और वीरत्वका चित्र उपस्थित करतो है । इस प्रकारके उपसगं बड़े-बड़े साहसियों के भी
१७४ : तोर्थंकर महावीर और उनकी प्राचार्य-परम्परा