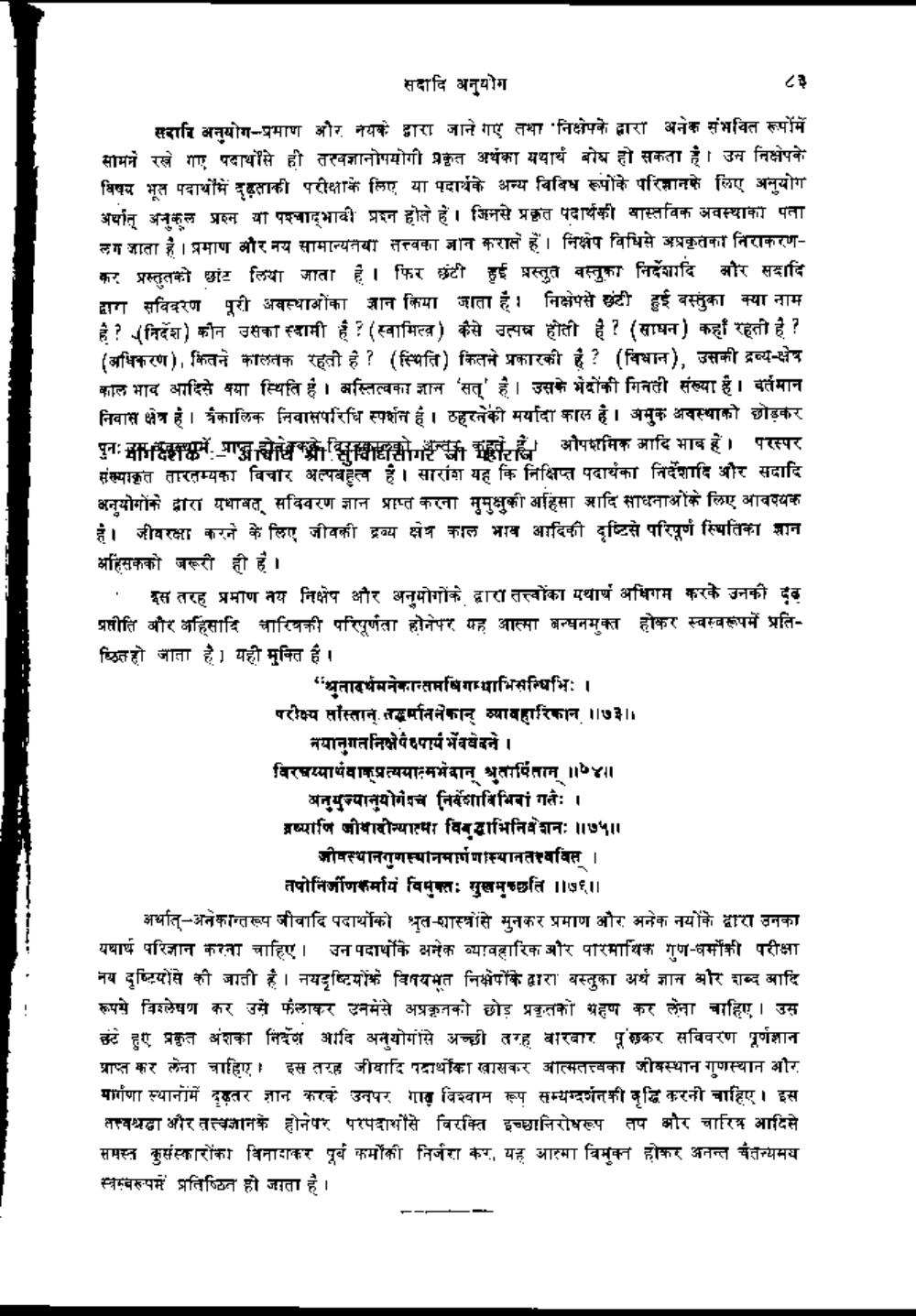________________
सदादि अनुयोग
८३
सानि अनुयोग - प्रमाण और नयके द्वारा जाने गए तथा निक्षेपके द्वारा अनेक संभावित रूपों में सामने रखे गए पदार्थोंसे ही तत्वज्ञानोपयोगी प्रकृत अर्थका यथार्थ बोध हो सकता हूँ। उन निक्षेपके विषय भूल पदार्थों में दृढ़ताकी परीक्षा के लिए या पदार्थके अन्य विविध रूपोंके परिज्ञानके लिए अनुयोग अर्थात् अनुकुल प्रश्न या पश्चाद्भावी प्रश्न होते हैं। जिनसे प्रकृत पदार्थकी वास्तविक अवस्थाका पता लग जाता है। प्रमाण और नय सामान्यतया तत्त्वका ज्ञान कराते हैं। निक्षेप विधिसे अप्रकृतका निराकरणकर प्रस्तुतको छांट लिया जाता है । फिर घंटी हुई प्रस्तुत वस्तुका निर्देशादि और सादि द्वारा सविवरण पूरी अवस्थाओंका ज्ञान किया जाता है। निक्षेपसे घंटी हुई बस्तुका क्या नाम है ? ( निर्देश) कौन उसका स्वामी हूँ ? (स्वामित्व ) कैसे उत्पन्न होती है ? (साधन) कहाँ रहती है ? (अधिकरण) कितने कालतक रहती है ? (स्थिति) कितने प्रकारकी हुँ ? (विधान), उसकी द्रव्य-क्षेत्र काल भाव आदिसे क्या स्थिति है। मस्तित्वका ज्ञान 'सत्' है। उसके भेदोंकी गिनती संख्या है। वर्तमान निवास क्षेत्र है। कालिक निवासपरिधि स्पर्शन है। ठहरतेकी मर्यादा काल है। अमुक अवस्थाको छोड़कर पुनः नाप्राप्त औपशमिक आदि भाव हैं । परस्पर संख्याकृत तारतम्यका विचार अल्पबहुत्व हैं । सारांश यह कि निक्षिप्त पदार्थका निर्देशादि और सदादि अनुयोगोंके द्वारा यथावत् सविवरण ज्ञान प्राप्त करना मुमुक्षुकी अहिंसा आदि साधनाओंके लिए आवश्यक है । जीवरक्षा करने के लिए जीवकी द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदिकी दृष्टिसे परिपूर्ण स्थितिका ज्ञान अहिंसकको जरूरी ही है ।
इस तरह प्रमाण नय निक्षेप और अनुयोगोंके द्वारा तत्त्वोंका यथार्थ अधिगम करके उनकी प्रतीति और अहिंसादि चारित्रकी परिपूर्णता होनेपर यह आत्मा बन्धनमुक्त होकर स्वस्वरूपमें प्रतिठित हो जाता है। यही मुक्ति हैं।
"श्रुतादर्थमनेकान्तमधिगम्याभिसन्धिभिः ।
परीक्ष्य साँस्तान् तद्धर्माननेकान् व्यावहारिकान ॥ ७३ ॥ नयानुगत निक्षेप ६ पार्य भँव वेदने । विरचय्यार्थवाक्प्रत्ययात्मवान् श्रुतार्थताम् ॥७४॥ अनुयुज्यानुयोगच निर्देशाविभियां गतैः । पाणि जीवावन्यात्मा विबुद्धाभिनिवेशनः ॥ ७५ ॥ जीवस्थानगुणस्थानमार्गणास्थानतरववित् । तपोनिर्जीणकर्मायं विमुक्तः सुखमुच्छति ॥७६॥
अर्थात् - अनेकान्तरूप जीवादि पदार्थोको श्रुत-शास्त्रोंसे सुनकर प्रमाण और अनेक नयोंके द्वारा उनका यथार्थ परिज्ञान करना चाहिए। उन पदार्थोके अनेक व्यावहारिक और पारमार्थिक गुण-वर्मोकी परीक्षा नय दृष्टियों से की जाती है। नयदृष्टियों विषयभूत निक्षेपोंके द्वारा वस्तुका अर्थ ज्ञान और शब्द आदि रूपये विश्लेषण कर उसे फैलाकर उनसे अप्रकृतको छोड़ प्रकृतको ग्रहण कर लेना चाहिए। उस छंटे हुए प्रकृत अंशका निर्देश आदि अनुयोगांसे अच्छी तरह वारवार पूछकर सविवरण पूर्णज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए । इस तरह जीवादिपदार्थोका खासकर आत्मतत्त्वका जीवस्थान गुणस्थान और मार्गणा स्थानोंमें दृढतर ज्ञान करके उनपर गाढ़ विश्वास रूप सम्यग्दर्शनकी वृद्धि करनी चाहिए। इस तत्वश्रद्धा और तत्त्वज्ञानके होनेपर परपदार्थोंसे विरक्ति इच्छा निरोधरूप तप और चारित्र आदिसे समस्त कुसंस्कारोंका विनाकर पूर्व कर्मोकी निर्जरा कर यह आत्मा विमुक्त होकर अनन्त चैतन्यमय स्वस्वरूपमं प्रतिष्ठित हो जाता है।