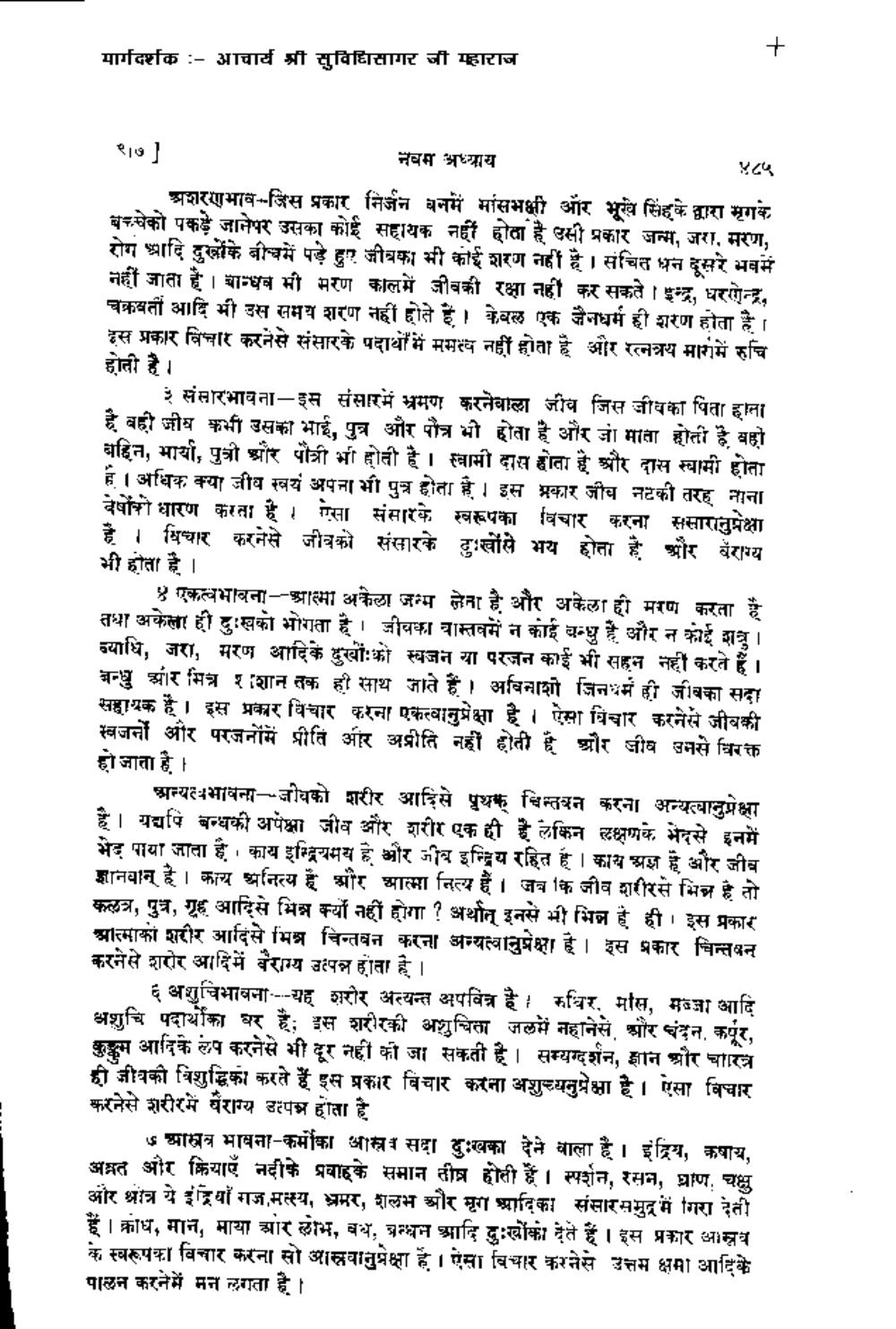________________
मार्गदर्शक :- आचार्य श्री सुविधिसागर जी महाराज
४८५
९७ ]
नवम अध्याय
शरणभाव -- जिस प्रकार निर्जन वनमें मांसभक्षी और भूखे सिंहके द्वारा मृगक को पकड़े जानेपर उसका कोई सहायक नहीं होता है उसी प्रकार जन्म, जरा, मरण, रोगादि दुख बीचमें पड़े हुए जीवका भी कोई शरण नहीं है। संचित धन दूसरे भवमें नहीं जाता है। बान्धव भी मरण कालमें जीवकी रक्षा नहीं कर सकते । इन्द्र, धरणेन्द्र, चक्रवती आदि भी उस समय शरण नहीं होते हैं। केवल एक जैनधर्म ही शरण होता है। इस प्रकार विचार करने से संसार के पदार्थों में ममत्व नहीं होता है और रत्नत्रय मार्गचि होती है।
३ संसारभावना - इस संसार में भ्रमण करनेवाला जीव जिस जीवका पिता होता है बड़ी जी कभी उसका भाई, पुत्र और पौत्र भी होता है और जो माता होती है, बड़ो बहिन, भार्या पुत्री और पौत्री भी होती है। स्वामी दास होता है और दास स्वामी होता है। अधिक क्या जीव स्वयं अपना भी पुत्र होता है। इस प्रकार जीव नटकी तरह नाना देषको धारण करता है। ऐसा संसार के स्वरूपका विचार करना संसारानुप्रेक्षा है । विचार करनेसे जीवको संसारके दुःखोंसे भय होता है और वैराग्य भी होता है ।
४ एकत्वभावना - आत्मा अकेला जन्म लेना है और अकेला ही मरण करता है तथा अकेला ही दुःखको भोगता है। जीवका वास्तवमें न कोई बन्धु है और न कोई शत्रु । व्याधि, जरा, मरण आदिके दुखों को स्वजन या परजन काई भी सहन नहीं करते हैं । बन्धु और मित्र र शान तक ही साथ जाते हैं। अविनाशी जिनधर्म ही जीवका सदा सहायक है । इस प्रकार विचार करना एकत्वानुप्रेक्षा है। ऐसा विचार करनेसे जीवकी स्वजनों और परजनोंमें प्रीति और अप्रीति नहीं होती है और जीव उनसे विरक्त हो जाता है ।
अन्य भावना - जीवको शरीर आदिसे पृथक् चिन्तन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है । यद्यपि बन्धकी अपेक्षा जीव और शरीर एक ही है लेकिन लक्षण के भेदसे इनमें भेद पाया जाता है। काय इन्द्रियमय है और जीव इन्द्रिय रहित हूं। काय अझ है और जीव ज्ञानवान् है । काय अनित्य है और आत्मा नित्य हैं। जब कि जीव शरीर से भिन्न है तो कलत्र, पुत्र, गृह आदिसे भिन्न क्यों नहीं होगा ? अर्थात् इनसे भी भिन्न है ही। इस प्रकार आत्माको शरीर आदि से भिन्न चिन्तवन करना अन्यत्वानुप्रेक्षा है। इस प्रकार चिन्तन करने से शरीर आदि में वैराग्य उत्पन्न होता है ।
६ अशुचिभावना -- यह शरीर अत्यन्त अपवित्र है । कविर, मांस, मब्जा आदि अशुचि पदार्थोंका घर है; इस शरीरकी अशुचिता जलमें नहाने से और चंदन, कर्पूर, कुकुम ' आदिके लेप करने से भी दूर नहीं की जा सकती है। सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र ही जtant विशुद्धिका करते हैं इस प्रकार विचार करना अशुच्यनुप्रेक्षा है। ऐसा विचार करनेसे शरीर में वैराग्य उत्पन्न होता है
+
७ आस्त्र भावना-कर्मो का आस्रव सदा दुःखका देने वाला है । इंद्रिय, कषाय, aa और क्रियाएँ नदीके प्रवाह के समान तीत्र होती हैं। स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु और ये इंद्रियाँ गज, मत्स्य, भ्रमर, शलभ और मृग आदिका संसारसमुद्र में गिरा देती हैं। क्राध, मान, माया और लोभ, वय, बन्धन आदि दुःखोंकी देते हैं। इस प्रकार अनव के स्वरूपका विचार करना सो आस्तवानुप्रेक्षा है। ऐसा विचार करनेसे उत्तम क्षमा आदिके पालन करने में मन लगता है।