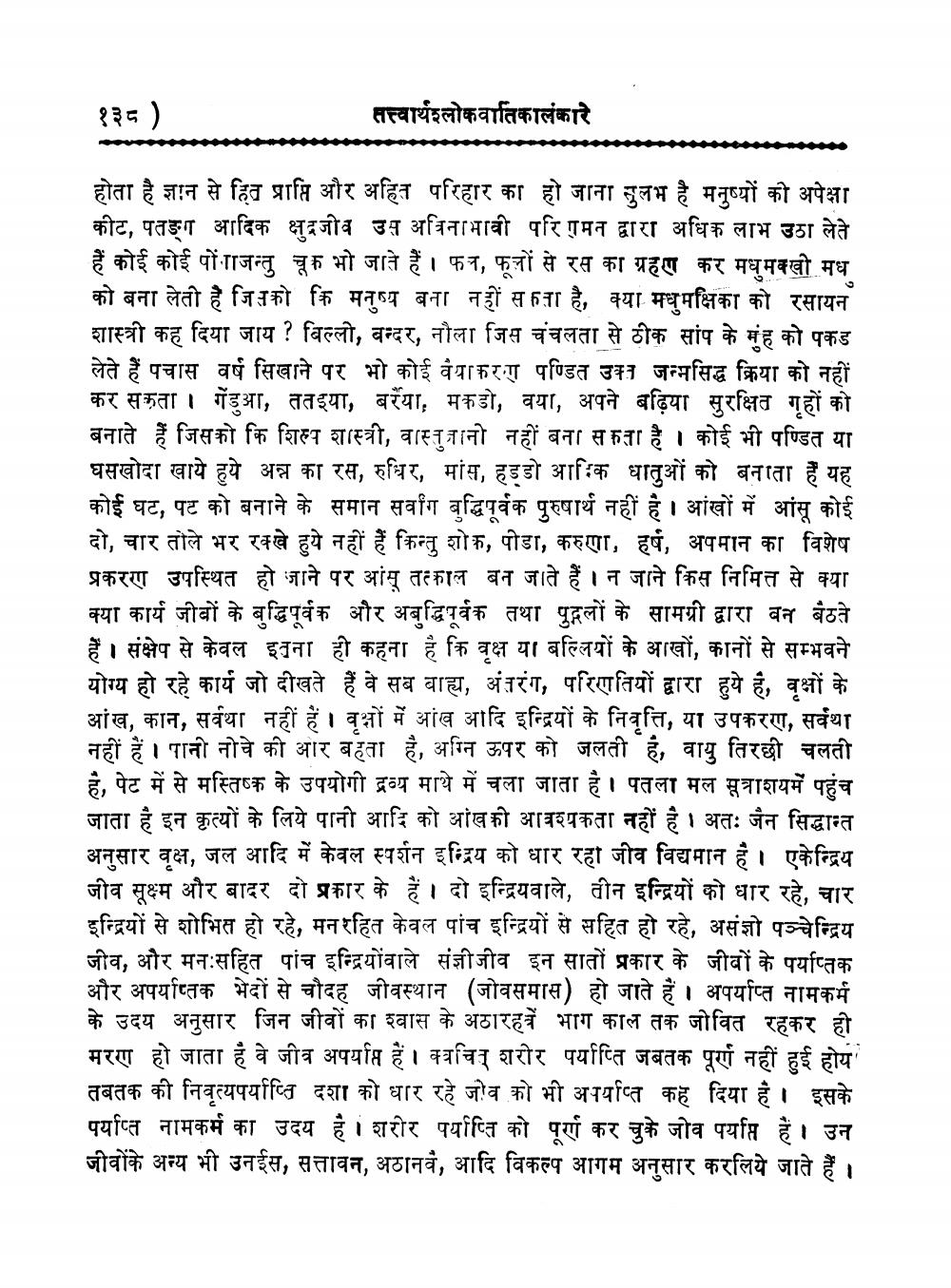________________
१३८ )
तत्त्वार्थश्लोकवातिकालंकारे
-
होता है ज्ञान से हित प्राप्ति और अहित परिहार का हो जाना सुलभ है मनुष्यों की अपेक्षा कीट, पतङ्ग आदिक क्षुद्रजीव उस अविनाभावी परि गमन द्वारा अधिक लाभ उठा लेते हैं कोई कोई पोंगाजन्तु चूक भो जाते हैं। फल, फूलों से रस का ग्रहण कर मधुमक्खी मध को बना लेती है जिसको कि मनुष्य बना नहीं सकता है, क्या मधुमक्षिका को रसायन शास्त्री कह दिया जाय ? बिल्ली, बन्दर, नौला जिस चंचलता से ठीक सांप के मुंह को पकड लेते हैं पचास वर्ष सिखाने पर भी कोई वैयाकरण पण्डित उक्त जन्मसिद्ध क्रिया को नहीं कर सकता। गेंडुआ, ततइया, बरैया, मकडो, वया, अपने बढ़िया सुरक्षित गृहों को बनाते हैं जिसको कि शिल्प शास्त्री, वास्तुनानो नहीं बना सकता है । कोई भी पण्डित या घसखोदा खाये हुये अन्न का रस, रुधिर, मांस, हड्डो आदिक धातुओं को बनाता हैं यह कोई घट, पट को बनाने के समान सर्वांग बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ नहीं है। आंखों में आंसू कोई दो, चार तोले भर रक्खे हुये नहीं हैं किन्तु शोक, पीडा, करुणा, हर्ष, अपमान का विशेष प्रकरण उपस्थित हो जाने पर आंसू तत्काल बन जाते हैं । न जाने किस निमित्त से क्या क्या कार्य जीवों के बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक तथा पुद्गलों के सामग्री द्वारा बन बैठते हैं। संक्षेप से केवल इतना ही कहना है कि वृक्ष या बल्लियों के आखों, कानों से सम्भवने योग्य हो रहे कार्य जो दीखते हैं वे सब बाह्य, अंतरंग, परिणतियों द्वारा हुये है, वृक्षों के आंख, कान, सर्वथा नहीं हैं। वृक्षों में आंख आदि इन्द्रियों के निवृत्ति, या उपकरण, सर्वथा नहीं हैं। पानी नोचे की आर बहता है, अग्नि ऊपर को जलती है, वायु तिरछी चलती है, पेट में से मस्तिष्क के उपयोगी द्रव्य माथे में चला जाता है। पतला मल मूत्राशयमें पहुंच जाता है इन कृत्यों के लिये पानी आदि को आंख की आवश्यकता नहीं है । अतः जैन सिद्धान्त अनुसार वृक्ष, जल आदि में केवल स्पर्शन इन्द्रिय को धार रहा जीव विद्यमान है। एकेन्द्रिय जीव सूक्ष्म और बादर दो प्रकार के हैं। दो इन्द्रियवाले, तीन इन्द्रियों को धार रहे, चार इन्द्रियों से शोभित हो रहे, मनरहित केवल पांच इन्द्रियों से सहित हो रहे, असंज्ञो पञ्चेन्द्रिय जीव, और मनःसहित पांच इन्द्रियोंवाले संज्ञीजीव इन सातों प्रकार के जीवों के पर्याप्तक
और अपर्याप्तक भेदों से चौदह जीवस्थान (जोवसमास) हो जाते हैं। अपर्याप्त नामकर्म के उदय अनुसार जिन जीवों का श्वास के अठारहवें भाग काल तक जीवित रहकर ही मरण हो जाता है वे जीव अपर्याप्त है। क्वचित् शरीर पर्याप्ति जबतक पूर्ण नहीं हुई होय' तबतक की निवृत्यपर्याप्ति दशा को धार रहे जोव को भी अपर्याप्त कह दिया है। इसके पर्याप्त नामकर्म का उदय है। शरीर पर्याप्ति को पूर्ण कर चुके जोव पर्याप्त हैं। उन जीवोंके अन्य भी उनईस, सत्तावन, अठानवे, आदि विकल्प आगम अनुसार करलिये जाते हैं।