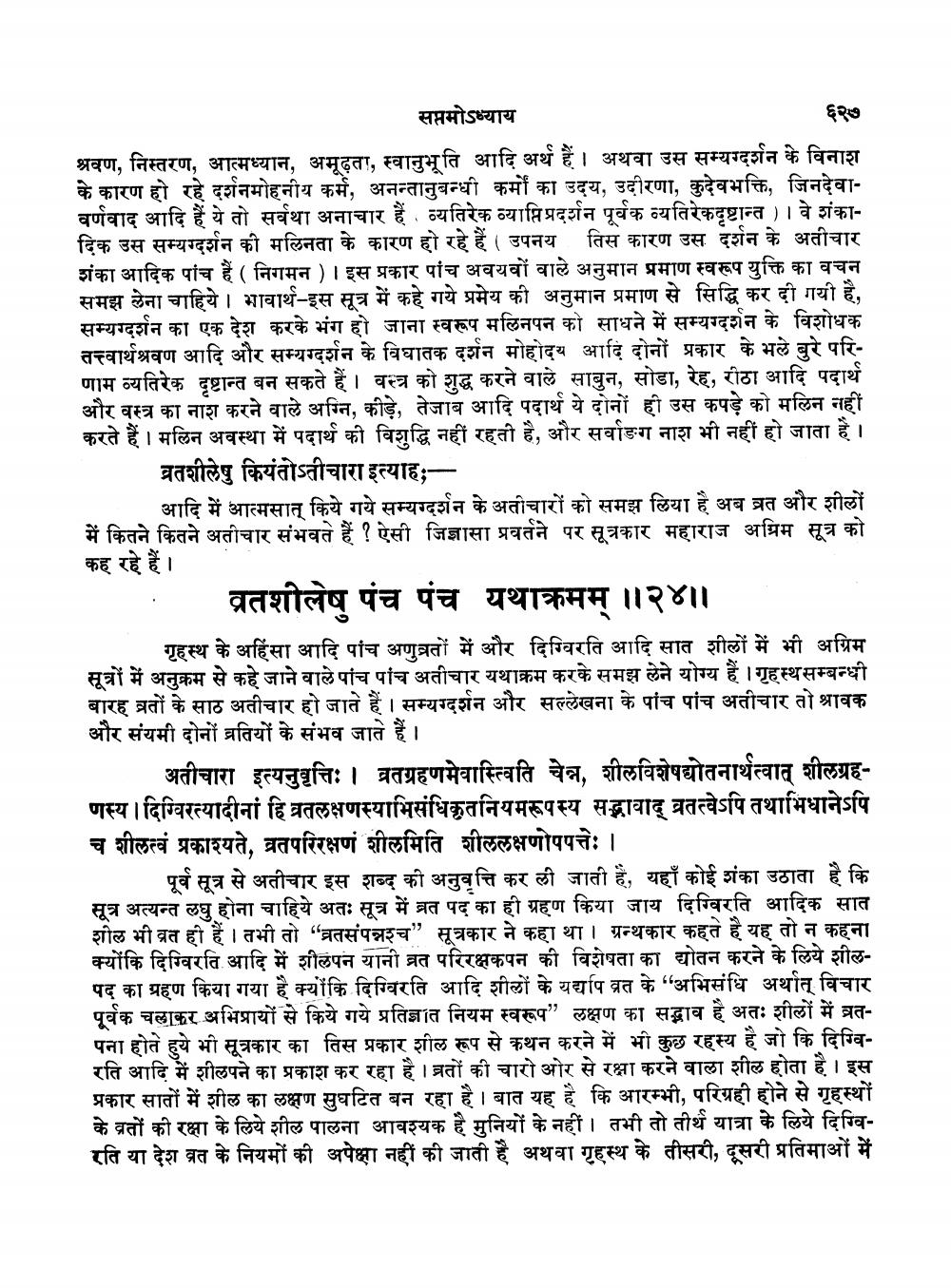________________
सप्तमोऽध्याय
६२७
श्रवण, निस्तरण, आत्मध्यान, अमूढ़ता, स्वानुभूति आदि अर्थ हैं । अथवा उस सम्यग्दर्शन के विनाश के कारण हो रहे दर्शनमोहनीय कर्म, अनन्तानुबन्धी कर्मों का उदय, उदीरणा, कुदेवभक्ति, जिनदेवावर्णवाद आदि हैं ये तो सर्वथा अनाचार हैं। व्यतिरेक व्याप्तिप्रदर्शन पूर्वक व्यतिरेकदृष्टान्त ) । वे शंकादिक उस सम्यग्दर्शन की मलिनता के कारण हो रहे हैं । उपनय तिस कारण उस दर्शन के अतीचार शंका आदि पांच हैं ( निगमन) । इस प्रकार पांच अवयवों वाले अनुमान प्रमाण स्वरूप युक्ति का वचन समझ लेना चाहिये। भावार्थ - इस सूत्र में कहे गये प्रमेय की अनुमान प्रमाण से सिद्धि कर दी गयी है, सम्यग्दर्शन का एक देश करके भंग हो जाना स्वरूप मलिनपन को साधने में सम्यग्दर्शन के विशोधक तत्वार्थश्रवण आदि और सम्यग्दर्शन के विघातक दर्शन मोहोदय आदि दोनों प्रकार के भले बुरे परिणाम व्यतिरेक दृष्टान्त बन सकते हैं । वस्त्र को शुद्ध करने वाले साबुन, सोडा, रेह, रीठा आदि पदार्थ और वस्त्र का नाश करने वाले अग्नि, कीड़े, तेजाब आदि पदार्थ ये दोनों ही उस कपड़े को मलिन नहीं करते हैं । मलिन अवस्था में पदार्थ की विशुद्धि नहीं रहती है, और सर्वाङग नाश भी नहीं हो जाता है ।
व्रतशीलेषु कियंतो ती चारा इत्याह;
आदि में आत्मसात किये गये सम्यग्दर्शन के अतीचारों को समझ लिया है अब व्रत और शीलों में कितने कितने अतीचार संभवते हैं ? ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर सूत्रकार महाराज अग्रिम सूत्र को कह रहे हैं।
व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् ॥२४॥
गृहस्थ के अहिंसा आदि पांच अणुव्रतों में और दिग्विरति आदि सात शीलों में भी अग्रिम सूत्रों में अनुक्रम से कहे जाने वाले पांच पांच अतीचार यथाक्रम करके समझ लेने योग्य हैं । गृहस्थ सम्बन्धी बारह व्रतों के साठ अतीचार हो जाते हैं। सम्यग्दर्शन और सल्लेखना के पांच पांच अतीचार तो श्रावक और संयमी दोनों व्रतियों के संभव जाते हैं ।
अतीचारा इत्यनुवृत्तिः । व्रतग्रहणमेवास्त्विति चेन्न, शीलविशेषद्योतनार्थत्वात् शीलग्रहrt | दिग्विरत्यादीनां हि व्रतलक्षणस्याभिसंधिकृतनियमरूपस्य सद्भावाद् व्रतत्वेऽपि तथाभिधानेऽपि च शीलत्वं प्रकाश्यते, व्रतपरिरक्षणं शीलमिति शीललक्षणोपपत्तेः ।
पूर्व सूत्र से अतीचार इस शब्द की अनुवृत्ति कर ली जाती हैं, यहाँ कोई शंका उठाता है कि सूत्र अत्यन्त लघु होना चाहिये अतः सूत्र में व्रत पद का ही ग्रहण किया जाय दिग्विरति आदिक सात शील भी व्रत ही हैं । तभी तो " व्रतसंपन्नश्च" सूत्रकार ने कहा था । ग्रन्थकार कहते है यह तो न कहना क्योंकि दिग्विरति आदि में शीलपन यानी व्रत परिरक्षकपन की विशेषता का द्योतन करने के लिये शीलपद का ग्रहण किया गया है क्योंकि दिग्विरति आदि शीलों के यद्यपि व्रत के "अभिसंधि अर्थात् विचार पूर्वक चलाकर अभिप्रायों से किये गये प्रतिज्ञात नियम स्वरूप" लक्षण का सद्भाव है अतः शीलों में व्रतपना होते हुये भी सूत्रकार का तिस प्रकार शील रूप से कथन करने में भी कुछ रहस्य है जो कि दिग्विरति आदि में शीलपने का प्रकाश कर रहा है । व्रतों की चारो ओर से रक्षा करने वाला शील होता है । इस प्रकार सातों में शील का लक्षण सुघटित बन रहा है । बात यह है कि आरम्भी, परिग्रही होने से गृहस्थों
व्रतों की रक्षा के लिये शील पालना आवश्यक है मुनियों के नहीं। तभी तो तीर्थ यात्रा के लिये दिग्विरतिया देश व्रत के नियमों की अपेक्षा नहीं की जाती है अथवा गृहस्थ के तीसरी, दूसरी प्रतिमाओं में