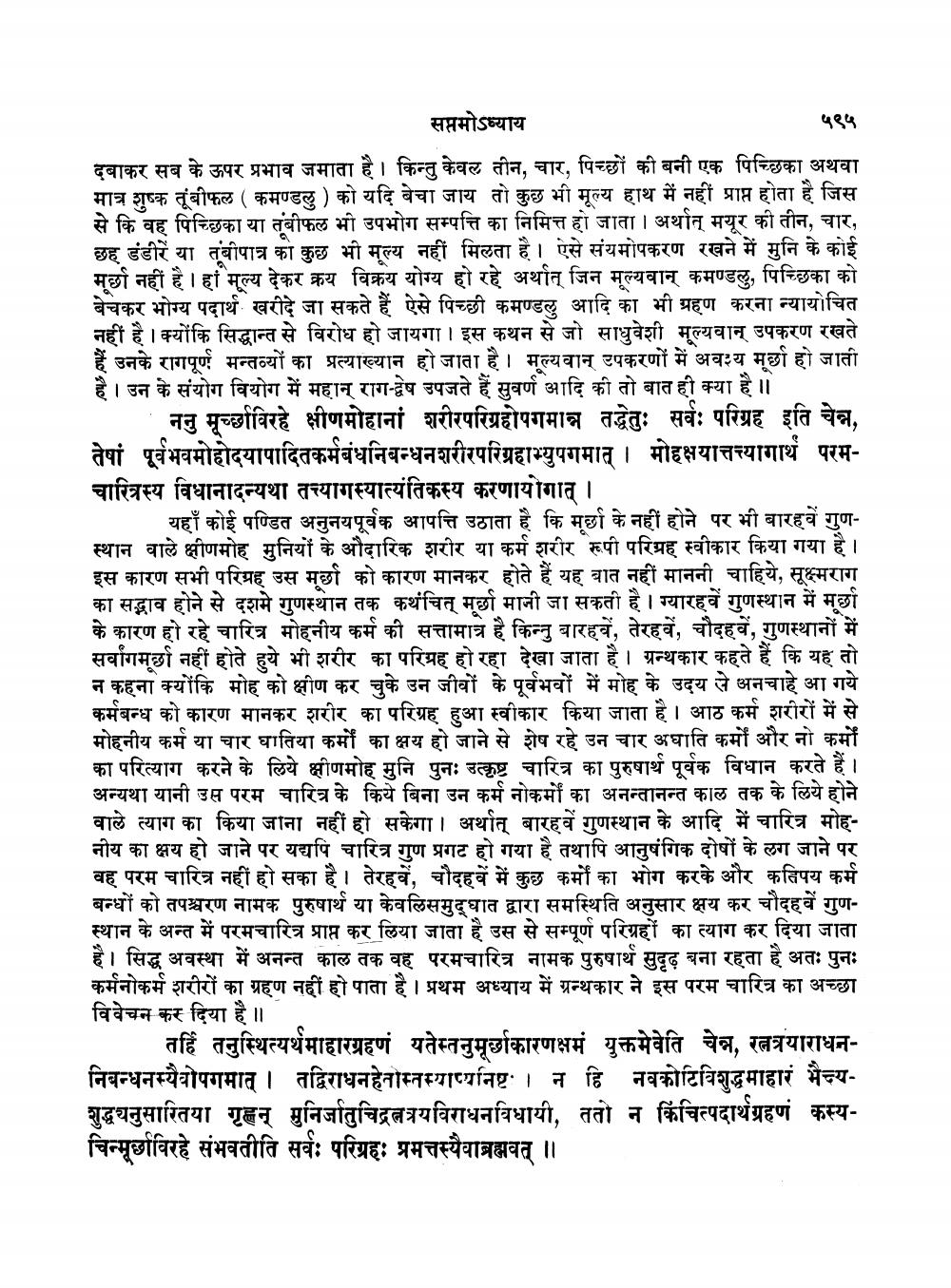________________
सप्तमोऽध्याय
५९५
दबाकर सब के ऊपर प्रभाव जमाता है । किन्तु केवल तीन, चार, पिच्छों की बनी एक पिच्छिका अथवा मात्र शुष्क तूंबीफल ( कमण्डलु ) को यदि बेचा जाय तो कुछ भी मूल्य हाथ में नहीं प्राप्त होता है जिस से कि वह पिच्छिका या तूंबीफल भी उपभोग सम्पत्ति का निमित्त हो जाता । अर्थात् मयूर की तीन, चार, छह डंडीरें या तंबीपात्र को कुछ भी मूल्य नहीं मिलता है। ऐसे संयमोपकरण रखने में मुनि के कोई मूर्छा नहीं है। मूल्य देकर क्रय विक्रय योग्य हो रहे अर्थात् जिन मूल्यवान् कमण्डलु, पिच्छिका को बेचकर भोग्य पदार्थ खरीदे जा सकते हैं ऐसे पिच्छी कमण्डलु आदि का भी ग्रहण करना न्यायोचित नहीं है । क्योंकि सिद्धान्त से विरोध हो जायगा । इस कथन से जो साधुवेशी मूल्यवान् उपकरण रखते हैं उनके रागपूर्ण मन्तव्यों का प्रत्याख्यान हो जाता है । मूल्यवान उपकरणों में अवश्य मूर्छा हो जाती है । उन के संयोग वियोग में महान् राग-द्वेष उपजते हैं सुवर्ण आदि की तो बात ही क्या है ॥
ननु मूर्च्छाविरहे क्षीणमोहानां शरीरपरिग्रहोपगमान्न तद्धेतुः सर्वः परिग्रह इति चेन्न, तेषां पूर्वभवमोहोदयापादितकर्मबंधनिबन्धनशरीरपरिग्रहाभ्युपगमात् । मोहक्षयात्तत्त्यागार्थं परमचारित्रस्य विधानादन्यथा तत्त्यागस्यात्यंतिकस्य करणायोगात् ।
यहाँ कोई पण्डित अनुनयपूर्वक आपत्ति उठाता है कि मूर्छा के नहीं होने पर भी बारहवें गुणस्थान वाले क्षीणमोह मुनियों के औदारिक शरीर या कर्म शरीर रूपी परिग्रह स्वीकार किया गया है। इस कारण सभी परिग्रह उस मूर्छा को कारण मानकर होते हैं यह बात नहीं माननी चाहिये, सूक्ष्मराग का सद्भाव होने से दशमे गुणस्थान तक कथंचित् मूर्छा मानी जा सकती है। ग्यारहवें गुणस्थान में मूर्छा के कारण हो रहे चारित्र मोहनीय कर्म की सत्तामात्र है किन्तु बारहवें, तेरहवें, चौदहवें, गुणस्थानों में सर्वांगमूर्छा नहीं होते हुये भी शरीर का परिग्रह हो रहा देखा जाता है । ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो
कहना क्योंकि मोह को क्षीण कर चुके उन जीवों के पूर्वभवों में मोह के उदय से अनचाहे आ गये कर्मबन्धको कारण मानकर शरीर का परिग्रह हुआ स्वीकार किया जाता है । आठ कर्म शरीरों में से मोहनीय कर्म या चार घातिया कर्मों का क्षय हो जाने से शेष रहे उन चार अघाति कर्मों और नो कर्मों का परित्याग करने के लिये क्षीणमोह मुनि पुनः उत्कृष्ट चारित्र का पुरुषार्थ पूर्वक विधान करते हैं । अन्यथा यानी उस परम चारित्र के किये बिना उन कर्म नोकर्मों का अनन्तानन्त काल तक के लिये होने वाले त्याग का किया जाना नहीं हो सकेगा । अर्थात् बारहवें गुणस्थान के आदि में चारित्र मोह - नी का क्षय हो जाने पर यद्यपि चारित्र गुण प्रगट हो गया है तथापि आनुषंगिक दोषों के लग जाने पर वह परम चारित्र नहीं हो सका है। तेरहवें, चौदहवें में कुछ कर्मों का भोग करके और कतिपय कर्म बन्धों को तपश्चरण नामक पुरुषार्थ या केवलिसमुद्घात द्वारा समस्थिति अनुसार क्षय कर चौदहवें गुणस्थान के अन्त में परमचारित्र प्राप्त कर लिया जाता है उस से सम्पूर्ण परिग्रहों का त्याग कर दिया जाता है । सिद्ध अवस्था में अनन्त काल तक वह परमचारित्र नामक पुरुषार्थं सुदृढ़ बना रहता है अतः पुनः कर्म नोकर्म शरीरों का ग्रहण नहीं हो पाता है । प्रथम अध्याय में ग्रन्थकार ने इस परम चारित्र का अच्छा विवेचन कर दिया है ॥
तर्हि तनुस्थित्यर्थमाहारग्रहणं यतेस्तनुमूर्छाकारणक्षमं युक्तमेवेति चेन्न, रत्नत्रयाराधननिबन्धनस्यैवोपगमात् । तद्विराधनहेतोस्तस्याप्यनिष्ट । न हि नवकोटिविशुद्ध माहारं भैच्यशुद्धयनुसारितया गृह्णन् मुनिर्जातुचिद्रत्नत्रय विराधनविधायी, ततो न किंचित्पदार्थग्रहणं कस्यचिन्मूर्छाविरहे संभवतीति सर्वः परिग्रहः प्रमत्तस्यैवाब्रह्मवत् ।