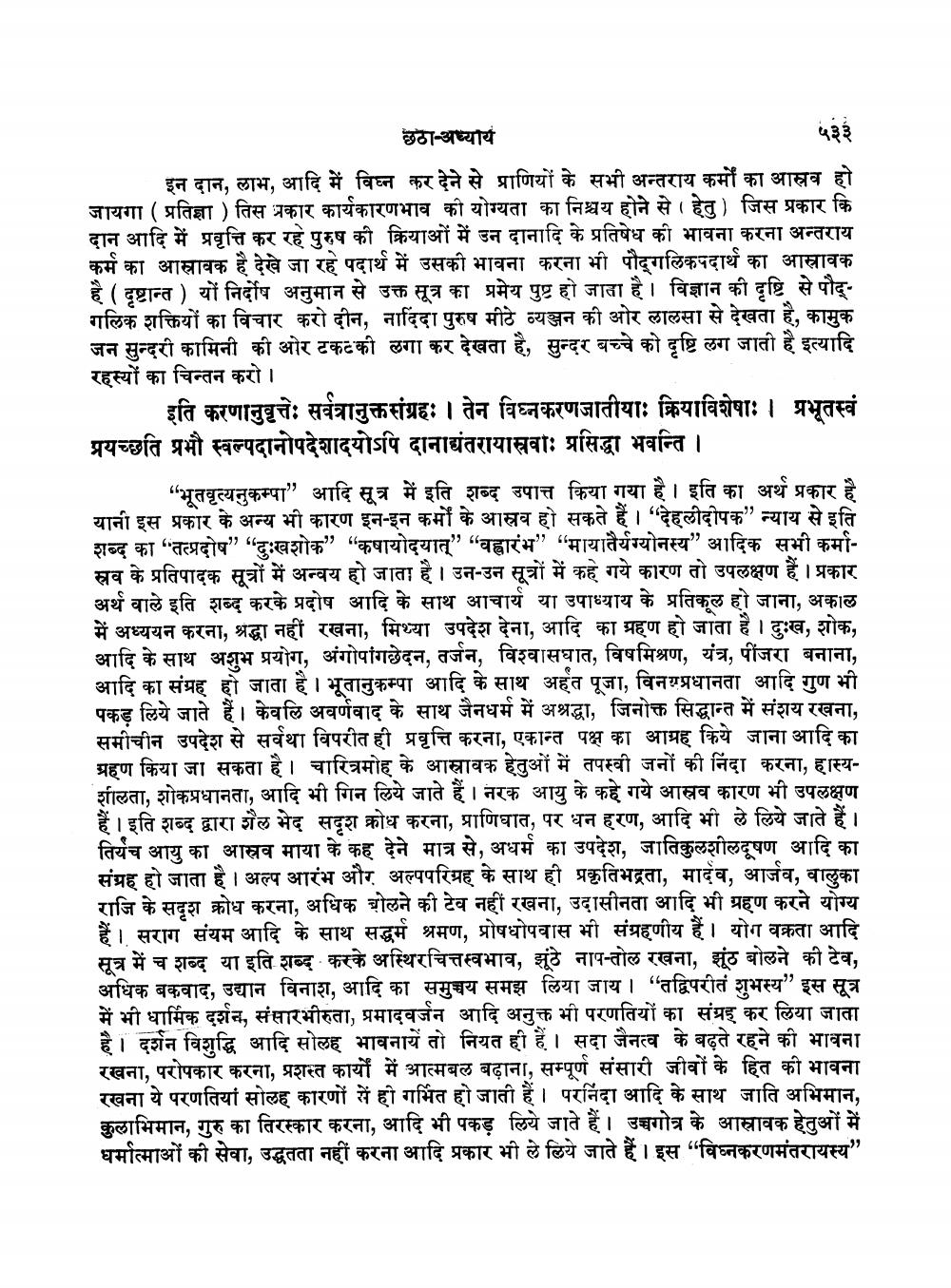________________
छठा अध्याय
५३३
इन दान, लाभ, आदि में विघ्न कर देने से प्राणियों के सभी अन्तराय कर्मों का आस्रव हो जायगा ( प्रतिज्ञा ) तिस प्रकार कार्यकारणभाव की योग्यता का निश्चय होने से । हेतु) जिस प्रकार कि दान आदि में प्रवृत्ति कर रहे पुरुष की क्रियाओं में उन दानादि के प्रतिषेध की भावना करना अन्तराय कर्म का आस्रावक है देखे जा रहे पदार्थ में उसकी भावना करना भी पौद्गलिकपदार्थ का आस्रावक है ( दृष्टान्त ) यों निर्दोष अनुमान से उक्त सूत्र का प्रमेय पुष्ट हो जाता है। विज्ञान की दृष्टि से पौद्गलिक शक्तियों का विचार करो दीन, नादिदा पुरुष मीठे व्यञ्जन की ओर लालसा से देखता है, कामुक जन सुन्दरी कामिनी की ओर टकटकी लगा कर देखता है, सुन्दर बच्चे को दृष्टि लग जाती है इत्यादि रहस्यों का चिन्तन करो ।
इति करणानुवृत्तेः सर्वत्रानुक्तसंग्रहः । तेन विघ्नकरणजातीयाः क्रियाविशेषाः । प्रभूतस्वं प्रयच्छति प्रभौ स्वल्पदानोपदेशादयोऽपि दानाद्यंतरायास्रवाः प्रसिद्धा भवन्ति ।
"भूतवृत्यनुकम्पा” आदि सूत्र में इति शब्द उपात्त किया गया है । इति का अर्थ प्रकार है। यानी इस प्रकार के अन्य भी कारण इन-इन कर्मों के आस्रव हो सकते हैं । " देहलीदीपक" न्याय से इति शब्द का " तत्प्रदोष" "दुःखशोक" “कषायोदयात्" "वहारंभ" "मायातैर्यग्योनस्य" आदिक सभी कर्मास्रव के प्रतिपादक सूत्रों में अन्वय हो जाता है । उन-उन सूत्रों में कहे गये कारण तो उपलक्षण हैं । प्रकार अर्थ वाले इति शब्द करके प्रदोष आदि के साथ आचार्य या उपाध्याय के प्रतिकूल हो जाना, अकाल में अध्ययन करना, श्रद्धा नहीं रखना, मिथ्या उपदेश देना, आदि का ग्रहण हो जाता है । दुःख, शोक, आदि के साथ अशुभ प्रयोग, अंगोपांगछेदन, तर्जन, विश्वासघात, विषमिश्रण, यंत्र, पींजरा बनाना, आदि का संग्रह हो जाता है । भूतानुकम्पा आदि के साथ अर्हत पूजा, विनयप्रधानता आदि गुण भी पकड़ लिये जाते हैं । केवलि अवर्णवाद के साथ जैनधर्म में अश्रद्धा, जिनोक्त सिद्धान्त में संशय रखना, समीचीन उपदेश से सर्वथा विपरीत ही प्रवृत्ति करना, एकान्त पक्ष का आग्रह किये जाना आदि का ग्रहण किया जा सकता है । चारित्रमोह के आस्रावक हेतुओं में तपस्वी जनों की निंदा करना, हास्यशीलता, शोकप्रधानता, आदि भी गिन लिये जाते हैं। नरक आयु के कहे गये आस्रव कारण भी उपलक्षण हैं । इति शब्द द्वारा शैल भेद सदृश क्रोध करना, प्राणिघात पर धन हरण, आदि भी ले लिये जाते हैं । तिर्यंच आयु का आस्रव माया के कह देने मात्र से, अधर्म का उपदेश, जातिकुलशीलदूषण आदि का संग्रह हो जाता है । अल्प आरंभ और अल्पपरिग्रह के साथ ही प्रकृतिभद्रता, मार्दव, आर्जव, वालुका राज के सदृश क्रोध करना, अधिक बोलने की टेव नहीं रखना, उदासीनता आदि भी ग्रहण करने योग्य हैं। सराग संयम आदि के साथ सद्धर्म श्रमण, प्रोषधोपवास भी संग्रहणीय हैं। योग वक्रता आदि सूत्र में च शब्द या इति शब्द करके अस्थिरचित्तस्वभाव, झूठे नाप-तोल रखना, झूठ बोलने की देव, अधिक बकवाद, उद्यान विनाश, आदि का समुच्चय समझ लिया जाय । " तद्विपरीतं शुभस्य" इस सूत्र में भी धार्मिक दर्शन, संसारभीरुता, प्रमादवर्जन आदि अनुक्त भी परणतियों का संग्रह कर लिया जाता है | दर्शन विशुद्ध आदि सोलह भावनायें तो नियत ही हैं । सदा जैनत्व के बढ़ते रहने की भावना रखना, परोपकार करना, प्रशस्त कार्यों में आत्मबल बढ़ाना, सम्पूर्ण संसारी जीवों के हित की भावना रखना ये परणतियां सोलह कारणों से हो गर्भित हो जाती हैं। परनिंदा आदि के साथ जाति अभिमान, कुलाभिमान, गुरु का तिरस्कार करना, आदि भी पकड़ लिये जाते हैं । उच्चगोत्र के आस्रावक हेतुओं में धर्मात्माओं की सेवा, उद्धतता नहीं करना आदि प्रकार भी ले लिये जाते हैं। इस "विघ्नकरणमंतरायस्य "