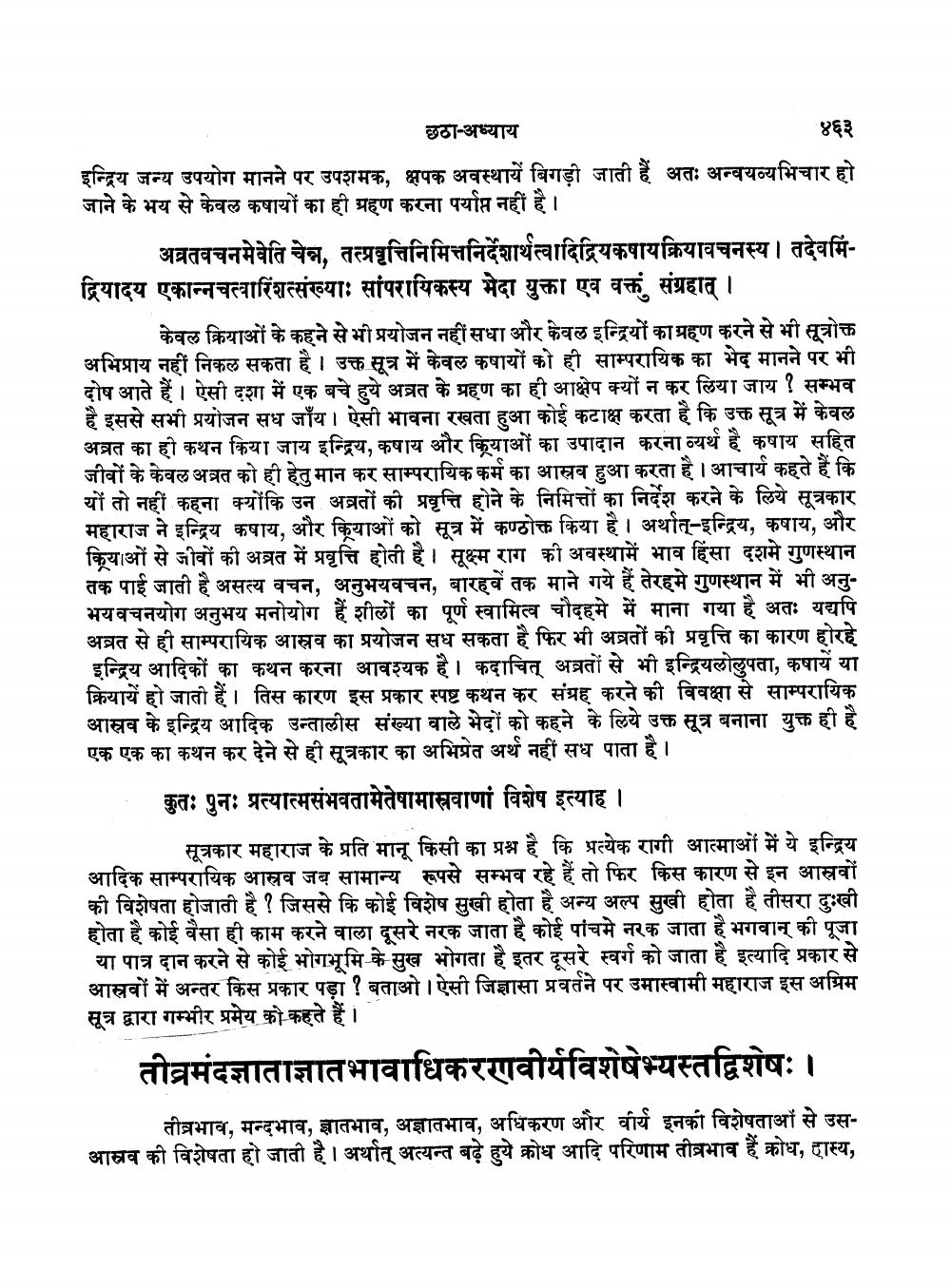________________
छठा अध्याय
४६३
इन्द्रियजन्य उपयोग मानने पर उपशमक, क्षपक अवस्थायें बिगड़ी जाती हैं अतः अन्वयव्यभिचार हो जाने के भय से केवल कषायों का ही ग्रहण करना पर्याप्त नहीं है ।
अत्रतवचनमेवेति चेन्न, तत्प्रवृत्तिनिमित्तनिर्देशार्थत्वादिद्रिय कषाय क्रियावचनस्य । तदेवमिंद्रियादय एकान्नचत्वारिंशत्संख्याः सांपरायिकस्य भेदा युक्ता एव वक्तुं संग्रहात् ।
केवल क्रियाओं के कहने से भी प्रयोजन नहीं सधा और केवल इन्द्रियों का ग्रहण करने से भी सूत्रोक्त अभिप्राय नहीं निकल सकता है। उक्त सूत्र में केवल कषायों को ही साम्परायिक का भेद मानने पर भी दोष आते हैं। ऐसी दशा में एक बचे हुये अव्रत के ग्रहण का ही आक्षेप क्यों न कर लिया जाय ? सम्भव है इससे सभी प्रयोजन सध जाँय । ऐसी भावना रखता हुआ कोई कटाक्ष करता है कि उक्त सूत्र में केवल अव्रत का ही कथन किया जाय इन्द्रिय, कषाय और क्रियाओं का उपादान करना व्यर्थ है कषाय सहित जीवों के केवल अव्रत को ही हेतु मान कर साम्परायिक कर्म का आस्रव हुआ करता है । आचार्य कहते हैं कि यों तो नहीं कहना क्योंकि उन अव्रतों की प्रवृत्ति होने के निमित्तों का निर्देश करने के लिये सूत्रकार महाराज ने इन्द्रिय कषाय, और क्रियाओं को सूत्र में कण्ठोक्त किया है । अर्थात्-इन्द्रिय, कषाय, और क्रियाओं से जीवों की अव्रत में प्रवृत्ति होती है। सूक्ष्म राग की अवस्थामें भाव हिंसा दशमे गुणस्थान तक पाई जाती है असत्य वचन, अनुभयवचन, बारहवें तक माने गये हैं तेरहमे गुणस्थान में भी अनुभयवचनयोग अनुभय मनोयोग हैं शीलों का पूर्ण स्वामित्व चौदहमे में माना गया है अतः यद्यपि अत से ही साम्परायिक आस्रव का प्रयोजन सध सकता है फिर भी अत्रतों की प्रवृत्ति का कारण होरहे इन्द्र आदिकों का कथन करना आवश्यक है । कदाचित् अत्रतों से भी इन्द्रियलोलुपता, कषायें या क्रियायें हो जाती हैं । तिस कारण इस प्रकार स्पष्ट कथन कर संग्रह करने की विवक्षा से साम्परायिक आस्रव के इन्द्रिय आदिक उन्तालीस संख्या वाले भेदों को कहने के लिये उक्त सूत्र बनाना युक्त ही है एक एक का कथन कर देने से ही सूत्रकार का अभिप्रेत अर्थ नहीं सघ पाता है ।
कुतः पुनः प्रत्यात्मसंभवतामेतेषामात्रवाणां विशेष इत्याह ।
सूत्रकार महाराज के प्रति मानू किसी का प्रश्न है कि प्रत्येक रागी आत्माओं में ये इन्द्रिय आदि साम्परायिक आस्रव जब सामान्य रूपसे सम्भव रहे हैं तो फिर किस कारण से इन आस्रवों की विशेषता होजाती है ? जिससे कि कोई विशेष सुखी होता है अन्य अल्प सुखी होता है तीसरा दुःखी होता है कोई वैसा ही काम करने वाला दूसरे नरक जाता है कोई पांचमे नरक जाता है भगवान् की पूजा या पात्र दान करने से कोई भोगभूमि के सुख भोगता है इतर दूसरे स्वर्ग को जाता है इत्यादि प्रकार से आस्रवों में अन्तर किस प्रकार पड़ा ? बताओ। ऐसी जिज्ञासा प्रवर्तने पर उमास्वामी महाराज इस अग्रिम सूत्र द्वारा गम्भीर प्रमेय को कहते हैं ।
तीव्रमंदज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्यविशेषेभ्यस्तद्विशेषः ।
तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातभाव, अज्ञातभाव, अधिकरण और वीर्य इनकी विशेषताओं से उसआस्रव की विशेषता हो जाती है । अर्थात् अत्यन्त बढ़े हुये क्रोध आदि परिणाम तीव्रभाव हैं क्रोध, हास्य,