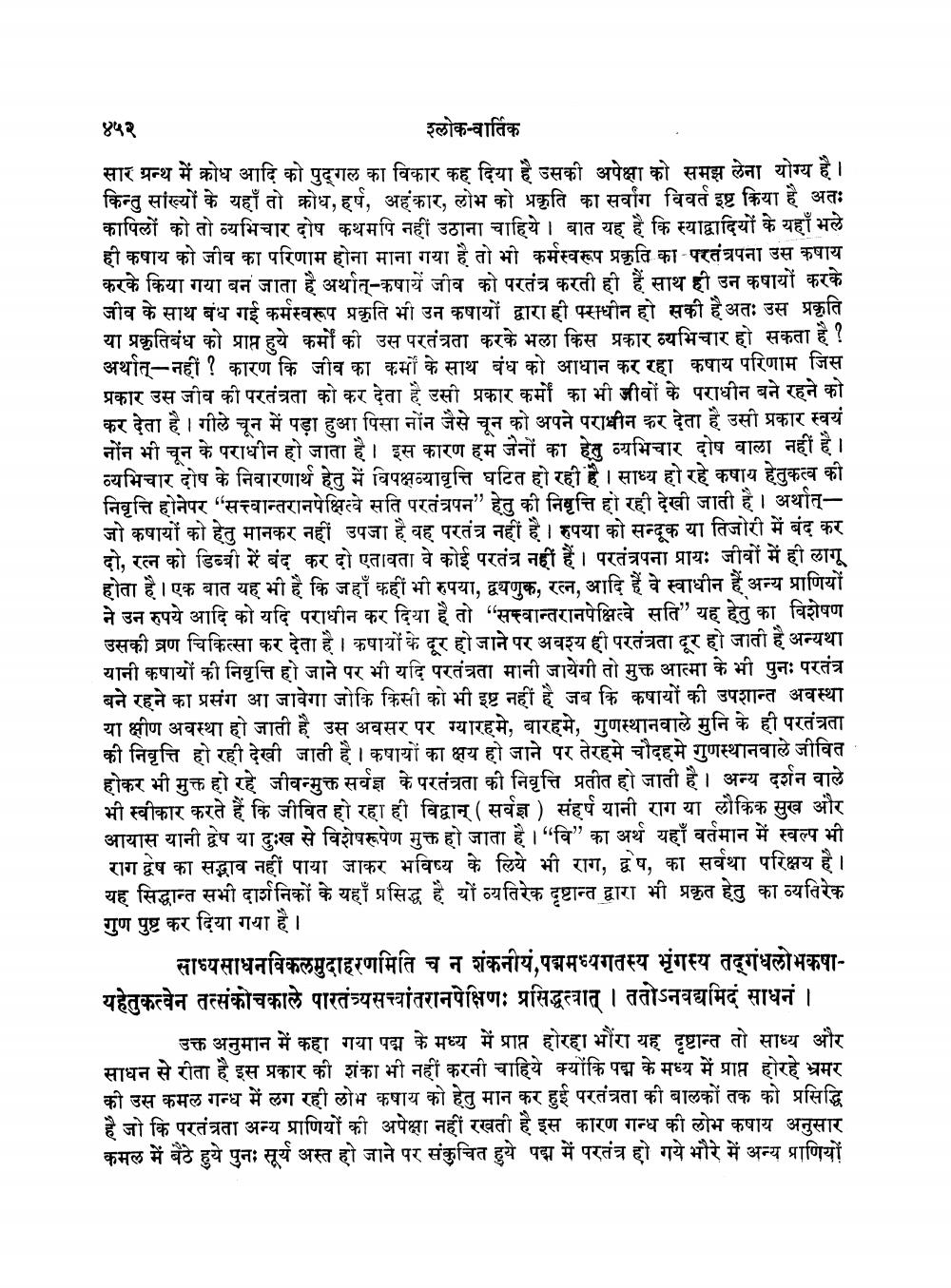________________
४५२
श्लोक-वार्तिक
सार ग्रन्थ में क्रोध आदि को पुद्गल का विकार कह दिया है उसकी अपेक्षा को समझ लेना योग्य है । किन्तु सांख्यों के यहाँ तो क्रोध, हर्ष, अहंकार, लोभ को प्रकृति का सर्वांग विवर्त इष्ट किया है अतः कापिलों को तो व्यभिचार दोष कथमपि नहीं उठाना चाहिये। बात यह है कि स्याद्वादियों के यहाँ भले ही कषाय को जीव का परिणाम होना माना गया है तो भी कर्मस्वरूप प्रकृति का परतंत्रपना उस कषाय करके किया गया बन जाता है अर्थात् कषायें जीव परतंत्र करती ही हैं साथ ही उन कषायों करके के साथ बंध गई कर्मस्वरूप प्रकृति भी उन कषायों द्वारा ही पसधीन हो सकी है अतः उस प्रकृति या प्रकृतिबंध को प्राप्त हुये कर्मों की उस परतंत्रता करके भला किस प्रकार व्यभिचार हो सकता है ? अर्थात् - नहीं ? कारण कि जीव का कर्मों के साथ बंध को आधान कर रहा कषाय परिणाम जिस प्रकार उस जीव की परतंत्रता को कर देता है उसी प्रकार कर्मों का भी जीवों के पराधीन बने रहने को कर देता है । गीले चून में पड़ा हुआ पिसा नोंन जैसे चून को अपने पराधीन कर देता है उसी प्रकार स्वयं नन भी चून के पराधीन हो जाता है। इस कारण हम जैनों का हेतु व्यभिचार दोष वाला नहीं है । व्यभिचार दोष के निवारणार्थ हेतु में विपक्षव्यावृत्ति घटित हो रही है । साध्य हो रहे कषाय हेतुकत्व की निवृत्ति होनेपर "सत्त्वान्तरानपेक्षित्वे सति परतंत्रपन" हेतु की निवृत्ति हो रही देखी जाती है । अर्थात्जो कषायों को हेतु मानकर नहीं उपजा है वह परतंत्र नहीं है। रुपया को सन्दूक या तिजोरी में बंद कर दो, रत्न को डिब्बी में बंद कर दो एतावता वे कोई परतंत्र नहीं हैं। परतंत्रपना प्रायः जीवों में ही लागू होता है। एक बात यह भी है कि जहाँ कहीं भी रुपया द्वयणुक, रत्न, आदि हैं वे स्वाधीन हैं अन्य प्राणियों ने उन रुपये आदि को यदि पराधीन कर दिया है तो "सस्वान्तरानपेक्षित्वे सति" यह हेतु का विशेषण उसकी व्रण चिकित्सा कर देता है । कषायों के दूर हो जाने पर अवश्य ही परतंत्रता दूर हो जाती है अन्यथा यानी कषायों की निवृत्ति हो जाने पर भी यदि परतंत्रता मानी जायेगी तो मुक्त आत्मा के भी पुनः परतंत्र बने रहने का प्रसंग आ जावेगा जोकि किसी को भी इष्ट नहीं है जब कि कषायों की उपशान्त अवस्था या क्षीण अवस्था हो जाती है उस अवसर पर ग्यारहमे, बारहमे, गुणस्थानवाले मुनि के ही परतंत्रता की निवृत्ति हो रही देखी जाती है। कषायों का क्षय हो जाने पर तेरह मे चौदह मे गुणस्थानवाले जीवित होकर भी मुक्त हो रहे जीवन्मुक्त सर्वज्ञ के परतंत्रता की निवृत्ति प्रतीत हो जाती है । अन्य दर्शन वाले भी स्वीकार करते हैं कि जीवित हो रहा ही विद्वान् ( सर्वज्ञ ) संहर्ष यानी राग या लौकिक सुख और आयास यानी द्वेष या दुःख से विशेषरूपेण मुक्त हो जाता है। "वि" का अर्थ यहाँ वर्तमान में स्वल्प भी राग द्वेष का सद्भाव नहीं पाया जाकर भविष्य के लिये भी राग, द्वेष, का सर्वथा परिक्षय है । यह सिद्धान्त सभी दार्शनिकों के यहाँ प्रसिद्ध है यों व्यतिरेक दृष्टान्त द्वारा भी प्रकृत हेतु का व्यतिरेक गुण पुष्ट कर दिया गया है।
1
उक्त अनुमान
साध्यसाधनविकलमुदाहरणमिति च न शंकनीयं पद्ममध्यगतस्य भृंगस्य तद्गंधलोभकषायहेतुकत्वेन तत्संकोचकाले पारतंत्र्य सच्चांतरानपेक्षिणः प्रसिद्धत्वात् । ततोऽनवद्यमिदं साधनं । कहा गया पद्म के मध्य में प्राप्त होरहा भौंरा यह दृष्टान्त तो साध्य और साधन से रीता है इस प्रकार की शंका भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि पद्म के मध्य में प्राप्त होरहे भ्रमर की उस कमल गन्ध में लग रही लोभ कषाय को हेतु मान कर हुई परतंत्रता की बालकों तक को प्रसिद्धि है जो कि परतंत्रता अन्य प्राणियों की अपेक्षा नहीं रखती है इस कारण गन्ध की लोभ कषाय अनुसार कमल में बैठे हुये पुनः सूर्य अस्त हो जाने पर संकुचित हुये पद्म में परतंत्र हो गये भौरे में अन्य प्राणियों