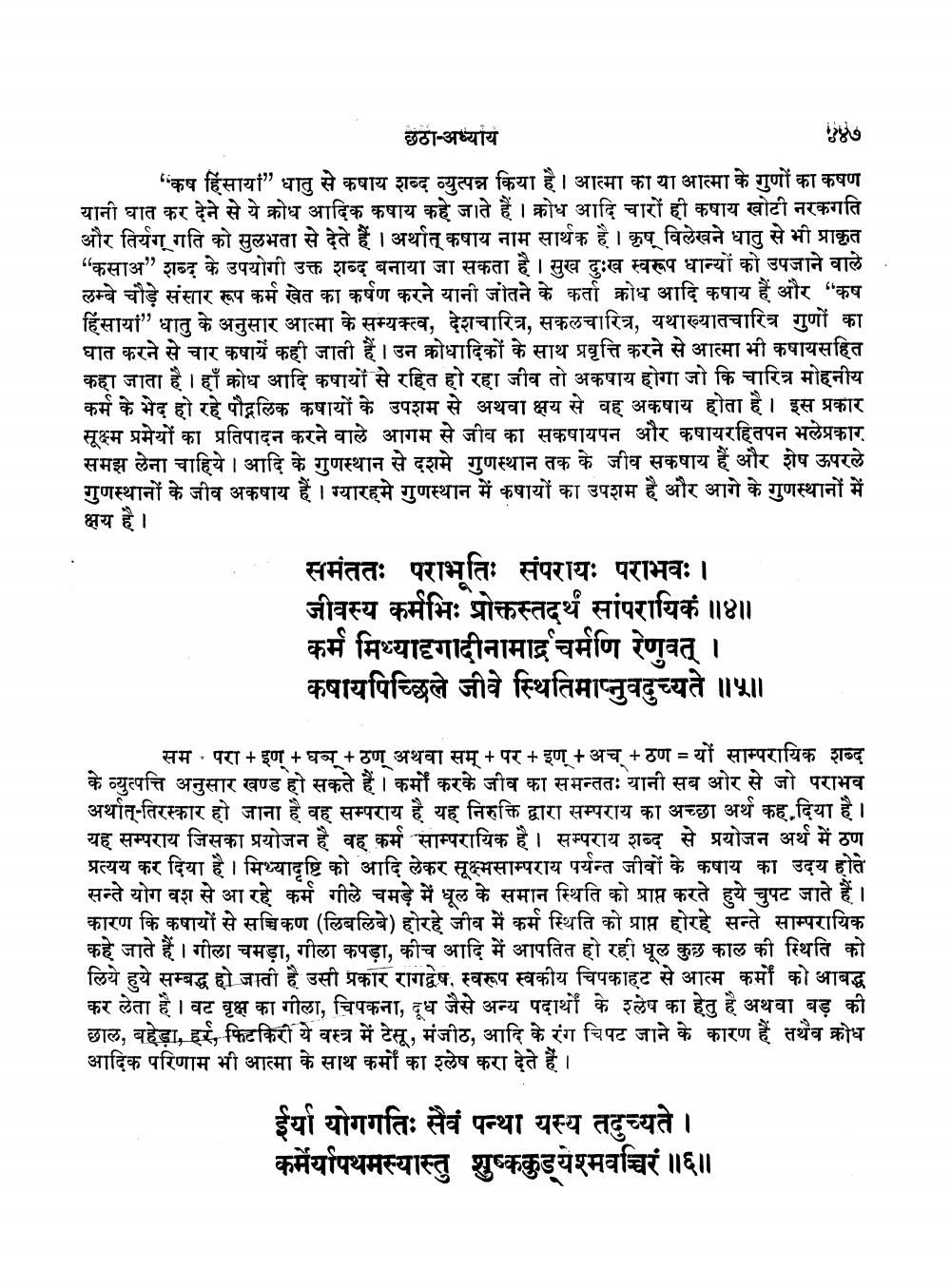________________
छठा अध्याय
૪૭
"कष हिंसाया" धातु से कषाय शब्द व्युत्पन्न किया है । आत्मा का या आत्मा के गुणों का कषण यानी घात कर देने से ये क्रोध आदिक कषाय कहे जाते हैं । क्रोध आदि चारों ही कषाय खोटी नरकगति और तिर्यग गति को सुलभता से देते हैं । अर्थात् कषाय नाम सार्थक है । कृष विलेखने धातु से भी प्राकृत "कसाअ" शब्द 'के उपयोगी उक्त शब्द बनाया जा सकता है। सुख दुःख स्वरूप धान्यों को उपजाने वाले लम्बे चौड़े संसार रूप कर्म खेत का कर्षण करने यानी जोतने के कर्ता क्रोध आदि कषाय हैं और " कष हिंसायां” धातु के अनुसार आत्मा के सम्यक्त्व, देशचारित्र, सकलचारित्र, यथाख्यातचारित्र गुणों का घात करने से चार कषायें कही जाती हैं। उन क्रोधादिकों के साथ प्रवृत्ति करने से आत्मा भी कषायसहित कहा जाता है । हाँ क्रोध आदि कषायों से रहित हो रहा जीव तो अकषाय होगा जो कि चारित्र मोहनीय कर्म के भेद हो रहे पौगलिक कषायों के उपशम से अथवा क्षय से वह अकषाय होता है । इस प्रकार सूक्ष्म प्रमेयों का प्रतिपादन करने वाले आगम से जीव का सकषायपन और कषायरहितपन भलेप्रकार समझ लेना चाहिये | आदि के गुणस्थान से दशमे गुणस्थान तक के जीव सकषाय हैं और शेष ऊपरले गुणस्थानों के जीव अकषाय हैं । ग्यारहमे गुणस्थान में कषायों का उपशम है और आगे के गुणस्थानों में है।
समंततः पराभूतिः संपरायः पराभवः । जीवस्य कर्मभिः प्रोक्तस्तदर्थं सांपरायिकं ॥ ४ ॥ कर्म मियागादीनामाद्र' चर्मणि रेणुवत् । कषायपिच्छिले जीवे स्थितिमाप्नुवदुच्यते ॥५॥
सम परा + इ + घञ् + ठण् अथवा सम् + पर + इण् + अच् + ठण = यों साम्परायिक शब्द के व्युत्पत्ति अनुसार खण्ड हो सकते हैं। कर्मों करके जीव का समन्ततः यानी सब ओर से जो पराभव अर्थात्-तिरस्कार हो जाना है वह सम्पराय है यह निरुक्ति द्वारा सम्पराय का अच्छा अर्थ कह दिया है । यह सम्पराय जिसका प्रयोजन है वह कर्म साम्परायिक है । सम्पराय शब्द से प्रयोजन अर्थ में ठण प्रत्यय कर दिया है । मिथ्यादृष्टि को आदि लेकर सूक्ष्मसाम्पराय पर्यन्त जीवों के कषाय का उदय होते सन्ते योग वश से आ रहे कर्म गीले चमड़े में धूल के समान स्थिति को प्राप्त करते हुये चुपट जाते हैं । कारण कि कषायों से सच्चिकण (लिबलिबे) होरहे जीव में कर्म स्थिति को प्राप्त होरहे सन्ते साम्परायिक कहे जाते हैं। गीला चमड़ा, गीला कपड़ा, कीच आदि में आपतित हो रही धूल कुछ काल की स्थिति को लिये हुये सम्बद्ध हो जाती है उसी प्रकार रागद्वेष, स्वरूप स्वकीय चिपकाहट से आत्म कर्मों को आबद्ध कर लेता है | वट वृक्ष का गीला, चिपकना, दूध जैसे अन्य पदार्थों के श्लेष का हेतु है अथवा बड़ की छाल, बहेड़ा, हर्र, फिटकिरी ये वस्त्र में टेसू, मंजीठ, आदि के रंग चिपट जाने के कारण हैं तथैव क्रोध आदिक परिणाम भी आत्मा के साथ कर्मों का श्लेष करा देते हैं ।
ईर्या योगगतिः सैवं पन्था यस्य तदुच्यते । कर्मेर्यापथमस्यास्तु शुष्ककुड्येश्मवच्चिरं ॥ ६ ॥