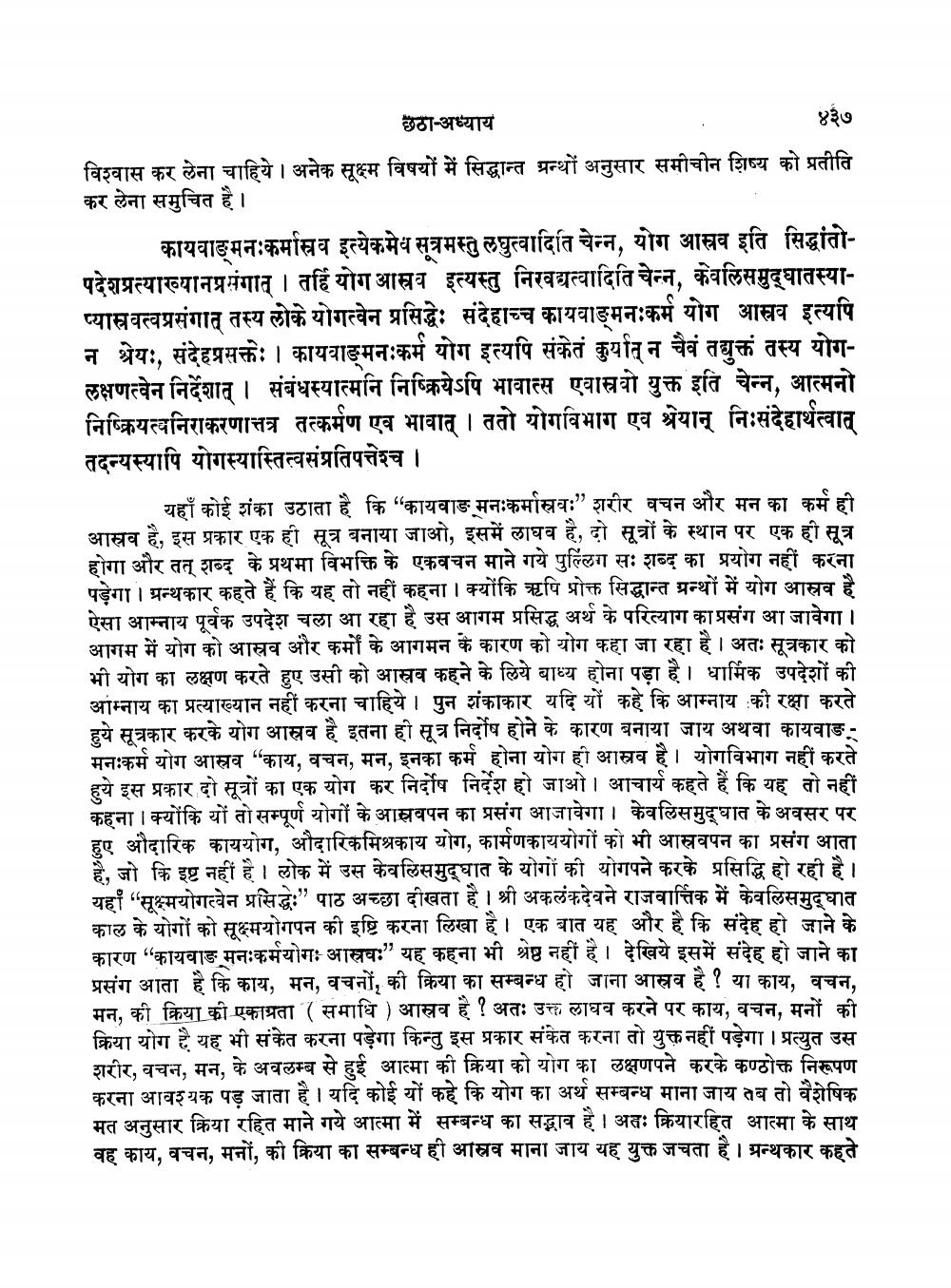________________
छठा अध्याय ४३७ विश्वास कर लेना चाहिये । अनेक सूक्ष्म विषयों में सिद्धान्त ग्रन्थों अनुसार समीचीन शिष्य को प्रतीति कर लेना समुचित है ।
कायवाङ्मनःकर्मास्रव इत्येकमेव सूत्रमस्तु लघुत्वादिति चेन्न, योग आस्रव इति सिद्धांतोपदेशप्रत्याख्यानप्रसंगात् । तर्हि योग आस्रव इत्यस्तु निरवद्यत्वादिति चेन्न, केवलिसमुद्घातस्याप्यास्रवत्वप्रसंगात् तस्य लोके योगत्वेन प्रसिद्धेः संदेहाच्च कायवाङ्मनःकर्म योग आस्रव इत्यपि न श्रेयः, संदेहप्रसक्तेः । कायवाङ्मनः कर्म योग इत्यपि संकेतं कुर्यात् न चैवं तद्युक्तं तस्य योगलक्षणत्वेन निर्देशात् । संबंधस्यात्मनि निष्क्रियेऽपि भावात्स एवास्रवो युक्त इति चेन्न, आत्मनो निष्क्रियत्वनिराकरणात्तत्र तत्कर्मण एव भावात् । ततो योगविभाग एव श्रेयान् निःसंदेहार्थत्वात् तदन्यस्यापि योगस्यास्तित्वसंप्रतिपत्तेश्च ।
यहाँ कोई शंका उठाता है कि “कायवाङ मनःकर्मास्रवः " शरीर वचन और मन का कर्म ही आस्रव है, इस प्रकार एक ही सूत्र बनाया जाओ, इसमें लाघव है, दो सूत्रों के स्थान पर एक ही सूत्र होगा और तत् शब्द के प्रथमा विभक्ति के एकवचन माने गये पुल्लिंग सः शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना । क्योंकि ऋषि प्रोक्त सिद्धान्त ग्रन्थों में योग आस्रव है ऐसा आम्नाय पूर्वक उपदेश चला आ रहा है उस आगम प्रसिद्ध अर्थ के परित्याग का प्रसंग आ जावेगा । आगम में योग को आस्रव और कर्मों के आगमन के कारण को योग कहा जा रहा है। अतः सूत्रकार को भी योग का लक्षण करते हुए उसी को आस्रव कहने के लिये बाध्य होना पड़ा है। धार्मिक उपदेशों की आम्नाय का प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिये । पुन शंकाकार यदि यों कहे कि आम्नाय की रक्षा करते हुये सूत्रकार करके योग आस्रव है इतना ही सूत्र निर्दोष होने के कारण बनाया जाय अथवा कायवाङ - मनःकर्म योग आस्रव "काय, वचन, मन, इनका कर्म होना योग ही आस्रव है। योगविभाग नहीं करते हुये इस प्रकार दो सूत्रों का एक योग कर निर्दोष निर्देश हो जाओ । आचार्य कहते हैं कि यह तो नहीं कहना | क्योंकि यों तो सम्पूर्ण योगों के आस्रवपन का प्रसंग आजावेगा । केवलिसमुद्घात के अवसर पर हुए औदारिक काययोग, औदारिकमिश्रकाय योग, कार्मणकाययोगों को भी आस्रवपन का प्रसंग आता है, जो कि इष्ट नहीं है । लोक में उस केवलिसमुद्घात के योगों की योगपने करके प्रसिद्धि हो रही है । यहाँ “सूक्ष्मयोगत्वेन प्रसिद्धेः " पाठ अच्छा दीखता है। श्री अकलंकदेवने राजवार्त्तिक में केवलिसमुद्घात काल के योगों को सूक्ष्मयोगपन की इष्टि करना लिखा है। एक बात यह और है कि संदेह हो जाने के कारण “कायवाङ मनःकर्मयोगः आस्रवः” यह कहना भी श्रेष्ठ नहीं है । देखिये इसमें संदेह हो जाने का प्रसंग आता है कि काय, मन, वचनों, की क्रिया का सम्बन्ध हो जाना आस्रव है ? या काय, वचन, मन, की क्रिया की एकाग्रता ( समाधि ) आस्रव है ? अतः उक्त लाघव करने पर काय, वचन, मनों की क्रिया योग है यह भी संकेत करना पड़ेगा किन्तु इस प्रकार संकेत करना तो युक्त नहीं पड़ेगा । प्रत्युत उस शरीर, वचन, मन, के अवलम्ब से हुई आत्मा की क्रिया को योग का लक्षणपने करके कण्ठोक्त निरूपण करना आवश्यक पड़ जाता है । यदि कोई यों कहे कि योग का अर्थ सम्बन्ध माना जाय तब तो वैशेषिक मत अनुसार क्रिया रहित माने गये आत्मा में सम्बन्ध का सद्भाव है । अतः क्रियारहित आत्मा के साथ वह काय, वचन, मनों, की क्रिया का सम्बन्ध ही आस्रव माना जाय यह युक्त जचता है । ग्रन्थकार कहते