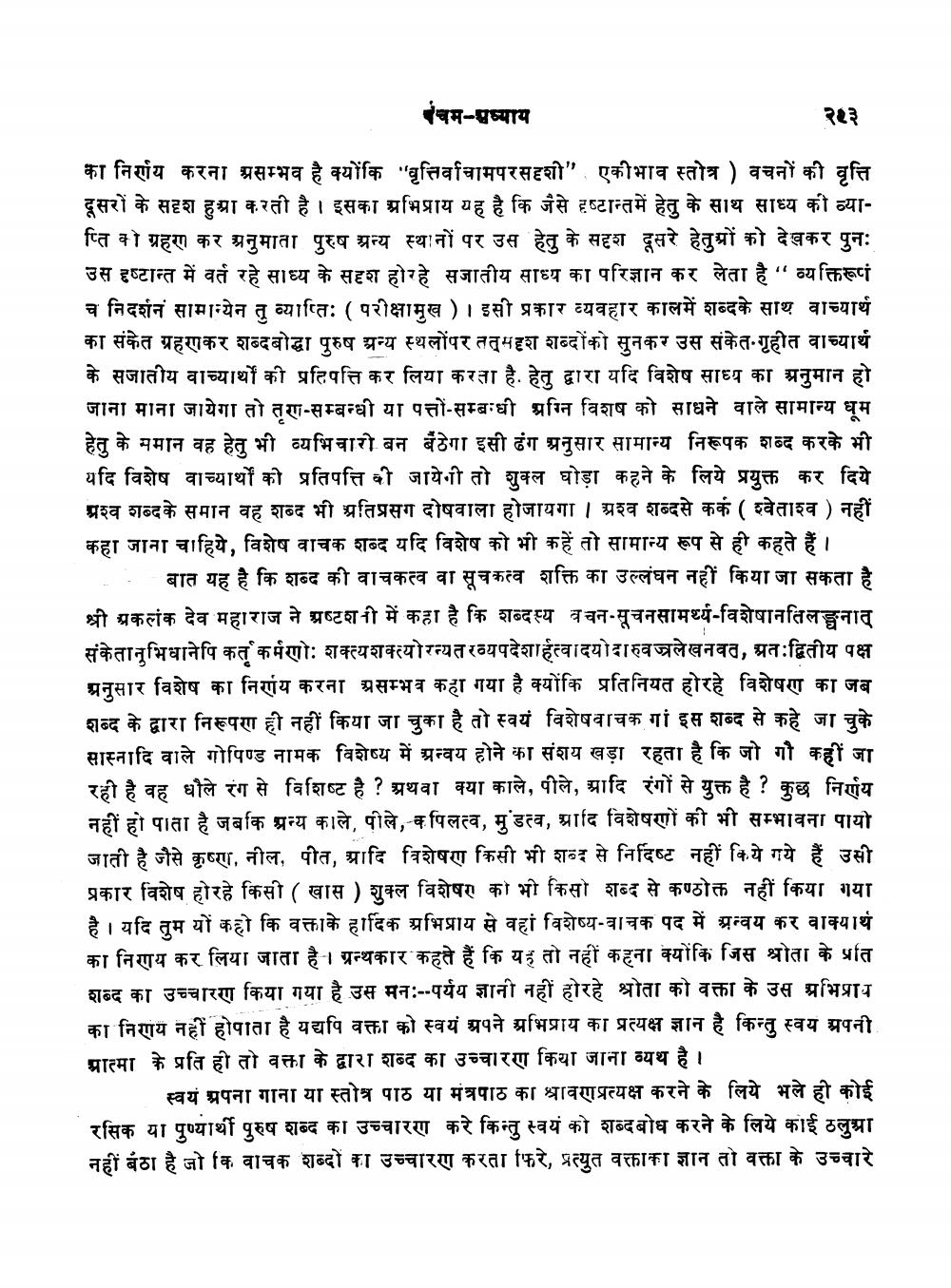________________
पंचम-ध्याय
२९३
निर्णय करना असम्भव है क्योंकि "वृत्तिर्वाचामपरसदृशी" एकीभाव स्तोत्र ) वचनों की वृत्ति दूसरों के सदृश हुआ करती है । इसका अभिप्राय यह है कि जैसे दृष्टान्तमें हेतु के साथ साध्य की व्याप्ति को ग्रहण कर अनुमाता पुरुष अन्य स्थानों पर उस हेतु के सदृश दूसरे हेतुत्रों को देखकर पुनः उस दृष्टान्त में वर्त रहे साध्य के सदृश हो रहे सजातीय साध्य का परिज्ञान कर लेता है " व्यक्तिरूपं च निदर्शनं सामान्येन तु व्याप्ति: ( परीक्षामुख ) । इसी प्रकार व्यवहार कालमें शब्द के साथ वाच्यार्थ का संकेत ग्रहणकर शब्दबोद्धा पुरुष अन्य स्थलोंपर तत्सदृश शब्दों को सुनकर उस संकेत गृहीत वाच्यार्थ के सजातीय वाच्यार्थों की प्रतिपत्ति कर लिया करता है. हेतु द्वारा यदि विशेष साध्य का अनुमान हो जाना माना जायेगा तो तृरण सम्बन्धी या पत्तों सम्बन्धी अग्नि विशेष को साधने वाले सामान्य धूम हेतु के ममान वह हेतु भी व्यभिचारी बन बैठेगा इसी ढंग अनुसार सामान्य निरूपक शब्द करके भी यदि विशेष वाच्यार्थों की प्रतिपत्ति की जायेगी तो शुक्ल घोड़ा कहने के लिये प्रयुक्त कर दिये अश्व शब्द के समान वह शब्द भी प्रतिप्रसग दोषवाला होजायगा । अश्व शब्दसे कर्क ( श्वेताश्व ) नहीं कहा जाना चाहिये, विशेष वाचक शब्द यदि विशेष को भी कहें तो सामान्य रूप से ही कहते हैं ।
बात यह है कि शब्द की वाचकत्व वा सूचकत्व शक्ति का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है श्री अकलंक देव महाराज ने अष्टशनी में कहा है कि शब्दस्य वचन सूचनसामर्थ्य- विशेषानतिलङ्घनात् भाप कर्तृकर्मणोः शक्त्यशक्त्योरन्यतरव्यपदेशार्हत्वादयो दारुवज्रलेखनवत, अतः द्वितीय पक्ष अनुसार विशेष का निर्णय करना असम्भव कहा गया है क्योंकि प्रतिनियत होरहे विशेषण का जब शब्द के द्वारा निरूपण ही नहीं किया जा चुका है तो स्वयं विशेषवाचक गां इस शब्द से कहे जा चुके सास्नादि वाले गोपिण्ड नामक विशेष्य में अन्वय होने का संशय खड़ा रहता है कि जो गौ कहीं जा रही है वह धौले रंग से विशिष्ट है ? अथवा क्या काले, पीले, आदि रंगों से युक्त है ? कुछ निर्णय नहीं हो पाता है जबकि अन्य काले, पीले, कपिलत्व, मुंडत्व, श्रादि विशेषरणों की भी सम्भावना पायो जाती है जैसे कृष्ण, नील, पीत, आदि विशेषण किसी भी शब्द से निर्दिष्ट नहीं किये गये हैं उसी प्रकार विशेष होरहे किसी ( खास ) शुक्ल विशेषण को भी किसो शब्द से कण्ठोक्त नहीं किया गया है | यदि तुम यों कहो कि वक्ताके हार्दिक अभिप्राय से वहां विशेष्य-वाचक पद में अन्वय कर वाक्यार्थ का निणय कर लिया जाता है । ग्रन्थकार कहते हैं कि यह तो नहीं कहना क्योंकि जिस श्रोता के प्रति शब्द का उच्चारण किया गया है उस मनः--पर्यय ज्ञानी नहीं होरहे श्रोता को वक्ता के उस अभिप्राय का निर्णय नहीं हो पाता है यद्यपि वक्ता को स्वयं अपने अभिप्राय का प्रत्यक्ष ज्ञान है किन्तु स्वयं अपनी श्रात्मा के प्रति ही तो वक्ता के द्वारा शब्द का उच्चारण किया जाना व्यथ है ।
स्वयं अपना गाना या स्तोत्र पाठ या मंत्रपाठ का श्रावणप्रत्यक्ष करने के लिये भले ही कोई रसिक या पुण्यार्थी पुरुष शब्द का उच्चारण करे किन्तु स्वयं को शब्दबोध करने के लिये कोई ठलुआ नहीं बैठा है जो कि वाचक शब्दों का उच्चारण करता फिरे, प्रत्युत वक्ताका ज्ञान तो वक्ता के उच्चारे