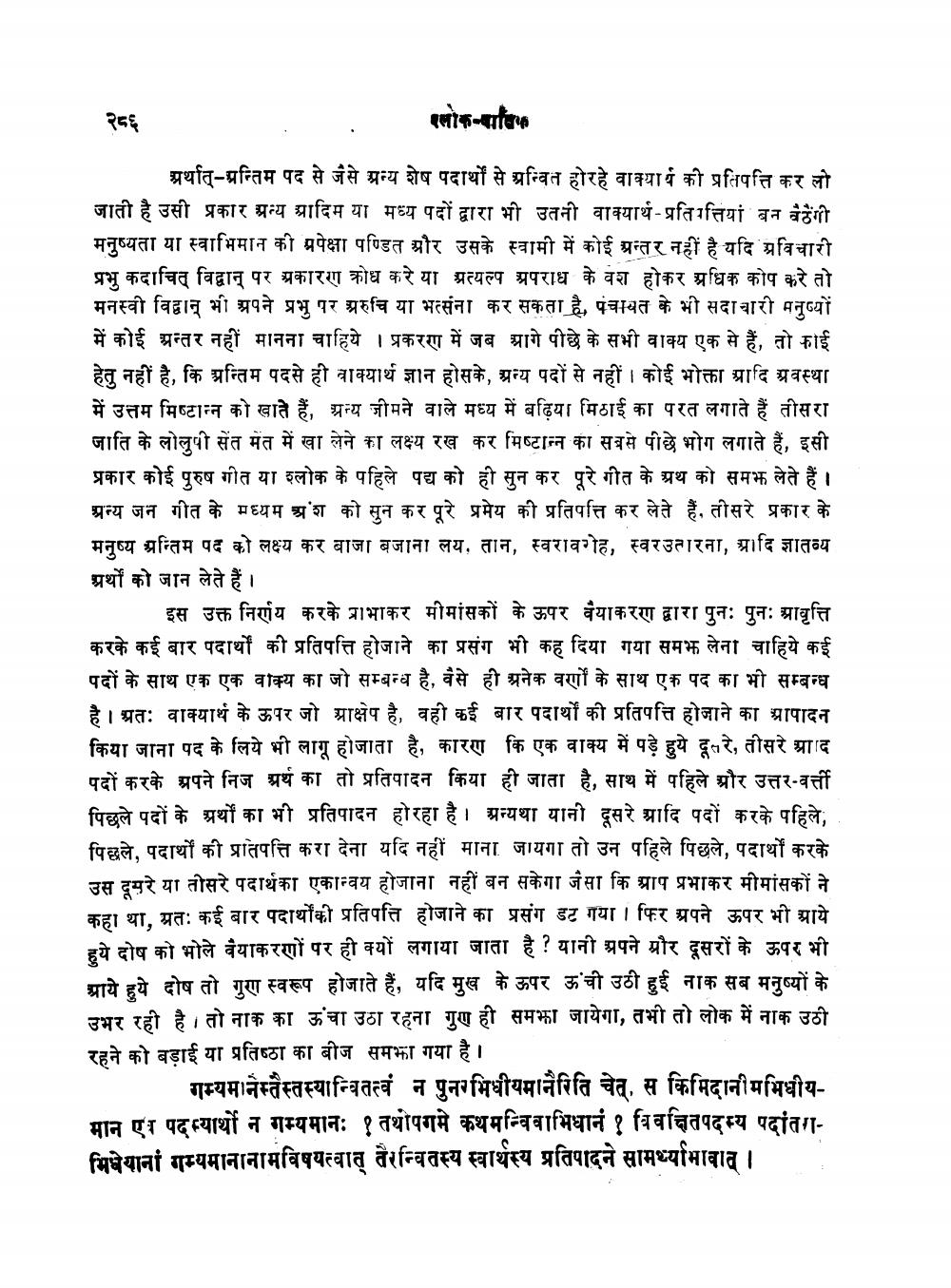________________
श्लोक-वादक
अर्थात्-प्रन्तिम पद से जैसे अन्य शेष पदार्थों से अन्वित होरहे वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति कर लो जाती है उसी प्रकार अन्य आदिम या मध्य पदों द्वारा भी उतनी वाक्यार्थ प्रतिपत्तियां बन बैठेंगी मनुष्यता या स्वाभिमान की प्रपेक्षा पण्डित और उसके स्वामी में कोई अन्तर नहीं है यदि प्रविचारी प्रभु कदाचित् विद्वान् पर अकारण क्रोध करे या अत्यल्प अपराध के वश होकर अधिक कोप करे तो मनस्वी विद्वान् भी अपने प्रभु पर अरुचि या भर्त्सना कर सकता है, पंचायत के भी सदाचारी मनुष्यों में कोई अन्तर नहीं मानना चाहिये । प्रकरण में जब आगे पीछे के सभी वाक्य एक से हैं, तो कोई हेतु नहीं है, कि अन्तिम पदसे ही वाक्यार्थ ज्ञान होसके, अन्य पदों से नहीं । कोई भोक्ता प्रादि अवस्था में उत्तम मिष्टान्न को खाते हैं, अन्य जीमने वाले मध्य में बढ़िया मिठाई का परत लगाते हैं तीसरा कर मिष्टान्न का सबसे पीछे भोग लगाते हैं, इसी ही सुन कर पूरे गीत के अथ को समझ लेते हैं । प्रमेय की प्रतिपत्ति कर लेते हैं, तीसरे प्रकार के तान, स्वरावरोह, स्वरउतारना, आदि ज्ञातव्य
२८६
जाति के लोलुपीतमंत में खा लेने का लक्ष्य रख प्रकार कोई पुरुष गीत या श्लोक के पहिले पद्य को अन्य जन गीत के मध्यम अंश को सुन कर पूरे मनुष्य अन्तिम पद को लक्ष्य कर बाजा बजाना लय श्रर्थों को जान लेते हैं ।
इस उक्त निर्णय करके प्राभाकर मीमांसकों के ऊपर वैयाकरण द्वारा पुनः पुनः प्रवृत्ति करके कई बार पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाने का प्रसंग भी कह दिया गया समझ लेना चाहिये कई पदों के साथ एक एक वाक्य का जो सम्बन्ध है, वैसे ही अनेक वर्णों के साथ एक पद का भी सम्बन्ध है । अतः वाक्यार्थ के ऊपर जो आक्षेप है, वही कई बार पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाने का आपादन किया जाना पद के लिये भी लागू होजाता है, कारण कि एक वाक्य में पड़े हुये दूसरे, तीसरे श्राद पदों करके अपने निज अर्थ का तो प्रतिपादन किया ही जाता है, साथ में पहिले और उत्तर-वर्त्ती पिछले पदों के अर्थों का भी प्रतिपादन होरहा है। अन्यथा यानी दूसरे प्रादि पदों करके पहिले, पिछले पदार्थों की प्रतिपत्ति करा देना यदि नहीं माना जायगा तो उन पहिले पिछले पदार्थों करके उस दूसरे या तीसरे पदार्थका एकान्वय होजाना नहीं बन सकेगा जैसा कि आप प्रभाकर मीमांसकों ने कहा था, अतः कई बार पदार्थों की प्रतिपत्ति होजाने का प्रसंग डट गया। फिर अपने ऊपर भी आये हुये दोष को भोले वैयाकरणों पर ही क्यों लगाया जाता है ? यानी अपने प्रौर दूसरों के ऊपर भी ये हुये दोष तो गुण स्वरूप होजाते हैं, यदि मुख के ऊपर ऊंची उठी हुई नाक सब मनुष्यों के उभर रही है। तो नाक का ऊंचा उठा रहना गुण ही समझा जायेगा, तभी तो लोक में नाक उठी रहने को बड़ाई या प्रतिष्ठा का बीज समझा गया है।
गम्यमानैस्तैस्तस्यान्वितत्वं न पुनरभिधीयमानैरिति चेत्, स किमिदानीमभिधीयमानव पदस्यार्थो न गम्यमानः १ तथोपगमे कथमन्विवाभिधानं ९ विवक्षितपदस्य पदांतराभिधेयानां गम्यमानानामविषयत्वात् तैरन्वितस्य स्वार्थस्य प्रतिपादने सामर्थ्याभावात् ।