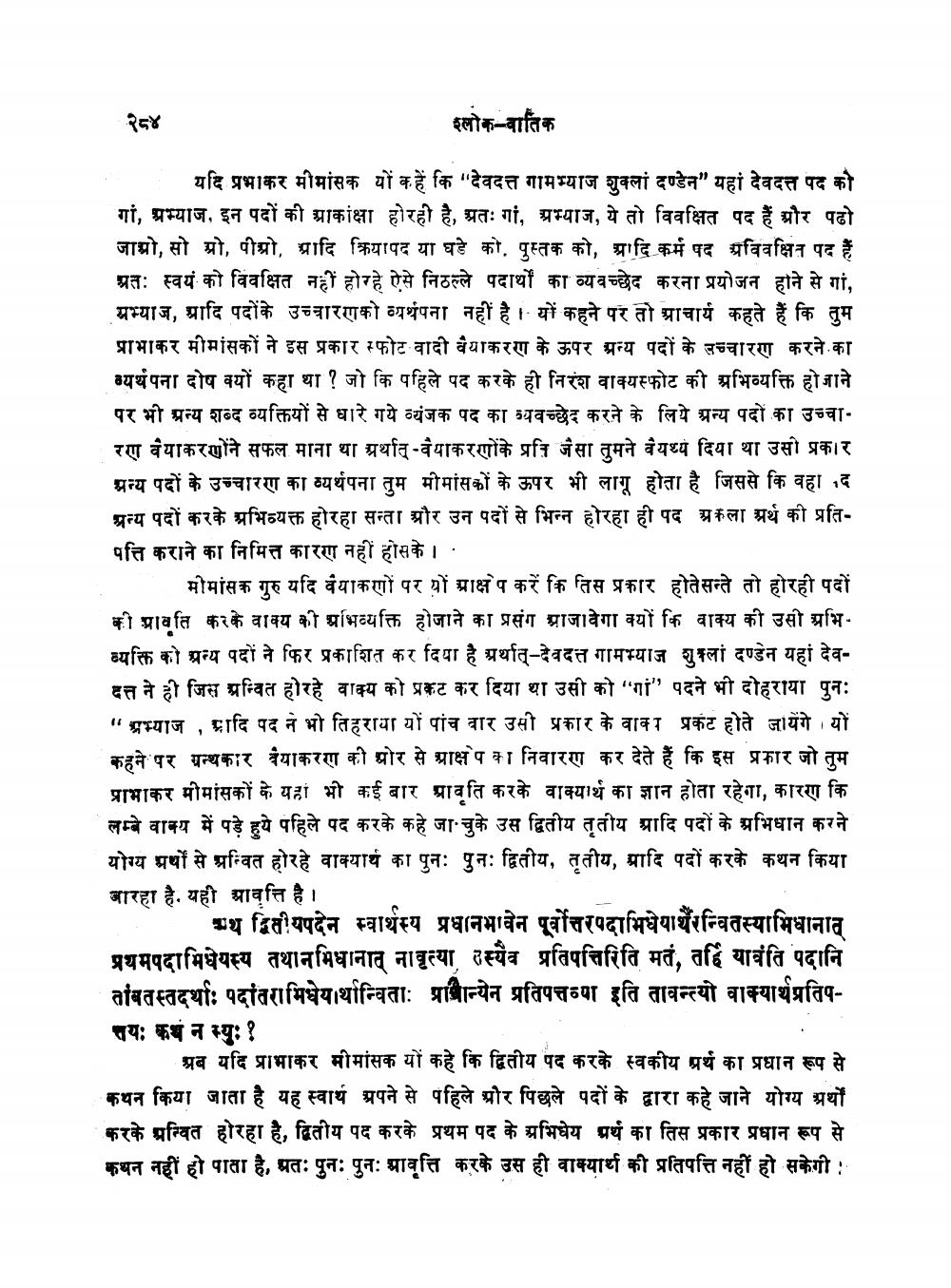________________
-२८४
श्लोक-वातिक
यदि प्रभाकर मीमांसक यों कहें कि "देवदत्त गामभ्याज शुक्लां दण्डेन" यहां देवदत्त पद को गां, अभ्याज, इन पदों की आकांक्षा होरही है, अतः गां, अभ्याज, ये तो विवक्षित पद हैं और पढो जानो, सो प्रो, पीरो, प्रादि क्रियापद या घडे को. पुस्तक को, अादि कर्म पद अविवक्षित पद हैं प्रतः स्वयं को विवक्षित नहीं होरहे ऐसे निठल्ले पदार्थों का व्यवच्छेद करना प्रयोजन होने से गां, अभ्याज, आदि पदों के उच्चारणको व्यर्थपना नहीं है। यों कहने पर तो प्राचार्य कहते हैं कि तुम प्राभाकर मीमांसकों ने इस प्रकार स्फोट वादी वैयाकरण के ऊपर अन्य पदों के उच्चारण करने का व्यर्थपना दोष क्यों कहा था ? जो कि पहिले पद करके ही निरंश वाक्यस्फोट की अभिव्यक्ति हो जाने पर भी अन्य शब्द व्यक्तियों से धारे गये व्यंजक पद का व्यवच्छेद करने के लिये अन्य पदों का उच्चारण वैयाकरणोंने सफल माना था अर्थात्-वैयाकरणोंके प्रति जैसा तमने वैयथ्य दिया था उसी प्रकार अन्य पदों के उच्चारण का व्यर्थपना तुम मीमांसकों के ऊपर भी लागू होता है जिससे कि वहा द अन्य पदों करके अभिव्यक्त होरहा सन्ता और उन पदों से भिन्न होरहा ही पद प्रकला अर्थ की प्रतिपत्ति कराने का निमित्त कारण नहीं होसके। .
____ मीमांसक गुरु यदि वैयाकणों पर यों प्राक्षेप करें कि तिस प्रकार होतेसन्ते तो होरही पदों की प्रावति करके वाक्य की अभिव्यक्ति होजाने का प्रसंग पाजावेगा क्यों कि वाक्य की उसी अभि. व्यक्ति को अन्य पदों ने फिर प्रकाशित कर दिया है अर्थात्-देवदत्त गामभ्याज शुक्लां दण्डेन यहां देवदत्त ने ही जिस अन्वित होरहे वाक्य को प्रकट कर दिया था उसी को “गां" पदने भी दोहराया पुनः
याज प्रादि पद ने भो तिहराया यों पांच बार उसी प्रकार के वाकर प्रकट होते जायेंगे। यों कहने पर ग्रन्थकार वैयाकरण की अोर से आक्षेप का निवारण कर देते हैं कि इस प्रकार जो तुम प्राभाकर मीमांसकों के यहां भी कई बार प्रावृति करके वाक्यार्थ का ज्ञान होता रहेगा, कारण कि लम्बे वाक्य में पड़े हुये पहिले पद करके कहे जा चुके उस द्वितीय तृतीय प्रादि पदों के अभिधान करने योग्य अर्थों से अन्वित होरहे वाक्यार्थ का पुनः पुनः द्वितीय, तृतीय, प्रादि पदों करके कथन किया आरहा है. यही आवृत्ति है।
द्वितीयपदेन स्वार्थस्य प्रधानभावेन पूर्वोत्तरपदाभिधेयाथै रन्वितस्याभिधानात् प्रथमपदामिधेयस्य तथानमिधानात् नावृत्या तस्यैव प्रतिपत्तिरिति मतं, तर्हि यावंति पदानि तांबतस्तदर्थाः पदातराभिधेयार्थान्विताः प्राधान्येन प्रतिपत्तव्या इति तावन्त्यो वाक्यार्थप्रतिपतयः कथं न म्युः?
अब यदि प्राभाकर मीमांसक यों कहे कि द्वितीय पद करके स्वकीय प्रर्थ का प्रधान रूप से कथन किया जाता है यह स्वार्थ अपने से पहिले और पिछले पदों के द्वारा कहे जाने योग्य अर्थों करके प्रन्वित होरहा है, द्वितीय पद करके प्रथम पद के अभिधेय अर्थ का तिस प्रकार प्रधान रूप से कथन नहीं हो पाता है, प्रतः पुनः पुनः प्रावृत्ति करके उस ही वाक्यार्थ की प्रतिपत्ति नहीं हो सकेगी :