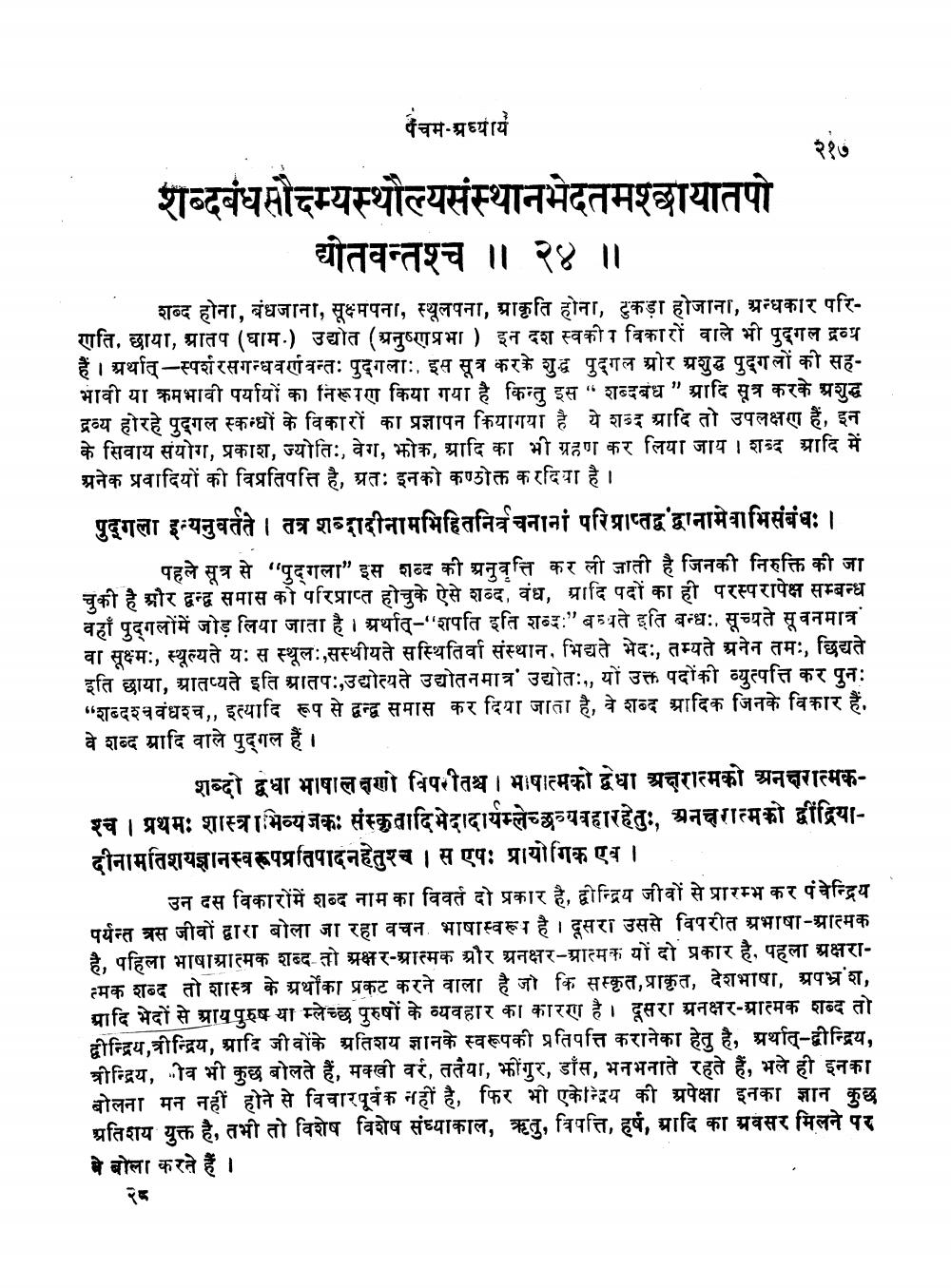________________
पंचम अध्याये
शब्दबंध सौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमश्छायातपो द्योतवन्तश्च ॥ २४ ॥
शब्द होना, बंधजाना, सूक्ष्मपना, स्थूलपना, प्रकृति होना, टुकड़ा होजाना, अन्धकार परिगति, छाया, प्रातप ( घाम) उद्योत ( अनुष्णप्रभा ) इन दश स्वकीय विकारों वाले भी पुद्गल द्रव्य हैं । अर्थात् - स्पर्श रसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः इस सूत्र करके शुद्ध पुद्गल प्रोर अशुद्ध पुद्गलों की सहभावी या क्रमभावी पर्यायों का निरूपण किया गया है किन्तु इस " शब्दबंध " आदि सूत्र करके अशुद्ध द्रव्य होरहे पुद्गल स्कन्धों के विकारों का प्रज्ञापन कियागया है ये शब्द आदि तो उपलक्षण हैं, इन के सिवाय संयोग, प्रकाश, ज्योतिः, वेग, भोक, आदि का भी ग्रहण कर लिया जाय । शब्द आदि में अनेक प्रवादियों की विप्रतिपत्ति है, अतः इनको कण्डोक्त करदिया है ।
पुद्गला इन्यनुवर्तते । तत्र शब्दादीनामभिहितनिर्वचनानां परिप्राप्तद्वद्वानामेवाभिसंबंधः ।
पहले सूत्र से "पुद्गला" इस शब्द की अनुवृत्ति कर ली जाती है जिनकी निरुक्ति की जा चुकी है और द्वन्द्व समास को परिप्राप्त होचुके ऐसे शब्द, वंध, प्रादि पदों का ही परस्परापेक्ष सम्बन्ध वहाँ पुद्गलों में जोड़ लिया जाता है। अर्थात् -" शपति इति शब्दः" बच्चते इति बन्धः सूच्यते सूचनमात्र वा सूक्ष्मः, स्थूल्यते यः स स्थूलः, सस्थीयते सस्थितिर्वा संस्थान, भिद्यते भेदः, तम्यते अनेन तमः, छिद्यते इति छाया, प्रातप्यते इति प्रातप:, उद्योत्यते उद्योतनमात्र उद्योतः यों उक्त पदोंकी व्युत्पत्ति कर पुनः "शब्दश्च वंधश्च, इत्यादि रूप से द्वन्द्व समास कर दिया जाता है, वे शब्द आदिक जिनके विकार हैं. वे शब्द प्रादि वाले पुद्गल हैं ।
२१७
शब्दो द्वेधा भाषा लक्षणो विपरीतश्च । भाषात्मको द्वेधा अक्षरात्मको अनक्षरात्मकश्च । प्रथमः शास्त्राभिव्यंजकः संस्कृतादिभेदादार्यम्लेच्छव्यवहारहेतुः, अनक्षरात्मको द्वींद्रियादीनामतिशयज्ञानस्वरूपप्रतिपादन हेतुश्च । स एषः प्रायोगिक एव ।
उन दस विकारों में शब्द नाम का विवर्त दो प्रकार है, द्वीन्द्रिय जीवों से प्रारम्भ कर पंचेन्द्रिय पर्यन्त त्रस जीवों द्वारा बोला जा रहा वचन भाषास्वरूप है । दूसरा उससे विपरीत प्रभाषा आत्मक है, पहिला भाषाग्रात्मक शब्द तो अक्षर श्रात्मक और अनक्षर - प्रात्मक यों दो प्रकार है, पहला अक्षरात्मक शब्द तो शास्त्र के अर्थोंका प्रकट करने वाला है जो कि संस्कृत, प्राकृत, देशभाषा, अपभ्रंश, आदि भेदों से प्राय पुरुष या म्लेच्छ पुरुषों के व्यवहार का कारण है। दूसरा अनक्षर- प्रात्मक शब्द तो द्वन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, श्रादि जीवोंके प्रतिशय ज्ञानके स्वरूपकी प्रतिपत्ति करानेका हेतु है, अर्थात् - द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, गीव भी कुछ बोलते हैं, मक्खी वरं, ततैया, झींगुर, डाँस, भनभनाते रहते हैं, भले ही इनका बोलना मन नहीं होने से विचारपूर्वक नहीं है, फिर भी एकेन्द्रिय की अपेक्षा इनका ज्ञान कुछ श्रतिशय युक्त है, तभी तो विशेष विशेष संध्याकाल, ऋतु, विपत्ति, हर्ष, आदि का अवसर मिलने पर मे बोला करते हैं ।
रेष