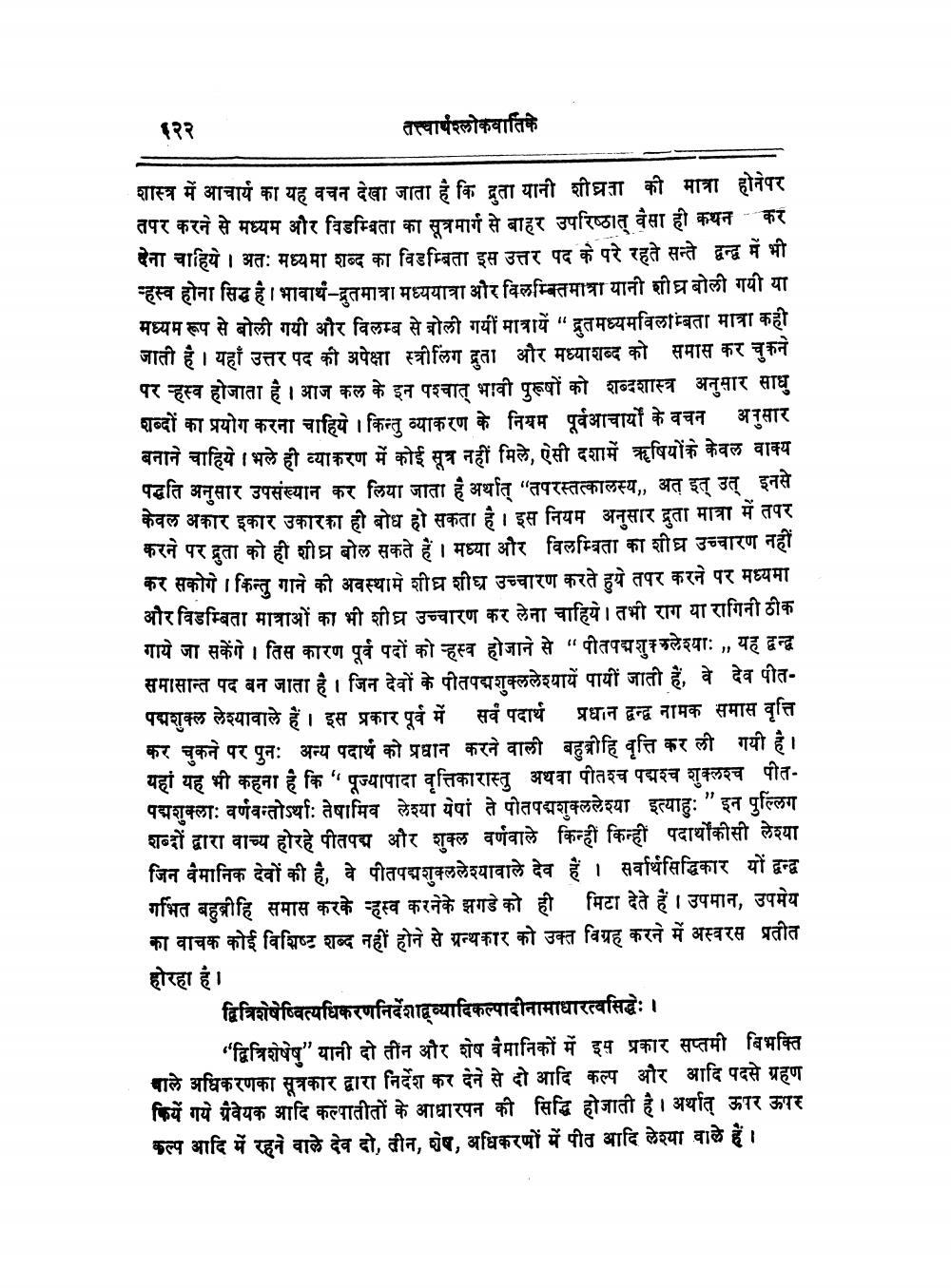________________
६२२
तत्त्वार्षश्लोकवार्तिके
-
शास्त्र में आचार्य का यह वचन देखा जाता है कि दूता यानी शीघ्रता की मात्रा होनेपर तपर करने से मध्यम और विडम्बिता का सूत्रमार्ग से बाहर उपरिष्ठात् वैसा ही कथन कर देना चाहिये । अतः मध्यमा शब्द का विडम्बिता इस उत्तर पद के परे रहते सन्ते द्वन्द्व में भी -हस्व होना सिद्ध है । भावार्थ-द्रुतमात्रा मध्ययात्रा और विलम्बितमात्रा यानी शीघ्र बोली गयी या मध्यम रूप से बोली गयी और विलम्ब से बोली गयीं मात्रायें " द्रुतमध्यमविलाम्बता मात्रा कही जाता है । यहाँ उत्तर पद की अपेक्षा स्त्रीलिंग द्रुता और मध्याशब्द को समास कर चुकन पर हस्व होजाता है। आज कल के इन पश्चात् भावी पुरूषों को शब्दशास्त्र अनुसार साधु शब्दों का प्रयोग करना चाहिये । किन्तु व्याकरण के नियम पूर्वआचार्यों के वचन अनुसार बनाने चाहिये । भले ही व्याकरण में कोई सूत्र नहीं मिले, ऐसी दशामें ऋषियोंके केवल वाक्य पद्धति अनुसार उपसंख्यान कर लिया जाता है अर्थात् "तपरस्तत्कालस्य,, अत इत् उत् इनसे केवल अकार इकार उकारका ही बोध हो सकता है । इस नियम अनुसार द्रुता मात्रा में तपर करने पर द्रुता को ही शीघ्र बोल सकते हैं । मध्या और विलम्बिता का शीघ्र उच्चारण नहीं कर सकोगे । किन्तु गाने की अवस्थामे शीघ्र शीघ्र उच्चारण करते हुये तपर करने पर मध्यमा और विडम्बिता मात्राओं का भी शीघ्र उच्चारण कर लेना चाहिये। तभी राग या रागिनी ठीक गाये जा सकेंगे। तिस कारण पूर्व पदों को हस्व होजाने से “ पीतपद्मशुक्ललेश्याः ,, यह द्वन्द्व समासान्त पद बन जाता है । जिन देवों के पीतपद्मशुक्ललेश्यायें पायी जाती हैं, वे देव पीतपद्मशुक्ल लेश्यावाले हैं। इस प्रकार पूर्व में सर्व पदार्थ प्रधान द्वन्द्व नामक समास वृत्ति कर चुकने पर पुनः अन्य पदार्थ को प्रधान करने वाली बहुव्रीहि वृत्ति कर ली गयी है। यहां यह भी कहना है कि 'पूज्यापादा वृत्तिकारास्तु अथवा पीतश्च पद्मश्च शुक्लश्च पीतपद्मशुक्लाः वर्णवन्तोऽर्थाः तेषामिव लेश्या येषां ते पोतपद्मशुक्ललेश्या इत्याहुः" इन पुल्लिग शब्दों द्वारा वाच्य होरहे पीतपद्म और शुक्ल वर्णवाले किन्हीं किन्हीं पदार्थोकीसी लेश्या जिन वैमानिक देवों की है, वे पीतपद्मशुक्ललेश्यावाले देव हैं । सर्वार्थसिद्धिकार यों द्वन्द्व गभित बहुव्रीहि समास करके -हस्व करनेके झगडे को ही मिटा देते हैं । उपमान, उपमेय का वाचक कोई विशिष्ट शब्द नहीं होने से ग्रन्थकार को उक्त विग्रह करने में अस्वरस प्रतीत होरहा है।
द्वित्रिशेषेष्वित्यधिकरणनिर्देशाव्यादिकल्पादीनामाधारत्वसिद्धेः ।
"द्वित्रिशेषेषु" यानी दो तीन और शेष वैमानिकों में इस प्रकार सप्तमी बिभक्ति वाले अधिकरणका सूत्रकार द्वारा निर्देश कर देने से दो आदि कल्प और आदि पदसे ग्रहण किये गये प्रैवेयक आदि कल्पातीतों के आधारपन की सिद्धि होजाती है । अर्थात् ऊपर ऊपर कल्प आदि में रहने वाले देव दो, तीन, शेष, अधिकरणों में पीत आदि लेश्या वाले हैं।