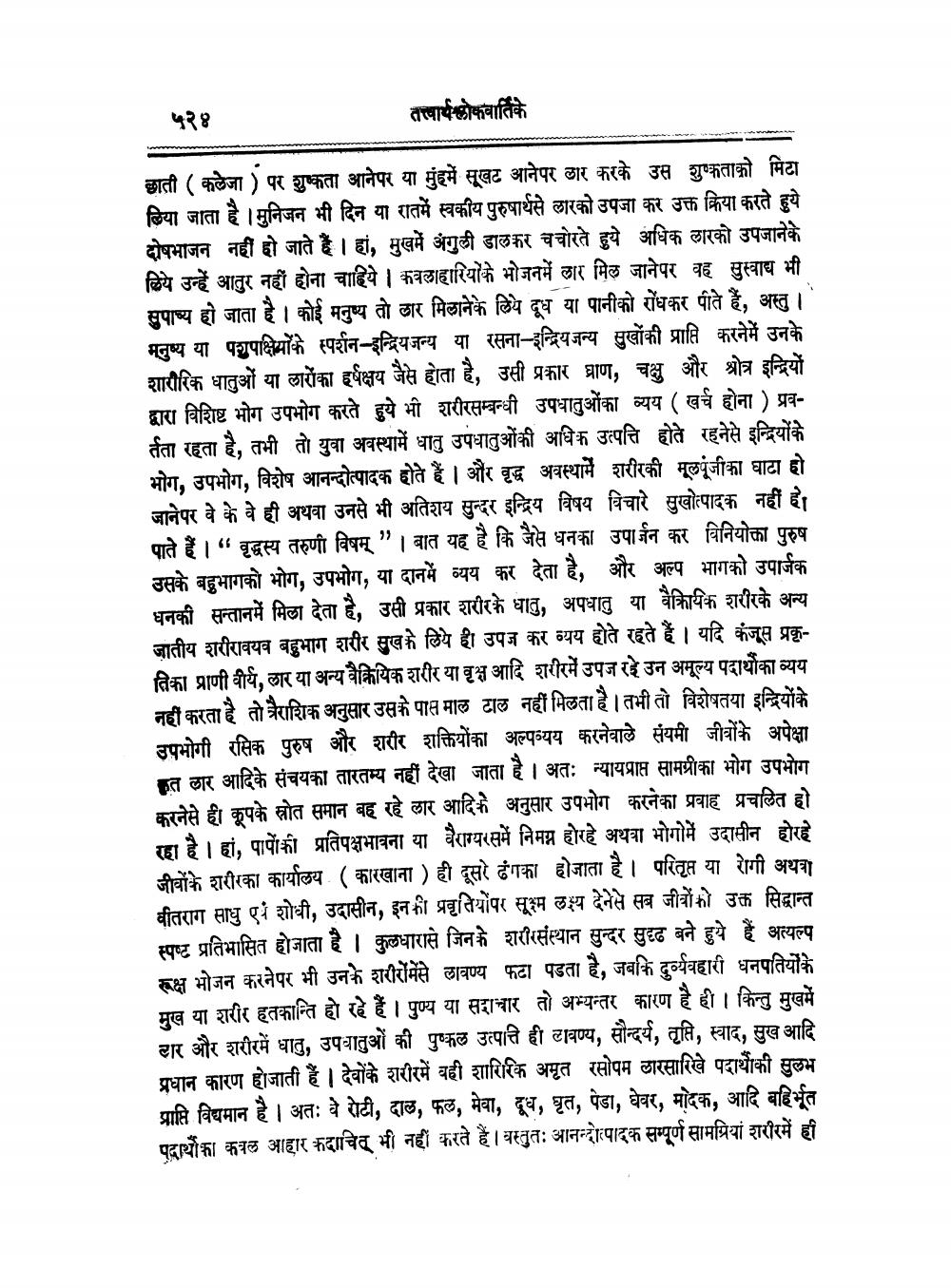________________
५२४
तत्वार्यश्लोकवार्तिके
छाती ( कलेजा ) पर शुष्कता आनेपर या मुंहमें सूखट आनेपर लार करके उस शुष्कताको मिटा लिया जाता है । मुनिजन भी दिन या रातमें स्वकीय पुरुषार्थसे लारको उपजा कर उक्त क्रिया करते हुये दोषभाजन नहीं हो जाते हैं । हां, मुखमें अंगुली डालकर चचोरते हुये अधिक लारको उपजानेके लिये उन्हें आतुर नहीं होना चाहिये । कवलाहारियोंके भोजनमें लार मिल जानेपर वह सुस्वाय भी सुपाच्य हो जाता है । कोई मनुष्य तो लार मिलानेके लिये दूध या पानीको रोंधकर पीते हैं, अस्तु । मनुष्य या पशुपक्षियोंके स्पर्शन-इन्द्रियजन्य या रसना-इन्द्रियजन्य सुखोंकी प्राप्ति करनेमें उनके शारीरिक धातुओं या लारोंका हर्षक्षय जैसे होता है, उसी प्रकार घ्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रियों द्वारा विशिष्ट भोग उपभोग करते हुये भी शरीरसम्बन्धी उपधातुओंका व्यय ( खर्च होना ) प्रवतता रहता है, तभी तो युवा अवस्थामें धातु उपधातुओंकी अधिक उत्पत्ति होते रहनेसे इन्द्रियों के भोग, उपभोग, विशेष आनन्दोत्पादक होते हैं । और वृद्ध अवस्थामें शरीरकी मूलपूंजीका घाटा हो जानेपर वे के वे ही अथवा उनसे भी अतिशय सुन्दर इन्द्रिय विषय विचारे सुखोत्पादक नहीं है। पाते हैं । " वृद्धस्य तरुणी विषम् "। बात यह है कि जैसे धनका उपार्जन कर विनियोक्ता पुरुष उसके बहुभागको भोग, उपभोग, या दानमें व्यय कर देता है, और अल्प भागको उपार्जक धनकी सन्तानमें मिला देता है, उसी प्रकार शरीरके धातु, अपधातु या वैक्रिायक शरीरके अन्य जातीय शरीरावयव बहुभाग शरीर सुखके लिये ही उपज कर व्यय होते रहते हैं। यदि कंजूस प्रकृतिका प्राणी वीर्य, लार या अन्य वैनियिक शरीर या वृक्ष आदि शरीरमें उपज रहे उन अमूल्य पदार्थोका व्यय नहीं करता है तो त्रैराशिक अनुसार उसके पास माल टाल नहीं मिलता है। तभी तो विशेषतया इन्द्रियों के उपभोगी रसिक पुरुष और शरीर शक्तियोंका अल्पव्यय करनेवाले संयमी जीवोंके अपेक्षा हत लार आदिके संचयका तारतम्य नहीं देखा जाता है । अतः न्यायप्राप्त सामग्रीका भोग उपभोग करनेसे ही कूपके स्रोत समान बह रहे लार आदिके अनुसार उपभोग करनेका प्रवाह प्रचलित हो रहा है । हां, पापोंकी प्रतिपक्षभावना या वैराग्यरसमें निमग्न होरहे अथवा भोगोमें उदासीन होरहे जीवोंके शरीरका कार्यालय ( कारखाना ) ही दूसरे ढंगका होजाता है। परितृप्त या रोगी अथवा वीतराग साधु एवं शोधी, उदासीन, इनकी प्रवृत्तियोंपर सूक्ष्म लक्ष्य देनेसे सब जीवों को उक्त सिद्धान्त स्पष्ट प्रतिभासित होजाता है । कुलधारासे जिनके शरीरसंस्थान सुन्दर सुदृढ बने हुये हैं अत्यल्प रूक्ष भोजन करनेपर भी उनके शरीरोंमेसे लावण्य फटा पडता है, जबकि दुर्व्यवहारी धनपतियों के मुख या शरीर हतकान्ति हो रहे हैं । पुण्य या सदाचार तो अभ्यन्तर कारण है ही। किन्तु मुखमें बार और शरीर में धातु, उपधातुओं की पुष्कल उत्पत्ति ही लावण्य, सौन्दर्य, तृप्ति, स्वाद, सुख आदि प्रधान कारण होजाती हैं । देवोंके शरीरमें वही शारिरिक अमृत रसोपम लारसारिखे पदार्थोकी सुलभ प्राप्ति विद्यमान है । अतः वे रोटी, दाल, फल, मेवा, दूध, घृत, पेडा, घेवर, मोदक, आदि बहिर्भूत पदार्थों का कवल आहार कदाचित् भी नहीं करते हैं । वस्तुतः आनन्दोत्पादक सम्पूर्ण सामग्रियां शरीरमें ही