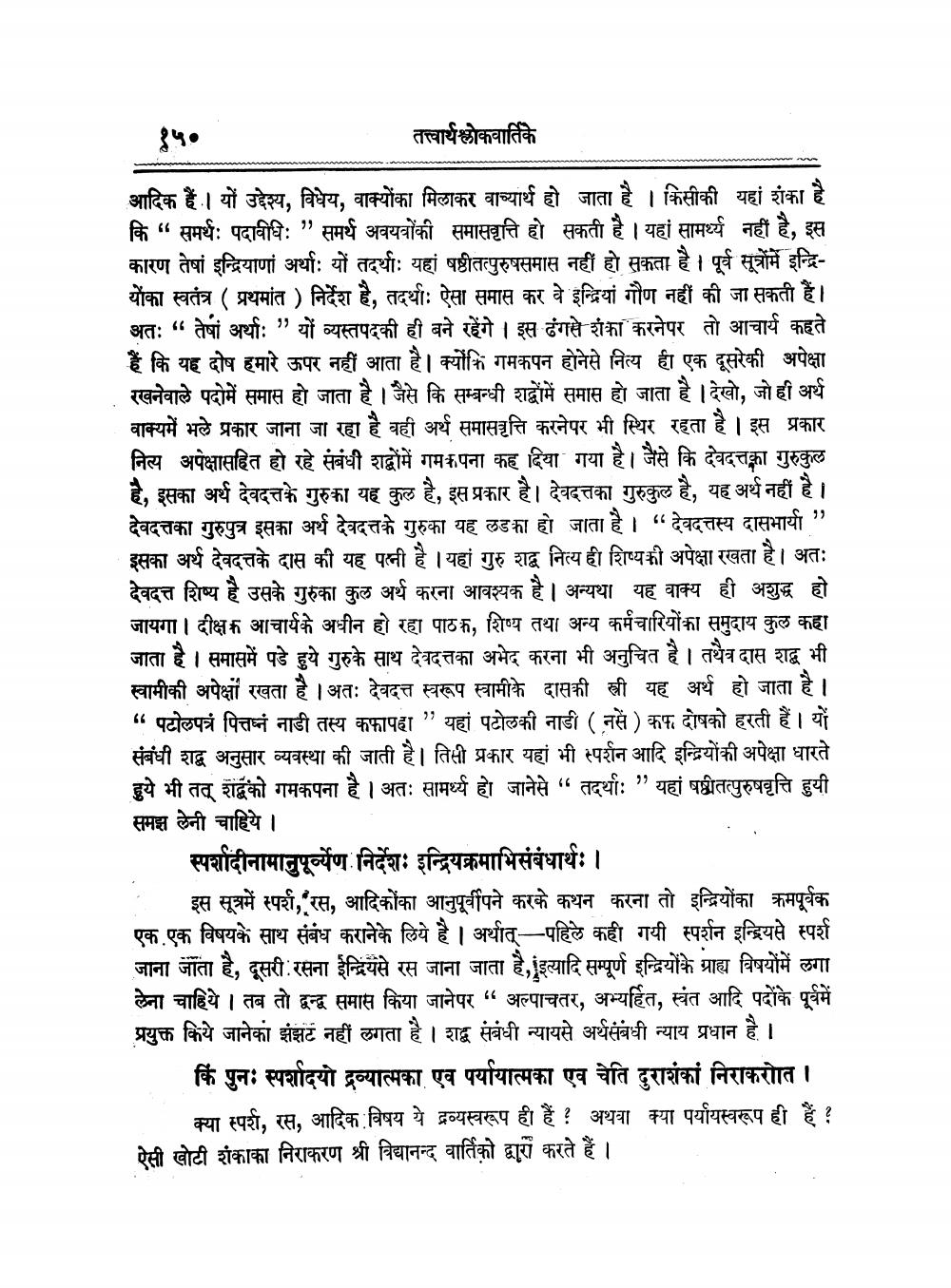________________
१५.
तत्त्वार्यश्लोकवार्तिके
आदिक हैं । यो उद्देश्य, विधेय, वाक्योंका मिलाकर वाच्यार्थ हो जाता है । किसीकी यहां शंका है कि " समर्थः पदावधिः " समर्थ अवयवोंकी समासवृत्ति हो सकती है । यहां सामर्थ्य नहीं है, इस कारण तेषां इन्द्रियाणां अर्थाः यों तदर्थाः यहां षष्ठीतत्पुरुषसमास नहीं हो सकता है। पूर्व सूत्रोंमें इन्द्रियोंका स्वतंत्र ( प्रथमांत ) निर्देश है, तदर्थाः ऐसा समास कर वे इन्द्रियां गौण नहीं की जा सकती हैं। अतः " तेषां अर्थाः " यों व्यस्तपदकी ही बने रहेंगे । इस ढंगसे शंका करनेपर तो आचार्य कहते हैं कि यह दोष हमारे ऊपर नहीं आता है। क्योंकि गमकपन होनेसे नित्य ही एक दूसरेकी अपेक्षा रखनेवाले पदोमें समास हो जाता है । जैसे कि सम्बन्धी शद्बोंमें समास हो जाता है । देखो, जो ही अर्थ वाक्यमें भले प्रकार जाना जा रहा है वही अर्थ समासवृत्ति करनेपर भी स्थिर रहता है । इस प्रकार नित्य अपेक्षासहित हो रहे संबंधी शद्बोंमें गमकपना कह दिया गया है। जैसे कि देवदत्तका गुरुकुल है, इसका अर्थ देवदत्तके गुरुका यह कुल है, इस प्रकार है। देवदत्तका गुरुकुल है, यह अर्थ नहीं है। देवदत्तका गुरुपुत्र इसका अर्थ देवदत्तके गुरुका यह लडका हो जाता है । " देवदत्तस्य दासभाया " इसका अर्थ देवदत्तके दास की यह पत्नी है । यहां गुरु शब्द नित्य ही शिष्यकी अपेक्षा रखता है। अतः देवदत्त शिष्य है उसके गुरुका कुल अर्थ करना आवश्यक है । अन्यथा यह वाक्य ही अशुद्ध हो जायगा। दीक्षक आचार्य के अधीन हो रहा पाठक, शिष्य तथा अन्य कर्मचारियोंका समुदाय कुल कहा जाता है । समासमें पडे हुये गुरुके साथ देवदत्तका अभेद करना भी अनुचित है । तथैव दास शब्द भी स्वामीकी अपेक्षा रखता है । अतः देवदत्त स्वरूप स्वामीके दासकी स्त्री यह अर्थ हो जाता है । " पटोलपत्रं पित्तघ्नं नाडी तस्य कफापहा" यहां पटोलकी नाडी ( नसें ) कफ दोषको हरती हैं। यों संबंधी शब्द अनुसार व्यवस्था की जाती है। तिसी प्रकार यहां भी स्पर्शन आदि इन्द्रियोंकी अपेक्षा धारते हुये भी तत् शद्वको गमकपना है । अतः सामर्थ्य हो जानेसे “ तदर्थाः " यहां षष्ठीतत्पुरुषवृत्ति हुयी समझ लेनी चाहिये ।
स्पर्शादीनामानुपूर्पण निर्देशः इन्द्रियक्रमाभिसंबंधार्थः।
इस सूत्रमें स्पर्श, रस, आदिकोंका आनुपूर्वीपने करके कथन करना तो इन्द्रियोंका क्रमपूर्वक एक एक विषयके साथ संबंध करानेके लिये है । अर्थात्-पहिले कही गयी स्पर्शन इन्द्रियसे स्पर्श जाना जाता है, दूसरी रसना ईन्द्रियंसे रस जाना जाता है, इत्यादि सम्पूर्ण इन्द्रियोंके ग्राह्य विषयोंमें लगा लेना चाहिये । तब तो द्वन्द्व समास किया जानेपर " अल्पाचतर, अभ्यहित, स्वंत आदि पदोंके पूर्वमें प्रयुक्त किये जानेका झंझट नहीं लगता है । शब्द संबंधी न्यायसे अर्थसंबंधी न्याय प्रधान है।
किं पुनः स्पर्शादयो द्रव्यात्मका एव पर्यायात्मका एव चेति दुराशंकां निराकरोति ।
क्या स्पर्श, रस, आदिक विषय ये द्रव्यस्वरूप ही हैं ? अथवा क्या पर्यायस्वरूप ही हैं ? ऐसी खोटी शंकाका निराकरण श्री विद्यानन्द वार्तिको द्वारा करते हैं ।