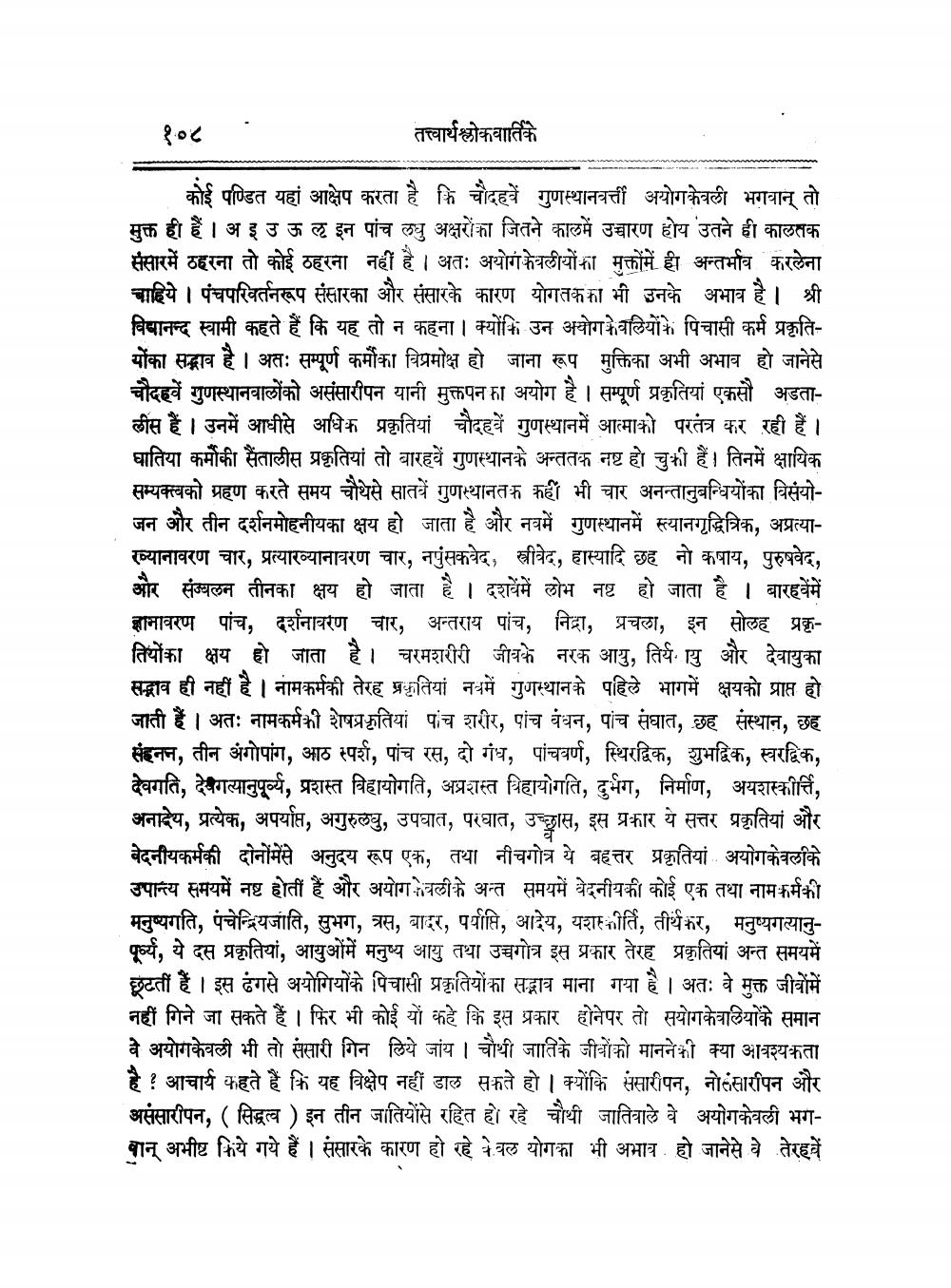________________
१०८
तत्त्वार्थश्लोक वार्तिके
कोई पण्डित यहां आक्षेप करता है कि चौदहवें गुणस्थानवर्त्ती अयोगकेवली भगवान् तो मुक्त ही हैं । अ इ उ ऊ ऌ इन पांच लघु अक्षरोंका जितने कालमें उच्चारण होय उतने ही कालतक संसारमें ठहरना तो कोई ठहरना नहीं है । अतः अयोगकेवलीयों का मुक्तोंमें ही अन्तर्भाव करना चाहिये । पंचपरिवर्तनरूप संसारका और संसार के कारण योगतक का भी उनके अभाव है। । श्री विद्यानन्द स्वामी कहते हैं कि यह तो न कहना । क्योंकि उन अयोग के वलियों के पिचासी कर्म प्रकृतियोंका सद्भाव है। अतः सम्पूर्ण कर्मोंका प्रमोक्ष हो जाना रूप मुक्तिका अभी अभाव हो जानेसे चौदहवें गुणस्थानवालोंको असंसारीपन यानी मुक्तपन का अयोग है । सम्पूर्ण प्रकृतियां एकसौ अडतालीस हैं । उनमें आधीसे अधिक प्रकृतियां चौदहवें गुणस्थानमें आत्माको परतंत्र कर रही हैं । घातिया कर्मों की सैंतालीस प्रकृतियां तो बारहवें गुणस्थानके अन्ततक नष्ट हो चुकी हैं । तिनमें क्षायिक सम्यक्त्वको ग्रहण करते समय चौथेसे सातवें गुणस्थानतक कहीं भी चार अनन्तानुबन्धियोंका विसयोजन और तीन दर्शनमोहनीयका क्षय हो जाता है और नवमें गुणस्थान में स्त्यानगृद्धित्रिक, अप्रत्यारव्यानावरण चार, प्रत्यारव्यानावरण चार, नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, हास्यादि छह नो कषाय, पुरुषवेद, और संज्वलन तीनका क्षय हो जाता है । दशवेंमें लोभ नष्ट हो जाता है । बारहवें में ज्ञानावरण पांच, दर्शनावरण चार, अन्तराय पांच, निद्रा, प्रचला इन सोलह प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। चरमशरीरी जीवके नरक आयु, तिर्ययु और देवायुका सद्भाव ही नहीं है । नामकर्मकी तेरह प्रकृतियां नत्रमें गुणस्थानके पहिले भागमें क्षयको प्राप्त हो जाती हैं । अतः नामकर्म की शेषप्रकृतियां पांच शरीर, पांच बंधन, पांच संघात, छह संस्थान, छह संहनन, तीन अंगोपांग, आठ स्पर्श, पांच रस, दो गंध, पांचवर्ण, स्थिरद्विक, शुभद्विक, स्वरद्विक, देवगति, देवगत्यानुपूर्व्य, प्रशस्त विहायोगति, अप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, निर्माण, अयशस्कीर्ति, अनादेय, प्रत्येक, अपर्याप्त, अगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्रास, इस प्रकार ये सत्तर प्रकृतियां और वेदनीयकर्मकी दोनोंमेंसे अनुदय रूप एक, तथा नीचगोत्र ये बहत्तर प्रकृतियां अयोगकेवलकि उपान्त्य समय में नष्ट होतीं हैं और अयोगकेवली के अन्त समयमें वेदनीयकी कोई एक तथा नामकर्मकी मनुष्यगति, पंचेन्द्रियजाति, सुभग, त्रस, बादर, पर्याप्ति, आय, यशस्कीर्ति, तीर्थकर, मनुष्यगत्यानुपूर्व्यं, ये दस प्रकृतियां, आयुओंमें मनुष्य आयु तथा उच्चगोत्र इस प्रकार तेरह प्रकृतियां अन्त समय में छूटतीं हैं । इस ढंगसे अयोगियों के पिचासी प्रकृतियों का सद्भाव माना गया है। अतः वे मुक्त जीवों में नहीं गिने जा सकते हैं । फिर भी कोई यों कहे कि इस प्रकार होनेपर तो सयोग केवालयों के समान a अयोगकेवली भी तो संसारी गिन लिये जांय । चौथी जाति के जीवों को मानने की क्या आवश्यकता है ? आचार्य कहते हैं कि यह विक्षेप नहीं डाल सकते हो। क्योंकि संसारीपन, नोसंसारपिन और असंसारीपन, ( सिद्धत्व ) इन तीन जातियोंसे रहित हो रहे चौथी जातिवाले वे अयोगकेवली भगबानू अभीष्ट किये गये हैं । संसारके कारण हो रहे केवल योगका भी अभाव हो जानेसे वे तेरहवें