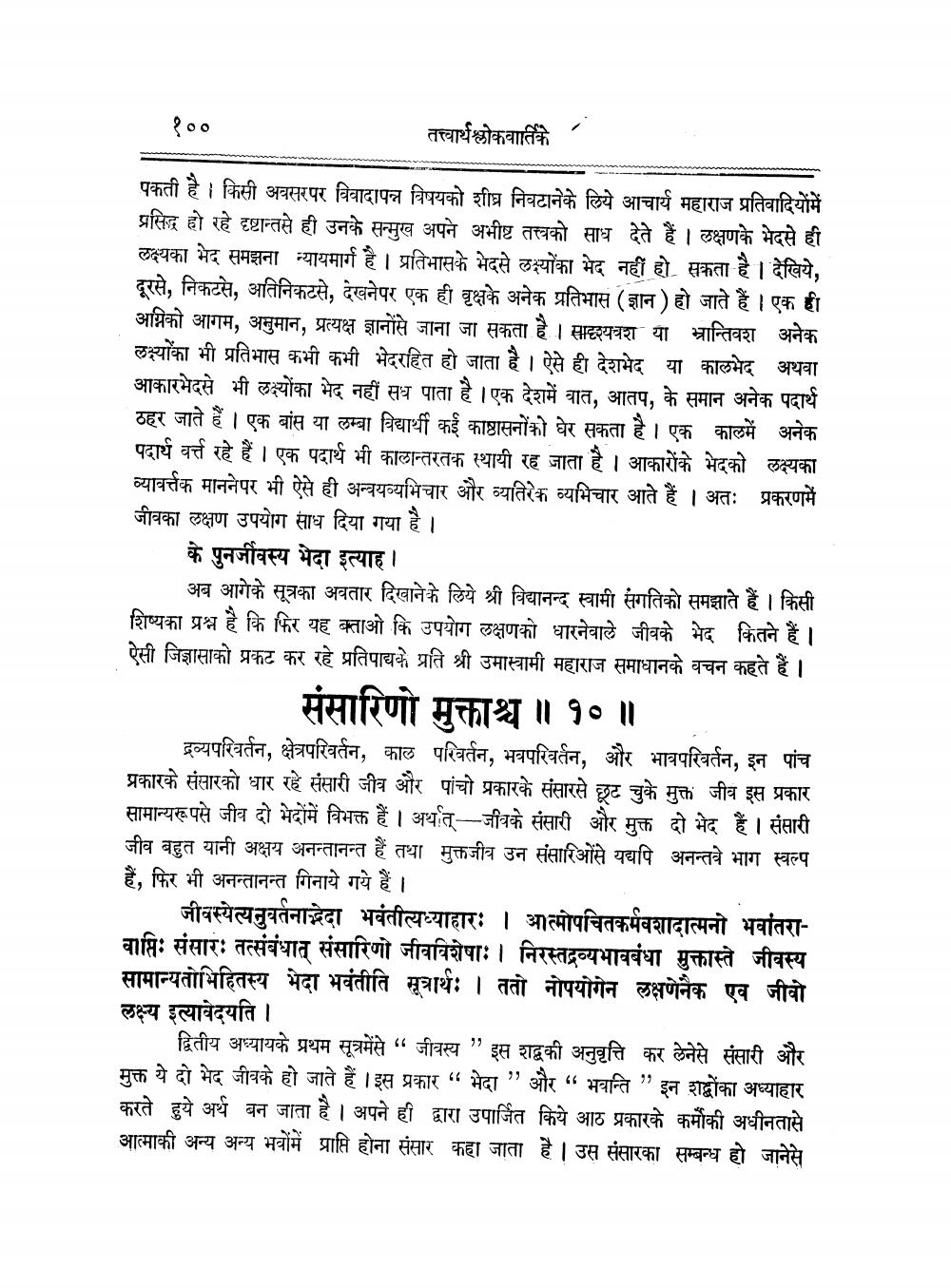________________
१००
तत्त्वार्थश्लोक वार्तिके
1
सकता है । देखिये,
पकती है । किसी अवसरपर विवादापन्न विषयको शीघ्र निवटानेके लिये आचार्य महाराज प्रतिवादियोंमें प्रसिद्ध हो रहे दृष्टान्तसे ही उनके सन्मुख अपने अभीष्ट तत्त्वको साध देते हैं । लक्षण के भेदसे ही लक्ष्यका भेद समझना न्यायमार्ग है । प्रतिभास के भेदसे लक्ष्योंका भेद नहीं हो दूरसे, निकटसे, अतिनिकटसे, देखनेपर एक ही वृक्षके अनेक प्रतिभास (ज्ञान) हो जाते हैं। एक ही अग्निको आगम, अनुमान, प्रत्यक्ष ज्ञानोंसे जाना जा सकता है । सादृश्यवश या भ्रान्तिवश अनेक लक्ष्योंका भी प्रतिभास कभी कभी भेदरहित हो जाता है। ऐसे ही देशभेद या कालभेद अथवा आकारभेदसे भी लक्ष्योंका भेद नहीं सब पाता । एक देशमें वात, आतप, समान अनेक पदार्थ ठहर जाते हैं । एक बांस या लम्बा विद्यार्थी कई काष्ठासनों को घेर सकता । एक कालमें अनेक पदार्थ वर्त्त रहे हैं । एक पदार्थ भी कालान्तरतक स्थायी रह जाता है । आकारोंके भेदको लक्ष्यका व्यावर्त्तक माननेपर भी ऐसे ही अन्वयव्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार आते हैं । अतः प्रकरणमें जीवका लक्षण उपयोग साध दिया गया 1
के पुनर्जीवस्य भेदा इत्याह ।
अब आगे के सूत्रका अवतार दिखाने के लिये श्री विद्यानन्द स्वामी संगतिको समझाते हैं । किसी शिष्यका प्रश्न है कि फिर यह बताओ कि उपयोग लक्षणको धारनेवाले जीवके भेद कितने हैं । ऐसी जिज्ञासाको प्रकट कर रहे प्रतिपाद्य के प्रति श्री उमास्वामी महाराज समाधानके वचन कहते हैं ।
संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १०॥
द्रव्यपरिवर्तन, क्षेत्रपरिवर्तन, काल परिवर्तन, भवपरिवर्तन, और भावपरिवर्तन, इन पांच प्रकारके संसारको धार रहे संसारी जीव और पांचो प्रकारके संसारसे छूट चुके मुक्त जीव इस प्रकार सामान्यरूपसे जीव दो भेदोंमें विभक्त हैं । अर्थात् जीवके संसारी और मुक्त जीव बहुत यानी अक्षय अनन्तानन्त हैं तथा मुक्तजीव उन संसारिओंसे यद्यपि हैं, फिर भी अनन्तानन्त गिनाये गये हैं ।
1
दो भेद हैं । संसारी अनन्तवे भाग स्वल्प
जीवस्येत्यनुवर्तनाद्भेदा भवतीत्यध्याहारः । आत्मोपचितकर्मवशादात्मनो भवांतरावाप्तिः संसारः तत्संबंधात् संसारिणो जीवविशेषाः । निरस्तद्रव्यभावबंधा मुक्तास्ते जीवस्य सामान्यतोभिहितस्य भेदा भवतीति सूत्रार्थः । ततो नोपयोगेन लक्षणेनैक एव जीवो लक्ष्य इत्यावेदयति ।
द्वितीय अध्यायके प्रथम सूत्रमेंसे " जीवस्य " इस शद्वकी अनुवृत्ति कर लेनेसे संसारी और मुक्त ये दो भेद जीवके हो जाते हैं । इस प्रकार " भेदा " और " भवन्ति " इन शब्दोंका अध्याहार करते हुये अर्थ बन जाता है । अपने ही द्वारा उपार्जित किये आठ प्रकारके कर्मोकी अधीनतासे आत्माकी अन्य अन्य भवोंमें प्राप्ति होना संसार कहा जाता है । उस संसारका सम्बन्ध हो जानेसे