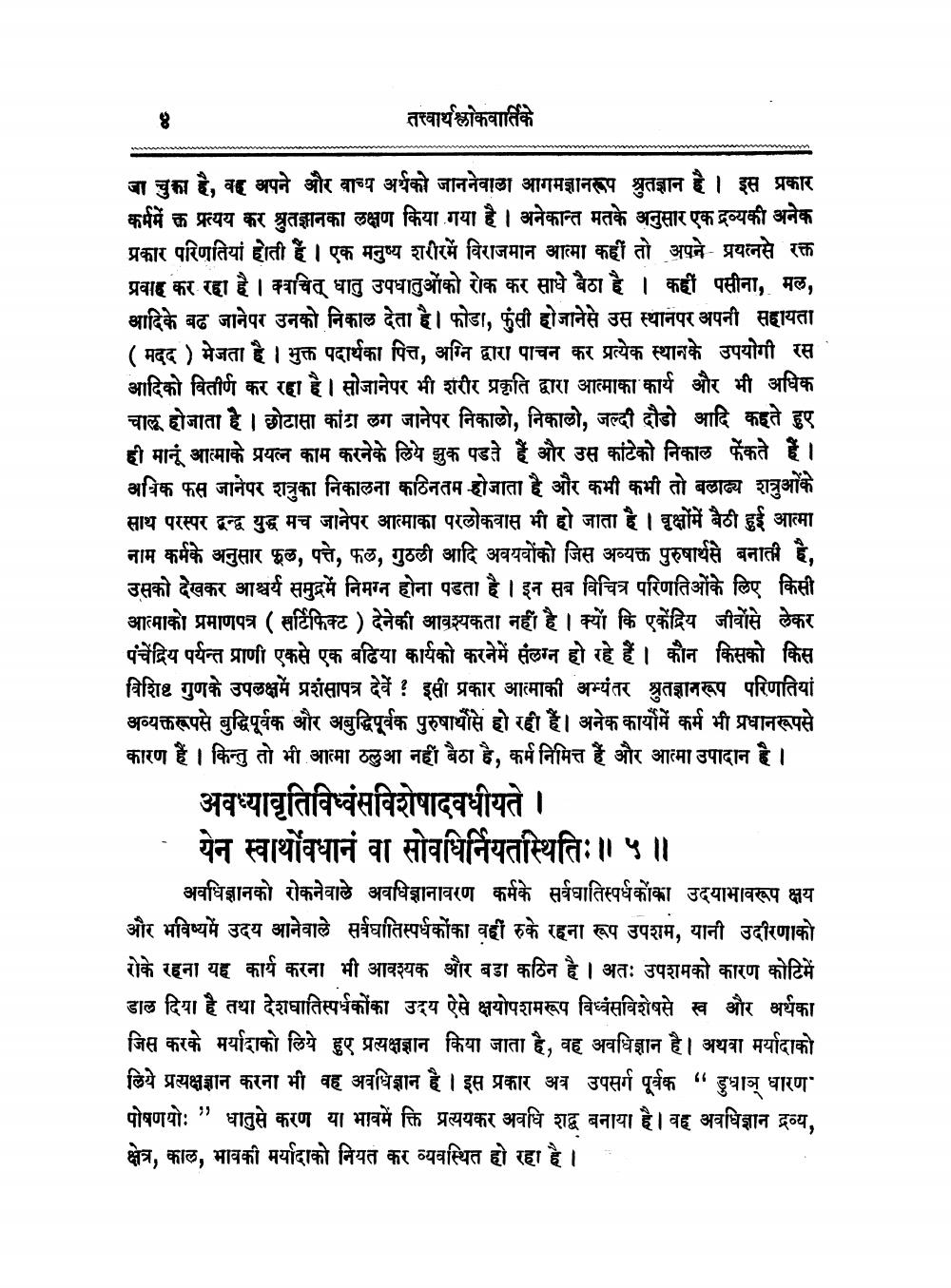________________
तस्वार्थश्लोकवार्तिके
जा चुका है, वह अपने और वाच्य अर्थको जाननेवाला आगमज्ञानरूप श्रुतज्ञान है । इस प्रकार कर्म प्रत्यय कर श्रुतज्ञानका लक्षण किया गया है । अनेकान्त मतके अनुसार एक द्रव्यकी अनेक प्रकार परिणतियां होती हैं । एक मनुष्य शरीर में विराजमान आत्मा कहीं तो अपने प्रयत्नसे रक्त प्रवाह कर रहा है । क्वचित् धातु उपधातुओं को रोक कर साधे बैठा है । कहीं पसीना, मल, आदिके बढ जानेपर उनको निकाल देता है। फोडा, फुंसी होजानेसे उस स्थानपर अपनी सहायता ( मदद ) मेजता है । भुक्त पदार्थका पित्त, अग्नि द्वारा पाचन कर प्रत्येक स्थानके उपयोगी रस आदिको वितीर्ण कर रहा है । सोजानेपर भी शरीर प्रकृति द्वारा आत्माका कार्य और भी अधिक चालू होजाता है । छोटासा कांटा लग जानेपर निकालो, निकालो, जल्दी दौडो आदि कहते हुए मनूं आत्मा प्रयत्न काम करनेके लिये झुक पडते हैं और उस कांटेको निकाल फेंकते हैं । अत्रिक फस जानेपर शत्रुका निकालना कठिनतम होजाता है और कभी कभी तो बलाढ्य शत्रुओं के साथ परस्पर द्वन्द्व युद्ध मच जानेपर आत्माका परलोकवास भी हो जाता है । वृक्षोंमें बैठी हुई आत्मा नाम कर्म अनुसार फूल, पत्ते, फल, गुठली आदि अवयवोंको जिस अव्यक्त पुरुषार्थसे बनाती है, उसको देखकर आश्चर्य समुद्र में निमग्न होना पडता है । इन सब विचित्र परिणतिओंके लिए किसी आत्माको प्रमाणपत्र ( सर्टिफिक्ट ) देने की आवश्यकता नहीं है । क्यों कि एकेंद्रिय जीवोंसे लेकर 1 पंचेंद्रिय पर्यन्त प्राणी एकसे एक बढिया कार्यको करनेमें संलग्न हो रहे हैं। कौन किसको किस विशिष्ट गुणके उपलक्ष में प्रशंसापत्र देवें ! इसी प्रकार आत्माकी अभ्यंतर श्रुतज्ञानरूप परिणतियां अव्यक्तरूपसे बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक पुरुषार्थोंसे हो रही हैं। अनेक कार्यों में कर्म भी प्रधानरूपसे कारण हैं । किन्तु तो भी आत्मा ठलुआ नहीं बैठा है, कर्म निमित्त हैं और आत्मा उपादान है ।
1
अवध्यावृतिविध्वंसविशेषादवधीयते । स्वार्थोवधानं वासोवधिर्नियतस्थितिः ॥ ५ ॥
अवधिज्ञानको रोकनेवाले अवधिज्ञानावरण कर्मके सर्वघातिस्पर्धकोंका उदयाभावरूप क्षय और भविष्य में उदय आनेवाले सर्वघातिस्पर्धकों का वहीं रुके रहना रूप उपशम, यानी उदीरणाको रोके रहना यह कार्य करना भी आवश्यक और बड़ा कठिन है । अतः उपशमको कारण कोटिमें डाल दिया है तथा देशघातिस्पर्धकोंका उदय ऐसे क्षयोपशमरूप विध्वंसविशेषसे स्व और अर्थका जिस करके मर्यादाको लिये हुए प्रत्यक्षज्ञान किया जाता है, वह अवधिज्ञान है । अथवा मर्यादाको लिये प्रत्यक्षज्ञान करना भी वह अवधिज्ञान है । इस प्रकार अत्र उपसर्गपूर्वक " डुधाञ् धारण पोषणयोः " धातुसे करण या भावमें क्ति प्रत्ययकर अवधि शब्द बनाया है । वह अवधिज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी मर्यादाको नियत कर व्यवस्थित हो रहा है ।
४