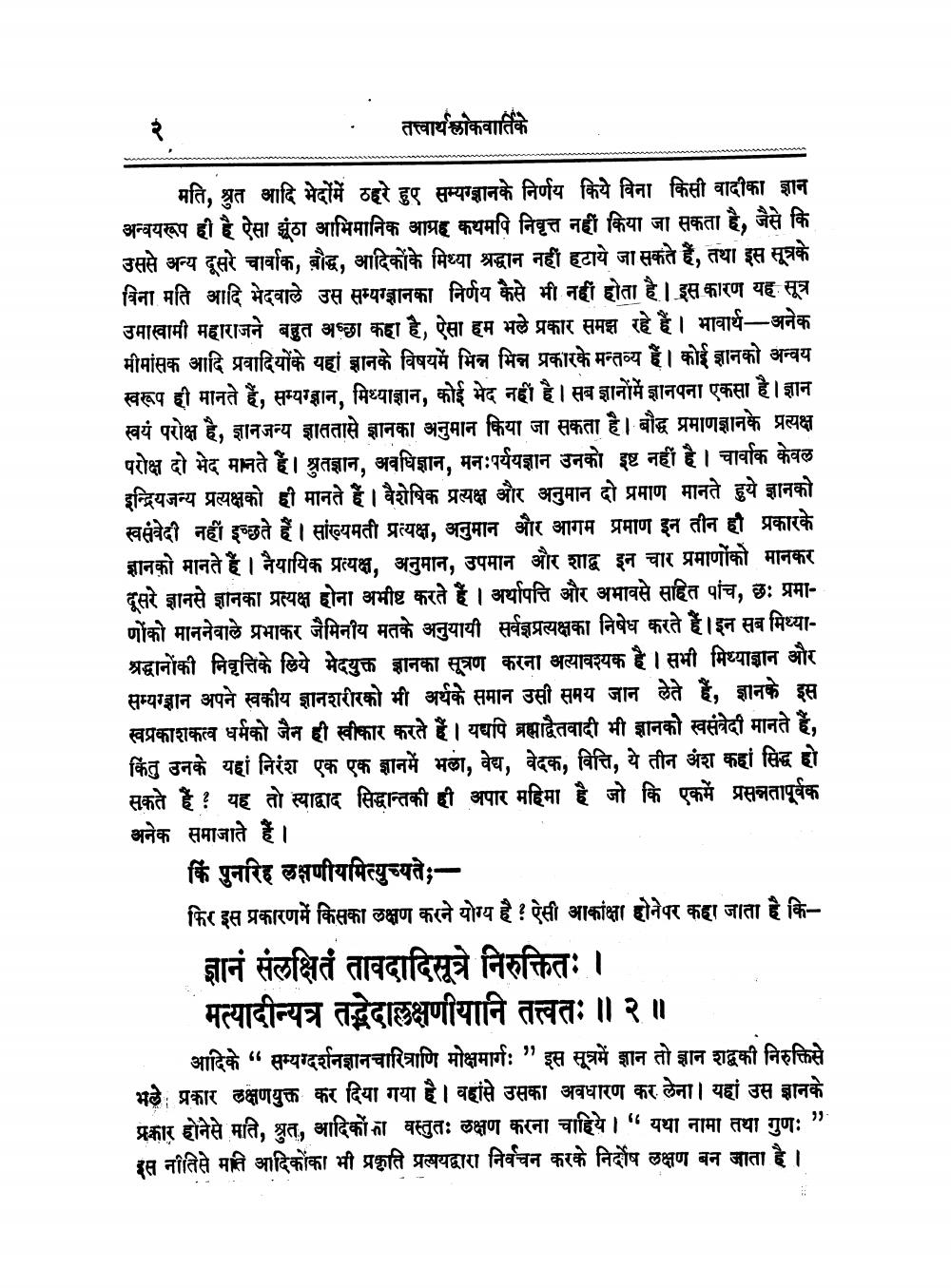________________
.
तत्त्वार्यश्लोकवार्तिके
मति, श्रुत आदि भेदोंमें ठहरे हुए सम्यग्ज्ञानके निर्णय किये विना किसी वादीका ज्ञान अन्वयरूप ही है ऐसा झूठा आमिमानिक आग्रह कथमपि निवृत्त नहीं किया जा सकता है, जैसे कि उससे अन्य दूसरे चार्वाक, बौद्ध, आदिकोंके मिथ्या श्रद्धान नहीं हटाये जा सकते हैं, तथा इस सूत्रके विना मति आदि भेदवाले उस सम्यग्ज्ञानका निर्णय कैसे भी नहीं होता है। इस कारण यह सूत्र उमाखामी महाराजने बहुत अच्छा कहा है, ऐसा हम भले प्रकार समझ रहे हैं। भावार्थ-अनेक मीमांसक आदि प्रवादियोंके यहां ज्ञान के विषयमें भिन्न भिन्न प्रकारके मन्तव्य हैं। कोई ज्ञानको अन्वय स्वरूप ही मानते हैं, सम्यग्ज्ञान, मिथ्याज्ञान, कोई भेद नहीं है। सब ज्ञानोंमें ज्ञानपना एकसा है। ज्ञान स्वयं परोक्ष है, ज्ञानजन्य ज्ञाततासे ज्ञानका अनुमान किया जा सकता है। बौद्ध प्रमाणज्ञानके प्रत्यक्ष परोक्ष दो भेद मानते हैं। श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान उनको इष्ट नहीं है । चार्वाक केवल इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षको ही मानते हैं । वैशेषिक प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण मानते हुये ज्ञानको स्वसंवेदी नहीं इच्छते हैं। सांख्यमती प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाण इन तीन ही प्रकारके ज्ञानको मानते हैं । नैयायिक प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शाद इन चार प्रमाणोंको मानकर दूसरे ज्ञानसे ज्ञानका प्रत्यक्ष होना अभीष्ट करते हैं । अर्थापत्ति और अमावसे सहित पांच, छः प्रमाणोंको माननेवाले प्रभाकर जैमिनीय मतके अनुयायी सर्वज्ञप्रत्यक्षका निषेध करते हैं। इन सब मिथ्याश्रद्धानोंकी निवृत्तिके लिये मेदयुक्त ज्ञानका सूत्रण करना अत्यावश्यक है। सभी मिथ्याज्ञान और सम्यग्ज्ञान अपने स्वकीय ज्ञानशरीरको भी अर्थके समान उसी समय जान लेते हैं, ज्ञानके इस खप्रकाशकत्व धर्मको जैन ही स्वीकार करते हैं। यद्यपि ब्रह्माद्वैतवादी भी ज्ञानको स्वसंवेदी मानते हैं, किंतु उनके यहां निरंश एक एक ज्ञानमें मला, वेद्य, वेदक, वित्ति, ये तीन अंश कहां सिद्ध हो सकते हैं ? यह तो स्याद्वाद सिद्धान्तकी ही अपार महिमा है जो कि एकमें प्रसन्नतापूर्वक अनेक समाजाते हैं।
किं पुनरिह लक्षणीयमित्युच्यतेफिर इस प्रकारणमें किसका लक्षण करने योग्य है ! ऐसी आकांक्षा होनेपर कहा जाता है कि
ज्ञानं संलक्षितं तावदादिसूत्रे निरुक्तितः । मत्यादीन्यत्र तद्भेदालक्षणीयानि तत्त्वतः॥२॥
आदिके " सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः " इस सूत्रमें ज्ञान तो ज्ञान शब्दकी निरुक्तिसे भले प्रकार लक्षणयुक्त कर दिया गया है। वहांसे उसका अवधारण कर लेना। यहां उस ज्ञानके प्रकार होनेसे मति, श्रुत, आदिकों का वस्तुतः लक्षण करना चाहिये । " यथा नामा तथा गुणः " इस नीतिसे मति आदिकोंका भी प्रकृति प्रलयद्वारा निर्वचन करके निर्दोष लक्षण बन जाता है।