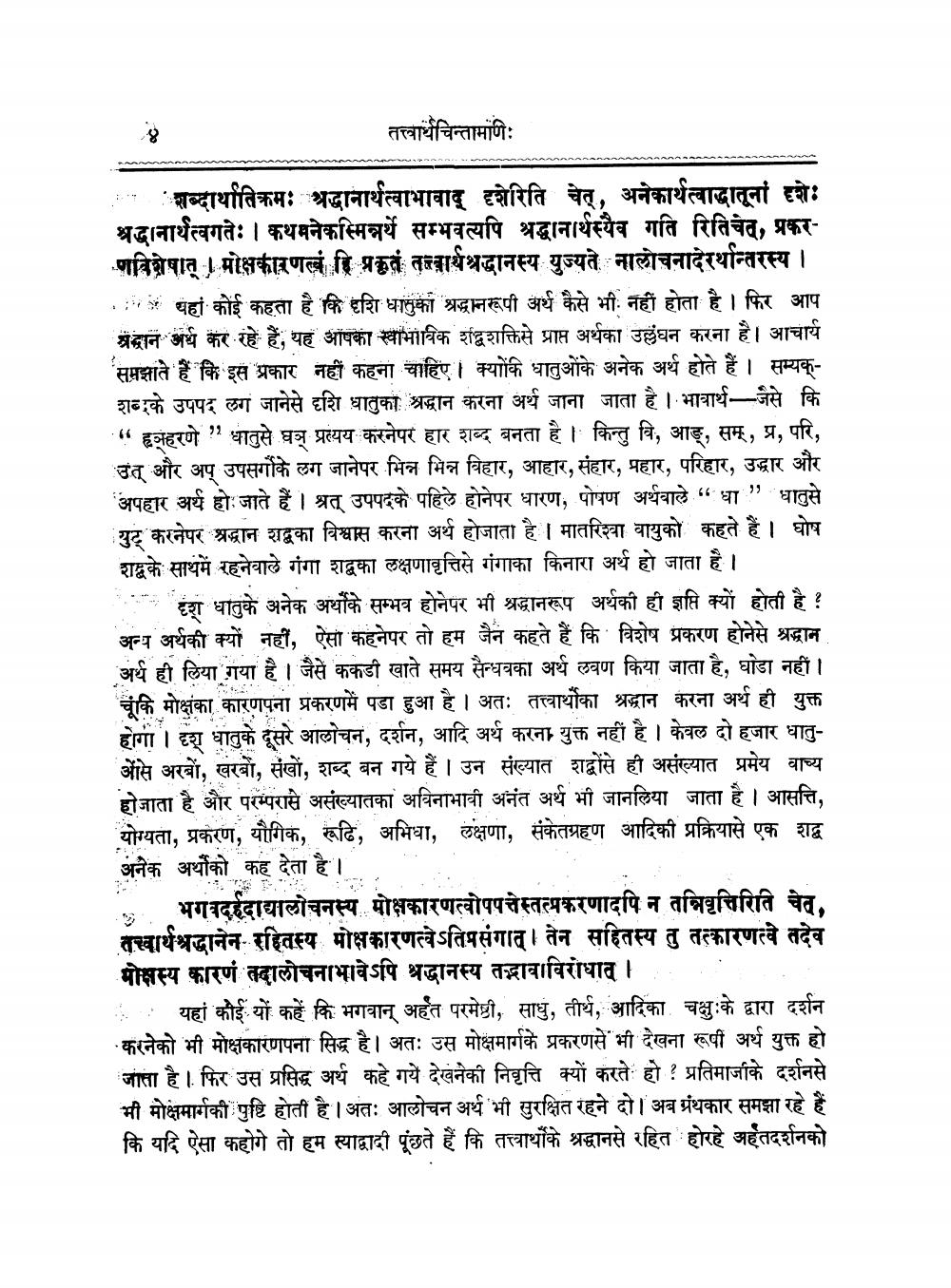________________
तत्त्वार्थेचिन्तामणिः
शब्दार्थातिक्रमः श्रद्धानार्थत्वाभावाद् दृशेरिति चेत्, अनेकार्थत्वाद्धातूनां दृशेः श्रद्धानार्थत्वगतेः । कथमनेकस्मिन्नर्थे सम्भवत्यपि श्रद्धानार्थस्यैव गति रितिचेत्, प्रकर-णविशेषात् । मोक्षकारणत्वं हि प्रकृतं तत्त्वार्थश्रद्धानस्य युज्यते नालोचनादेरर्थान्तरस्य ।
यहां कोई कहता है कि दृशि धातुका श्रद्धानरूपी अर्थ कैसे भी नहीं होता है। फिर आप श्रद्वान अर्थ कर रहे हैं, यह आपका स्वाभाविक शद्वशक्तिसे प्राप्त अर्थका उल्लंघन करना है। आचार्य समझाते हैं कि इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। क्योंकि धातुओंके अनेक अर्थ होते हैं । सम्यक्शब्द उपपद लग जानेसे दृशि धातुका श्रद्धान करना अर्थ जाना जाता है । भावार्थ जैसे कि " हृञ् हरणे " धातुसे घञ् प्रत्यय करनेपर हार शब्द बनता है । किन्तु वि, आङ्, सम्, प्र, परि, उत् और अप् उपसर्गौके लग जानेपर भिन्न भिन्न विहार, आहार, संहार, प्रहार, परिहार, उद्धार और 'अपहार अर्थ हो जाते हैं । श्रत् उपपदके पहिले होनेपर धारण, पोषण अर्थवाले “ धा धातुसे युद्ध करनेपर श्रद्धान शद्वका विश्वास करना अर्थ होजाता है । मातरिश्वा वायुको कहते हैं । घोष रावके साथ में रहनेवाले गंगा शद्वका लक्षणावृत्तिसे गंगाका किनारा अर्थ हो जाता है ।
""
दृश् धातुके अनेक अर्थोके सम्भव होनेपर भी श्रद्धानरूप अर्थकी ही ज्ञप्ति क्यों होती है ? अन्य अर्थकी क्यों नहीं, ऐसा कहनेपर तो हम जैन कहते हैं कि विशेष प्रकरण होनेसे श्रद्धान अर्थ ही लिया गया है । जैसे ककडी खाते समय सैन्धवका अर्थ लवण किया जाता है, घोडा नहीं । चूंकि मोक्षका कारणपना प्रकरणमें पडा हुआ है । अतः तत्त्वार्थीका श्रद्धान करना अर्थ ही युक्त होगा । दृश् धातुके दूसरे आलोचन, दर्शन, आदि अर्थ करना युक्त नहीं है । केवल दो हजार धातुअसे अरबों, खरबों, संखों, शब्द बन गये हैं । उन संख्यात शद्वोंसे ही असंख्यात प्रमेय वाच्य हो जाता है और परम्परासे असंख्यातका अविनाभावी अनंत अर्थ भी जानलिया जाता है । आसत्ति, योग्यता, प्रकरण, यौगिक, रूढि, अभिधा, लक्षणा, संकेतग्रहण आदिकी प्रक्रियासे एक शब्द अनेक अर्थोको कह देता है ।
भगवदईदाद्यालोचनस्य मोक्षकारणत्वोपपत्तेस्तत्प्रकरणादपि न तन्निवृत्तिरिति चेत्, तस्वार्थ श्रद्धानेन रहितस्य मोक्षकारणत्वेऽतिप्रसंगात् । तेन सहितस्य तु तत्कारणत्वे तदेव मोक्षस्य कारणं तदालोचनाभावेऽपि श्रद्धानस्य तद्भावाविरोधात् ।
यहां कोई यों कहें कि भगवान् अर्हत परमेष्ठी, साधु, तीर्थ, आदिका चक्षुः के द्वारा दर्शन • करने को भी मोक्षकारणपना सिद्ध है । अतः उस मोक्षमार्गके प्रकरणसे भी देखना रूपी अर्थ युक्त हो जाता है । फिर उस प्रसिद्ध अर्थ कहे गये देखनेकी निवृत्ति क्यों करते हो ? प्रतिमाजीके दर्शनसे भी मोक्षमार्ग पुष्टि होती है । अतः आलोचन अर्थ भी सुरक्षित रहने दो। अब ग्रंथकार समझा रहे हैं कि यदि ऐसा कहोगे तो हम स्याद्वादी पूंछते हैं कि तत्त्वार्थोके श्रद्धानसे रहित होरहे अर्हतदर्शनको