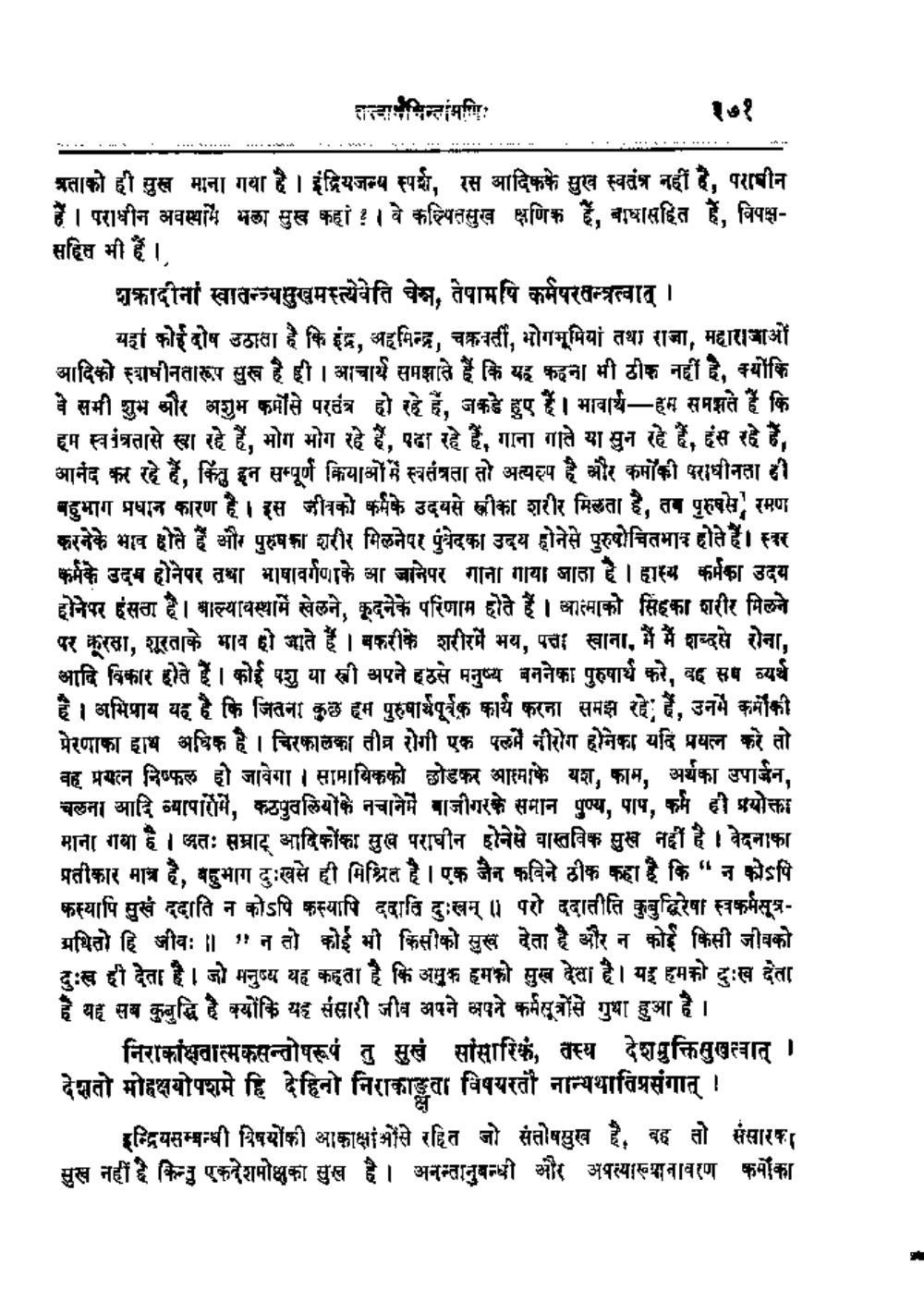________________
चिन्तामणिः
१७१
ता को ही सुख माना गया है। इंद्रियजन्य स्पर्श, रस आदिकके सुख स्वतंत्र नहीं है, पराधीन हैं । पराधीन अवस्था मला सुख कहां ? | वे कल्पितसुख क्षणिक हैं, वाघासहित हैं, विपक्षसहित भी हैं।
शक्रादीनां स्वातन्त्र्य सुखमस्त्येवेति चेन, तेषामपि कर्मपरतन्त्रत्वात् ।
4
3
कोई दोष उठाता है कि इंद्र, अहमिन्द्र, चक्रवर्ती, भोगभूमियां तथा राजा, महाराजाओं आदिको स्वाधीनतारूप सुख है ही । आचार्य समझाते हैं कि यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वे सभी शुभ और अशुभ कर्मोंसे परतंत्र हो रहे हैं, जकड़े हुए हैं। भावार्थ- हम समझते हैं कि हम स्वतंत्रता से खा रहे हैं, भोग भोग रहे हैं, पढा रहे हैं, गाना गाते या सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, किंतु इन सम्पूर्ण क्रियाओं में स्वतंत्रता तो अत्यल्प है और कमोंकी पराधीनता ही बहुभाग प्रधान कारण है। इस जीवको कर्मके उदयसे स्त्रीका शरीर मिलता है, तब पुरुषसे रमण करनेके भाव होते हैं और पुरुषका शरीर मिलनेवर पुंवेदका उदय होनेसे पुरुषोचितभाव होते हैं। स्वर कर्मके उदय होनेपर तथा भाषावणाके आ जानेपर गाना गाया जाता है । हास्य कर्मका उदय होनेपर हंसता है । बाल्यावस्था में खेलने कूदनेके परिणाम होते हैं। आत्माको सिंहका शरीर मिलने पर क्रूरता, शूरता के भाव हो जाते हैं। बकरीके शरीर में भय, पत्ता खाना, मैं मैं शब्दसे रोना, आदि विकार होते हैं । कोई पशु या स्त्री अपने इसे मनुष्य बननेका पुरुषार्थ करे, वह सब व्यर्थ है । अभिप्राय यह है कि जितना कुछ हम पुरुषार्थपूर्वक कार्य करना समझ रहे हैं, उनमें कमकी प्रेरणाका air afte है । चिरकालका तीव्र रोगी एक पलमें नीरोग होने का यदि प्रयत्न करे तो वह प्रयत्न निष्फल हो जावेगा । सामायिकको छोडकर आत्माके यश, काम, अर्थका उपार्जन, चलना आदि व्यापारोंमें, कठपुतलियों के नचाने में बाजीगर के समान पुण्य, पाप, कर्म ही प्रयोक्ता माना गया है । अतः सम्राट् आदिकोंका सुख पराधीन होनेसे वास्तविक सुख नहीं है । वेदनाका प्रतीकार मात्र है, बहुभाग दुःखसे ही मिश्रित है । एक जैन कविने ठीक कहा है कि " न कोऽपि कस्यापि सुखं ददाति न कोऽपि कस्यापि ददाति दुःखन् परो ददातीति कुबुद्धिरेषा स्वकर्मसूत्रप्रधितो हि जीवः ॥ " न तो कोई भी किसीको सुख देता है और न कोई किसी जीवको दुःख ही देता है। जो मनुष्य यह कहता है कि अमुक हमको सुख देता है। यह हमको दुःख देता है यह सब कुबुद्धि है क्योंकि यह संसारी जीव अपने अपने कर्मसूत्रोंसे गुथा हुआ है ।
I
।
निराकांक्षवात्मक सन्तोषरूपं तु सुखं सांसारिकं तस्य देशमुक्तिसुखत्वात् । देशतो मोक्षयोपशमे हि देहिनो निराकाङ्क्षता विषयस्तौ नान्यथाविप्रसंगात् ।
इन्द्री आकाक्षाओंसे रहित जो संतोषसुख है, वह तो संसारका सुख नहीं है किन्तु एकदेशमोक्षका सुख है । अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानावरण कर्मों का