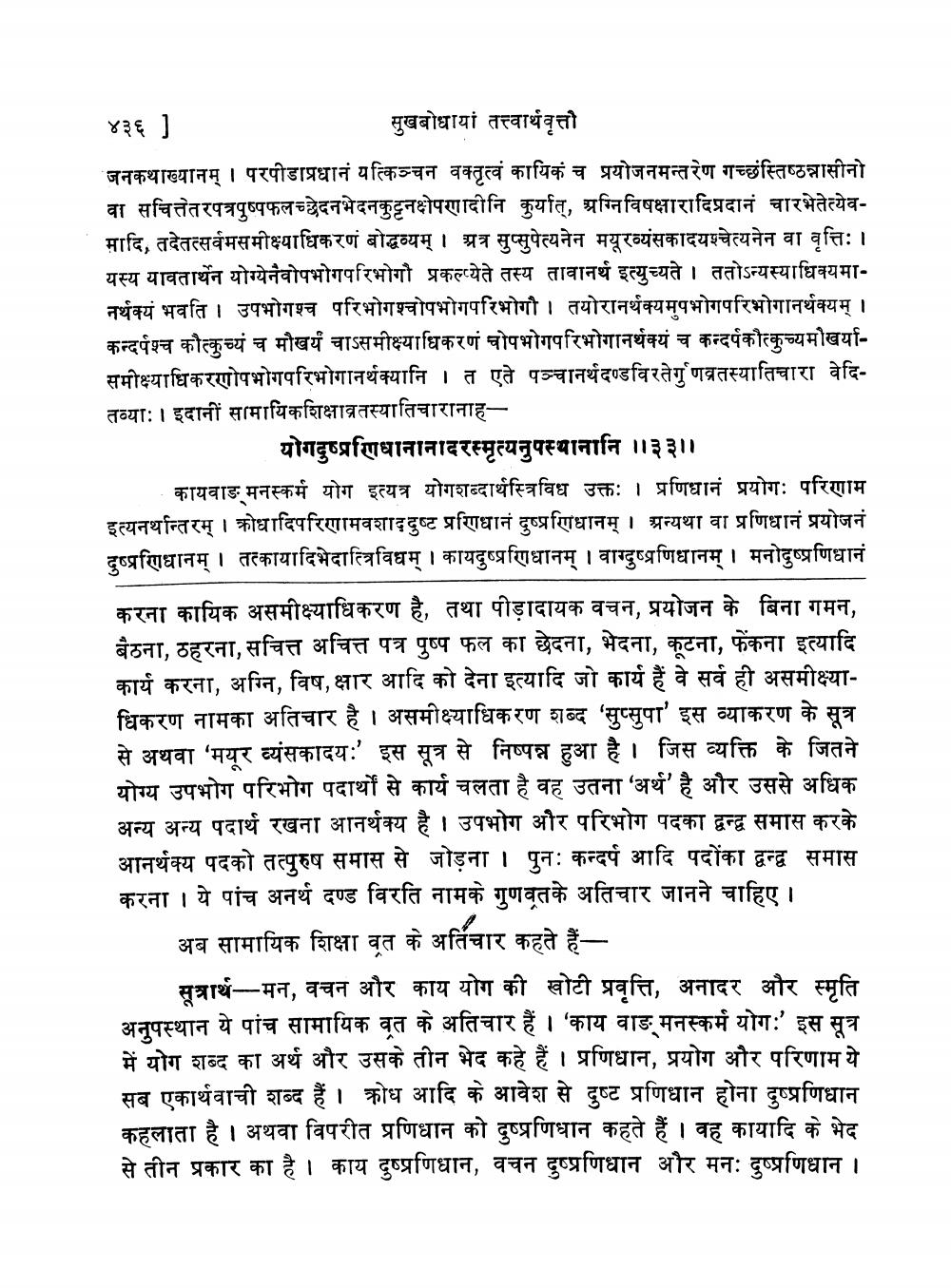________________
४३६ ]
सुखबोधायां तत्त्वार्थवृत्ती जनकथाख्यानम् । परपीडाप्रधानं यत्किञ्चन वक्तृत्वं कायिकं च प्रयोजनमन्तरेण गच्छंस्तिष्ठन्नासीनो वा सचित्तेतरपत्रपुष्पफलच्छेदनभेदनकुट्टनक्षेपणादीनि कुर्यात्, अग्निविषक्षारादिप्रदानं चारभेतेत्येवमादि, तदेतत्सर्वमसमीक्ष्याधिकरणं बोद्धव्यम् । अत्र सुप्सुपेत्यनेन मयूरव्यंसकादयश्चेत्यनेन वा वृत्तिः । यस्य यावतार्थेन योग्येनैवोपभोगपरिभोगौ प्रकल्प्येते तस्य तावानर्थ इत्युच्यते । ततोऽन्यस्याधिक्यमानर्थक्यं भवति । उपभोगश्च परिभोगश्चोपभोगपरिभोगौ। तयोरानर्थक्यमुपभोगपरिभोगानर्थक्यम् । कन्दर्पश्च कौत्कुच्यं च मौखयं चाऽसमीक्ष्याधिकरणं चोपभोगपरिभोगानर्थक्यं च कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्यासमीक्ष्याधिकरणोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि । त एते पञ्चानर्थदण्डविरतेगुणवतस्यातिचारा वेदितव्याः । इदानीं सामायिकशिक्षाव्रतस्यातिचारानाह
योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥३३॥ - कायवाङ मनस्कर्म योग इत्यत्र योगशब्दार्थस्त्रिविध उक्तः । प्रणिधानं प्रयोगः परिणाम इत्यनन्तरम् । क्रोधादिपरिणामवशाददुष्ट प्रणिधानं दुष्प्रणिधानम् । अन्यथा वा प्रणिधानं प्रयोजनं दुष्प्रणिधानम् । तत्कायादिभेदात्त्रिविधम् । कायदुष्प्रणिधानम् । वाग्दुष्प्रणिधानम् । मनोदुष्प्रणिधानं करना कायिक असमीक्ष्याधिकरण है, तथा पीड़ादायक वचन, प्रयोजन के बिना गमन, बैठना, ठहरना, सचित्त अचित्त पत्र पुष्प फल का छेदना, भेदना, कूटना, फेंकना इत्यादि कार्य करना, अग्नि, विष, क्षार आदि को देना इत्यादि जो कार्य हैं वे सर्व ही असमीक्ष्याधिकरण नामका अतिचार है । असमीक्ष्याधिकरण शब्द 'सुप्सुपा' इस व्याकरण के सूत्र से अथवा 'मयूर व्यंसकादयः' इस सूत्र से निष्पन्न हुआ है। जिस व्यक्ति के जितने योग्य उपभोग परिभोग पदार्थों से कार्य चलता है वह उतना 'अर्थ' है और उससे अधिक अन्य अन्य पदार्थ रखना आनर्थक्य है । उपभोग और परिभोग पदका द्वन्द्व समास करके आनर्थक्य पदको तत्पुरुष समास से जोड़ना । पुनः कन्दर्प आदि पदोंका द्वन्द्व समास करना । ये पांच अनर्थ दण्ड विरति नामके गुणवतके अतिचार जानने चाहिए।
अब सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार कहते हैं
सूत्रार्थ-मन, वचन और काय योग की खोटी प्रवृत्ति, अनादर और स्मृति अनुपस्थान ये पांच सामायिक व्रत के अतिचार हैं । 'काय वाङ मनस्कर्म योगः' इस सूत्र में योग शब्द का अर्थ और उसके तीन भेद कहे हैं । प्रणिधान, प्रयोग और परिणाम ये सब एकार्थवाची शब्द हैं। क्रोध आदि के आवेश से दुष्ट प्रणिधान होना दुष्प्रणिधान कहलाता है । अथवा विपरीत प्रणिधान को दुष्प्रणिधान कहते हैं । वह कायादि के भेद से तीन प्रकार का है। काय दुष्प्रणिधान, वचन दुष्प्रणिधान और मनः दुष्प्रणिधान ।