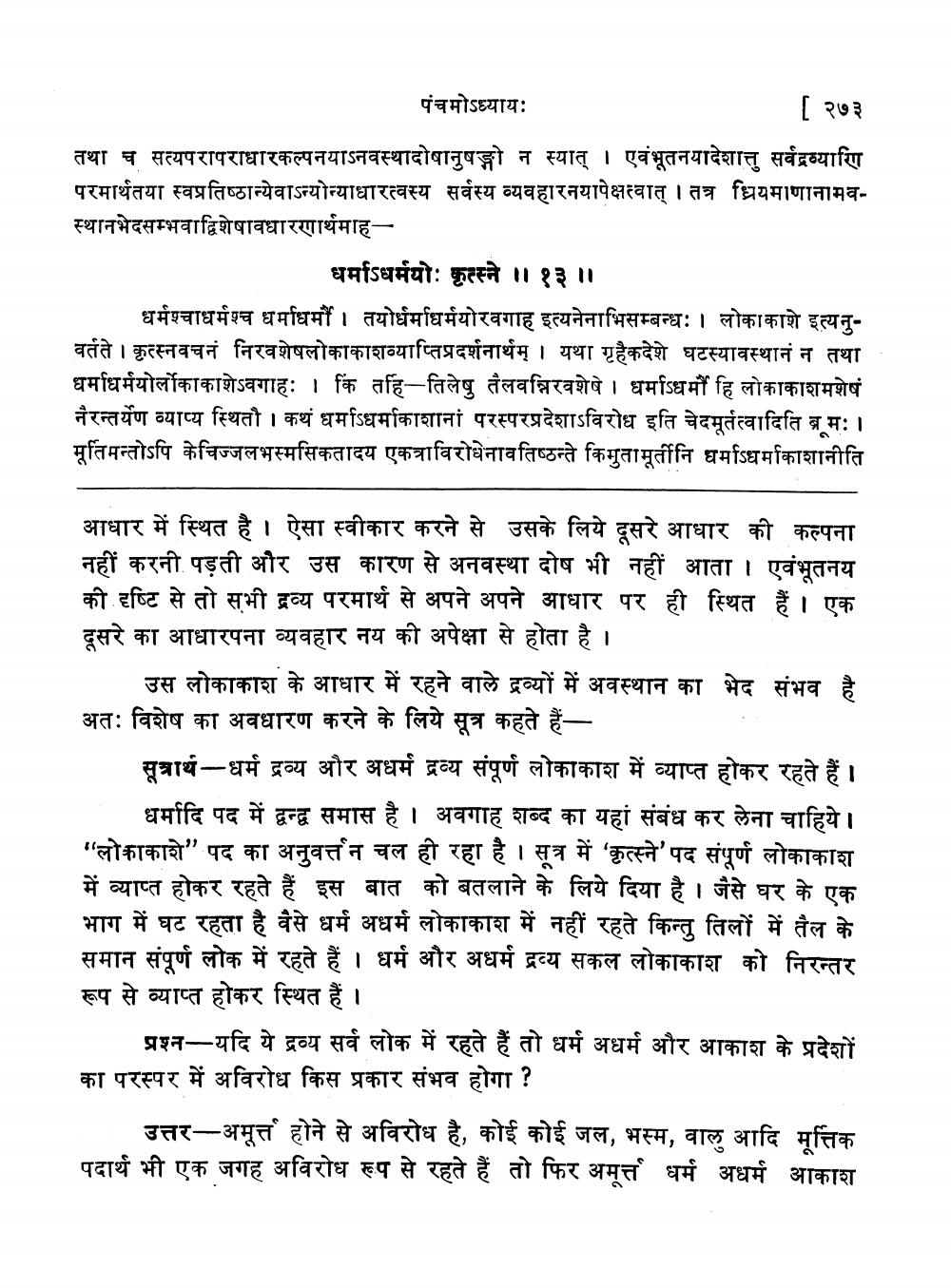________________
पंचमोऽध्यायः
[ २७३ तथा च सत्यपरापराधारकल्पनयाऽनवस्थादोषानुषङ्गो न स्यात् । एवंभूतनयादेशात्तु सर्वद्रव्याणि परमार्थतया स्वप्रतिष्ठान्येवाऽन्योन्याधारत्वस्य सर्वस्य व्यवहारनयापेक्षत्वात् । तत्र ध्रियमाणानामवस्थानभेदसम्भवाद्विशेषावधारणार्थमाह
धर्माऽधर्मयोः कृत्स्ने ॥१३॥ ____धर्मश्चाधर्मश्च धर्माधर्मों। तयोर्धर्माधर्मयोरवगाह इत्यनेनाभिसम्बन्धः । लोकाकाशे इत्यनुवर्तते । कृत्स्नवचनं निरवशेषलोकाकाशव्याप्तिप्रदर्शनार्थम् । यथा गृहैकदेशे घटस्यावस्थानं न तथा धर्माधर्मयोर्लोकाकाशेऽवगाहः । किं तर्हि-तिलेषु तैलवन्निरवशेषे । धर्माऽधौं हि लोकाकाशमशेषं नैरन्तर्येण व्याप्य स्थितौ । कथं धर्माऽधर्माकाशानां परस्परप्रदेशाऽविरोध इति चेदमूर्तत्वादिति ब्रमः । मूर्तिमन्तोऽपि केचिज्जलभस्मसिकतादय एकत्राविरोधेनावतिष्ठन्ते किमुतामूर्तीनि धर्माऽधर्माकाशानीति
आधार में स्थित है। ऐसा स्वीकार करने से उसके लिये दूसरे आधार की कल्पना नहीं करनी पड़ती और उस कारण से अनवस्था दोष भी नहीं आता । एवंभूतनय की दृष्टि से तो सभी द्रव्य परमार्थ से अपने अपने आधार पर ही स्थित हैं। एक दूसरे का आधारपना व्यवहार नय की अपेक्षा से होता है ।
उस लोकाकाश के आधार में रहने वाले द्रव्यों में अवस्थान का भेद संभव है अतः विशेष का अवधारण करने के लिये सूत्र कहते हैं
सूत्रार्थ-धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त होकर रहते हैं ।
धर्मादि पद में द्वन्द्व समास है । अवगाह शब्द का यहां संबंध कर लेना चाहिये। "लोकाकाशे" पद का अनुवर्तन चल ही रहा है । सूत्र में 'कृत्स्ने' पद संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त होकर रहते हैं इस बात को बतलाने के लिये दिया है। जैसे घर के एक भाग में घट रहता है वैसे धर्म अधर्म लोकाकाश में नहीं रहते किन्तु तिलों में तैल के समान संपूर्ण लोक में रहते हैं । धर्म और अधर्म द्रव्य सकल लोकाकाश को निरन्तर रूप से व्याप्त होकर स्थित हैं।
प्रश्न-यदि ये द्रव्य सर्व लोक में रहते हैं तो धर्म अधर्म और आकाश के प्रदेशों का परस्पर में अविरोध किस प्रकार संभव होगा?
उत्तर-अमूर्त होने से अविरोध है, कोई कोई जल, भस्म, वालु आदि मूर्तिक पदार्थ भी एक जगह अविरोध रूप से रहते हैं तो फिर अमूर्त धर्म अधर्म आकाश