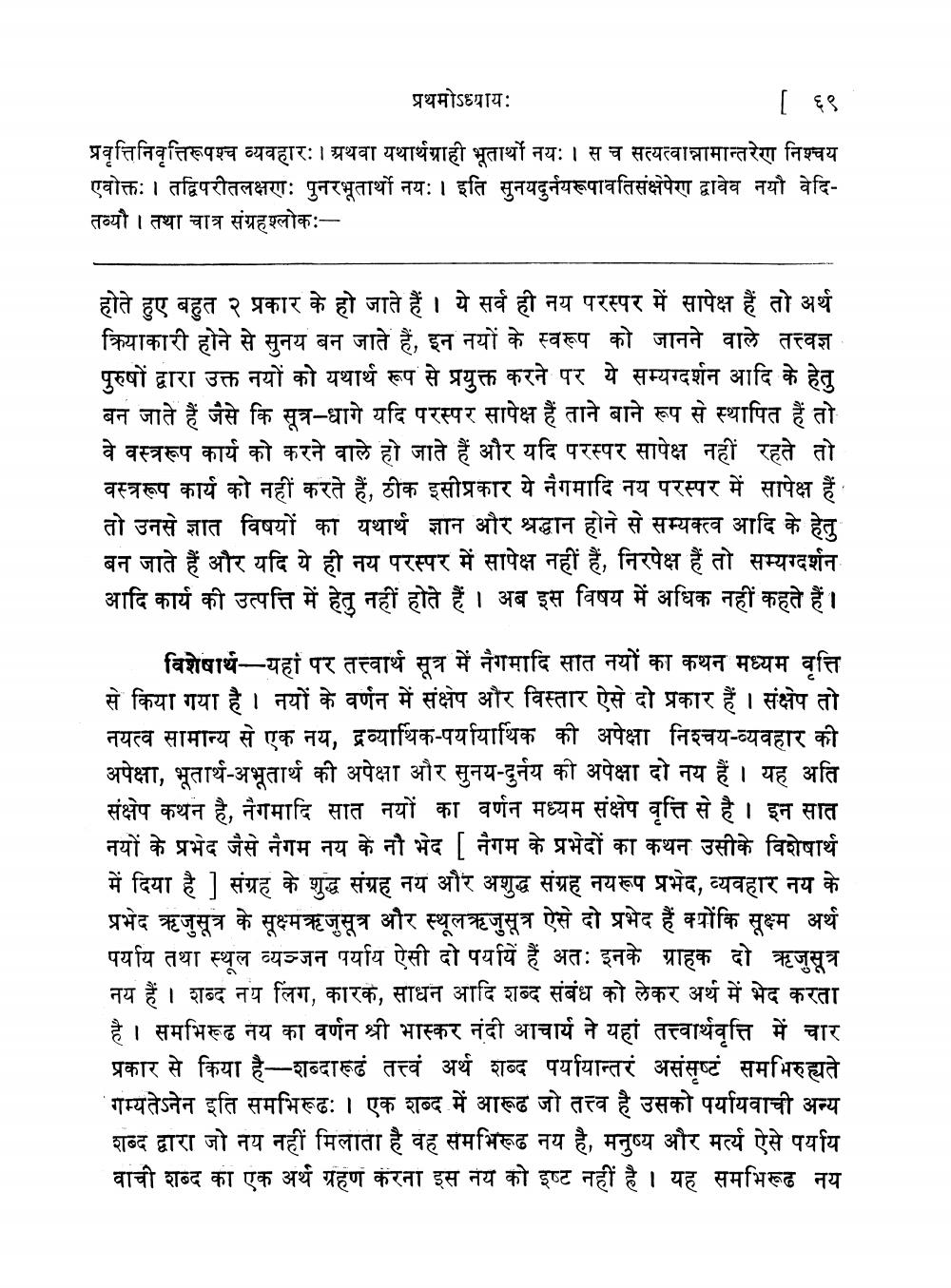________________
प्रथमोऽध्यायः
प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपश्च व्यवहारः । अथवा यथार्थग्राही भूतार्थो नयः । स च सत्यत्वान्नामान्तरेण निश्चय एवोक्तः । तद्विपरीतलक्षण: पुनरभूतार्थो नयः । इति सुनयदुर्नयरूपावतिसंक्षेपेण द्वावेव नयौ वेदितव्यौ । तथा चात्र संग्रहश्लोकः
होते हुए बहुत २ प्रकार के हो जाते हैं। ये सर्व ही नय परस्पर में सापेक्ष हैं तो अर्थ क्रियाकारी होने से सुनय बन जाते हैं, इन नयों के स्वरूप को जानने वाले तत्त्वज्ञ पुरुषों द्वारा उक्त नयों को यथार्थ रूप से प्रयुक्त करने पर ये सम्यग्दर्शन आदि के हेतु बन जाते हैं जैसे कि सूत्र-धागे यदि परस्पर सापेक्ष हैं ताने बाने रूप से स्थापित हैं तो वे वस्त्ररूप कार्य को करने वाले हो जाते हैं और यदि परस्पर सापेक्ष नहीं रहते तो वस्त्ररूप कार्य को नहीं करते हैं, ठीक इसीप्रकार ये नैगमादि नय परस्पर में सापेक्ष हैं तो उनसे ज्ञात विषयों का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान होने से सम्यक्त्व आदि के हेतु बन जाते हैं और यदि ये ही नय परस्पर में सापेक्ष नहीं हैं, निरपेक्ष हैं तो सम्यग्दर्शन आदि कार्य की उत्पत्ति में हेतु नहीं होते हैं । अब इस विषय में अधिक नहीं कहते हैं।
विशेषार्थ-यहां पर तत्त्वार्थ सूत्र में नैगमादि सात नयों का कथन मध्यम वृत्ति से किया गया है । नयों के वर्णन में संक्षेप और विस्तार ऐसे दो प्रकार हैं । संक्षेप तो नयत्व सामान्य से एक नय, द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक की अपेक्षा निश्चय-व्यवहार की अपेक्षा, भूतार्थ-अभूतार्थ की अपेक्षा और सुनय-दुर्नय की अपेक्षा दो नय हैं। यह अति संक्षेप कथन है, नैगमादि सात नयों का वर्णन मध्यम संक्षेप वृत्ति से है । इन सात नयों के प्रभेद जैसे नैगम नय के नौ भेद [ नैगम के प्रभेदों का कथन उसीके विशेषार्थ में दिया है ] संग्रह के शुद्ध संग्रह नय और अशुद्ध संग्रह नयरूप प्रभेद, व्यवहार नय के प्रभेद ऋजुसूत्र के सूक्ष्मऋजुसूत्र और स्थूलऋजुसूत्र ऐसे दो प्रभेद हैं क्योंकि सूक्ष्म अर्थ पर्याय तथा स्थूल व्यञ्जन पर्याय ऐसी दो पर्यायें हैं अतः इनके ग्राहक दो ऋजुसूत्र नय हैं । शब्द नय लिंग, कारक, साधन आदि शब्द संबंध को लेकर अर्थ में भेद करता है। समभिरूढ नय का वर्णन श्री भास्कर नंदी आचार्य ने यहां तत्त्वार्थवृत्ति में चार प्रकार से किया है-शब्दारूढं तत्त्वं अर्थ शब्द पर्यायान्तरं असंसृष्टं समभिरुह्यते गम्यतेऽनेन इति समभिरूढः । एक शब्द में आरूढ जो तत्त्व है उसको पर्यायवाची अन्य शब्द द्वारा जो नय नहीं मिलाता है वह समभिरूढ नय है, मनुष्य और मर्त्य ऐसे पर्याय वाची शब्द का एक अर्थ ग्रहण करना इस नय को इष्ट नहीं है । यह समभिरूढ नय