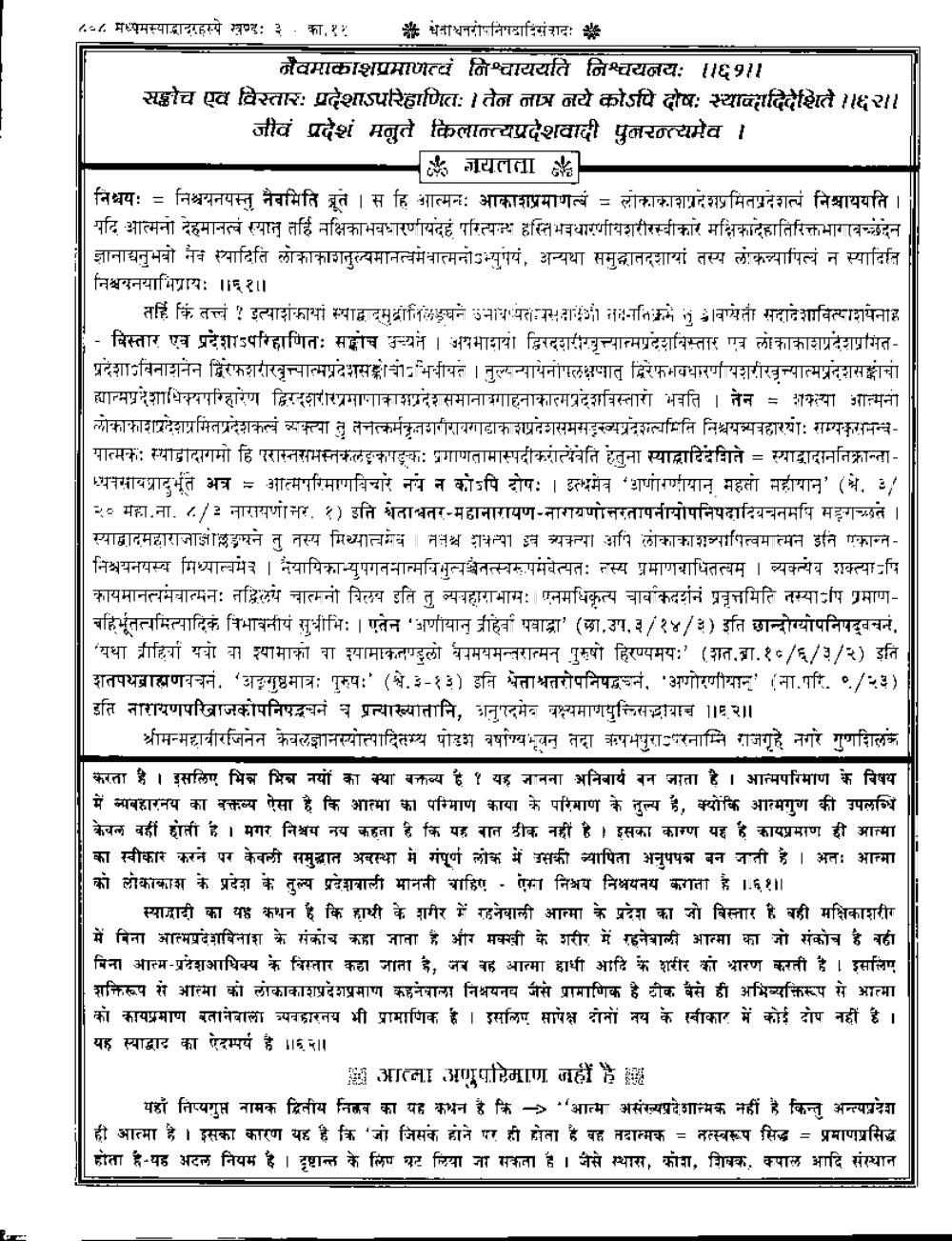________________
८०८८ मध्यमस्याद्वाद रहस्ये खण्ड ३ का. १४ * धेताश्वतरोपनिषदादिसंसदः
जैवमाकाशप्रमाणत्वं निश्वाययति निश्चयनयः ॥ ६१॥ सङ्कोच एवं विस्तार : प्रदेशाऽपरिहाणित: । तेन नात्र नये कोऽपि दोष: स्थाव्दादिदेशिते ॥६॥ जीवं प्रदेशं मनुते किलान्त्यप्रदेशवादी पुनरन्त्यमेव । * जयलता
निश्वयः = निश्वयनयस्तु नैवमिति ब्रूते । स हि आत्मन: आकाशप्रमाणत्वं लोकाकाशप्रदेशप्रमितप्रदेशत्वं निश्वाययति । यदि आत्मनो देहमानत्वं स्यात् तर्हि नक्षिकामवधारणीयदहं परित्यज्य हस्तिभवधारणीयशरीरस्वीकारे मक्षिकादेहातिरिक्तभागगवच्छेदन ज्ञानाद्यनुभवो नैव स्वादिति लोकाकाशमुल्यमानत्वमेवात्मनोऽभ्युपेयं, अन्यथा समुद्रातदशायां तस्य लोकन्यापित्वं न स्यादिति निश्चरनयाभिप्रायः ॥ ६२॥
तर्हि किं तत्त्वं ॥ इत्याशंकास्पद
दतक्रमे
ती सदादेशावित्याशयेनाह
विस्तार एव प्रदेशाsपरिहाणितः सङ्कोच उच्यते । अयमादायां द्विरददारीरवृत्त्यात्मप्रदेशविस्तार एवं लोकाकाशप्रदेशप्रमितप्रदेशाऽविनाशनेन द्विरेफशरीरवृत्यात्मप्रदेशसङ्कोचीऽभिचयते । तुल्यन्यायेनोपलक्षणात् द्विरेफभवधारणीयशरीरवृन्यात्मप्रदेशसङ्कांची ह्यात्मप्रदेशाधिक्यपरिहारेण द्विरदाराप्रमाणाकाशप्रदेशसमानावगाहनाकात्मप्रदेशविस्तारो भवति । तेन = शक्त्या आत्मना लोकाकाशप्रदेशप्रमितप्रदेशकत्वं व्यक्त्या तु तचत्कर्मकृतशरीरावणढाकाशप्रदेशसमसत्यप्रदेशत्वमिति निश्वमभ्यवहारयोः सम्यक समन्व यात्मकः स्याद्वादागमो हि परास्तसमस्तकलकपक: प्रमाणतामास्पदीकरोत्येवेति हेतुना स्याद्रादिदेशिते = स्याद्वादानतिक्रान्ताव्यवसायप्रादुर्भूत अत्र = आत्मपरिमाणविचारे नये न कोऽपि दोषः । इत्थमेव 'अणोरणीयान महतो महीयान' (भे. ३) २० महा.ना. ८/३ नारायणोत्तर १) इति वेताश्वतर- महानारायण नारायणोत्तरतापनीयोपनिषदादिवचनमपि मगच्छते । स्याद्वादमहाराजाझील्लङघने तु तस्य मिथ्यात्वमेव नाव व्यक्त्या अपि लोकाकाशव्यापित्वमात्मन इति एकान्ननिश्रयनयस्व मिध्यात्वमंत्र । नैयायिकाभ्युपगतनात्मविभुत्वश्चैतत्स्वरूपमेवेत्यतः तस्य प्रमाणवाधितत्वम् । व्यक्त्येव शक्त्यापि कायमानत्वमंचात्मनः तद्विलये चात्मनी विलय इति तु व्यवहाराभासः । एनमधिकृत्य चावदिदर्शनं प्रवृत्तमिति तस्याऽपि प्रमाणबहिर्भूतत्वमित्यादिकं विभावनीयं सुधीभिः । एतेन 'अणीयान् जीव वाद्रा' (छा.उप. ३/१४/३) इति छान्दोग्योपनिषदुवचनं, "यथा त्रीहियवी वा श्यामाको वा श्यामाकतण्डुलमन्तरात्मन पुरुषो हिरण्यमयः' (शत.ब्रा. १०/६/३/२) इति शतपथब्राह्मणवचनं 'अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषः' (श्र.३ - १३) इति वेताश्वतरोपनिषद्वचनं, 'अणोरणीयान (मा. परि. ९ / २३) इति नारायणपरिखाजकोपनिषदचनं च प्रत्याख्यातानि धनुरदमेव वक्ष्यमाणसिद्धावाच ॥६२॥
श्रीमन्महावीरजिनेन केवलज्ञानस्योत्पादितस्य पोडशवर्षायभूत तदा ऋषभपुराऽपरनाम्नि राजगृहे नगरे गुणशिलंक
=
ני
करता है । इसलिए भिन्न भिन्न नयों का क्या वक्तव्य है ? यह जानना अनिवार्य बन जाता है । आत्मपरिमाण के विषय में व्यवहारनय का वक्तव्य ऐसा है कि आत्मा का परिमाण काया के परिमाण के तुल्य है, क्योंकि आत्मगुण की उपलब्धि केवल वहीं होती है। मगर निश्चय नय कहता है कि यह बात ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कायप्रमाण ही आत्मा का स्वीकार करने पर केवली समुद्रात अवस्था में संपूर्ण लोक में उसकी व्यापिता अनुपपन्न बन जाती है । अतः आत्मा को लोकाकाश के प्रदेश के तुल्य प्रदेशवाली माननी चाहिए ऐसा निश्रय निश्रयनय कराता है ।.६१।।
स्यानादी का यह कथन है कि हाथी के शरीर में रहनेवाली आत्मा के प्रदेश का जो विस्तार है वही मक्षिकाशरीर में बिना आत्मप्रदेशविनाश के संकोच कहा जाता है और Heat के शरीर में रहनेवाली आत्मा का जो संकोच है वही बिन्दा आत्म-प्रदेशआधिक्य के विस्तार कहा जाता है, जब वह आत्मा हाथी आदि के शरीर को धारण करती है। इसलिए शक्तिरूप से आत्मा को लोकाकाशप्रदेशप्रमाण कहनेवाला निश्रयनव जैसे प्रामाणिक है ठीक वैसे ही अभिव्यक्तिरूप से आत्मा को कार्यप्रमाण बतानेवाला व्यवहारनय भी प्रामाणिक है । इसलिए सापेक्ष दोनों नय के स्वीकार में कोई दोष नहीं है । यह स्याद्वाद का ऐदम्पर्य है ||5||
आत्मा अणुपरिमाण नहीं है
यहाँ तिप्यगुप्त नामक द्वितीय free का यह कथन है कि
"आत्मा असंत्यप्रदेशात्मक नहीं है किन्तु अन्त्यप्रदेश ही आत्मा है । इसका कारण यह है कि 'जो जिसके होने पर ही होता है वह तदात्मक = तत्स्वरूप सिद्ध प्रमाणप्रसिद्ध होता है - यह अटल नियम है । दृष्टान्त के लिए लिया जा सकता है। जैसे स्थास, कोश, शिवक, कपाल आदि संस्थान
=