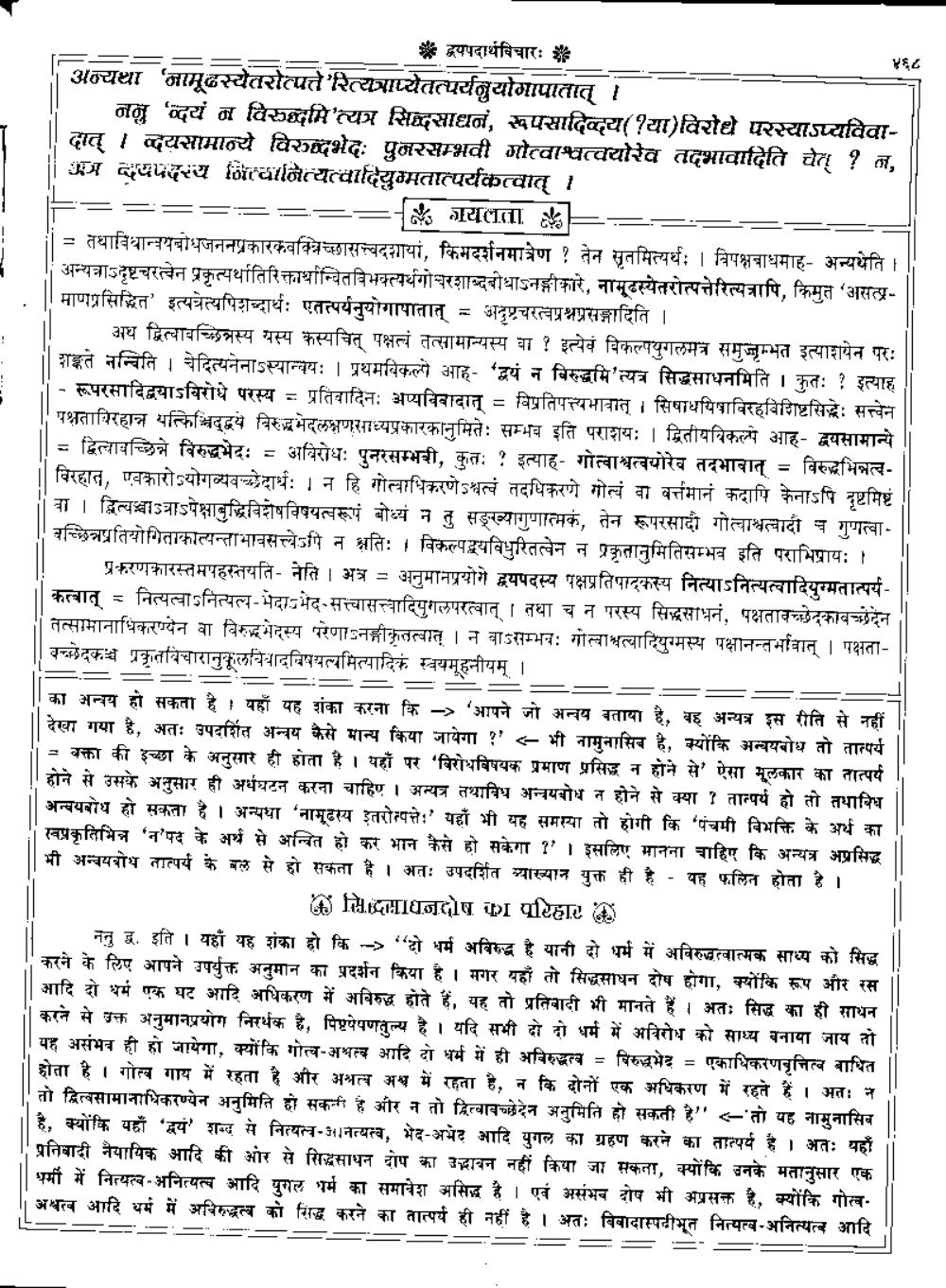________________
४६८
*द्वयपदार्थविचारः* अन्यथा 'नामूढस्येतरोत्पत्ते'रित्यत्राप्येतत्यर्यनुयोगापातात् ।
ननु 'ब्दयं न विरुदमि'त्यत्र सिन्दसाधनं, रूपसादिब्दय(?या)विरोधे परस्याऽप्यविवादात् । व्दयसामान्ये विरुदभेदः पुनरसम्भवी गोत्वाश्वत्वयोरेव तदभावादिति चेत् ? न,
मा दयपदस्य forallनत्यत्वादियुग्मतात्पर्यकत्वात् ।। =========ायलता *=1 = तथाविधान्वयबोधजननप्रकारकवक्वेिच्छासत्वदशायां, किमदर्शनमात्रेण ? तेन सृतमित्यर्थः । विपक्षबाधमाह- अन्यथेति ।
अन्यत्राऽदृष्टचरत्वेन प्रकृत्यातिरिक्तार्यान्वितविभक्त्यर्थगोचरशाब्दबोधाऽनङ्गीकारे, नामूढस्येतरोत्पत्तेरित्यत्रापि, किमुत 'असत्प्र| माण्णप्रसिद्धित' इत्यत्रेत्यपिशब्दार्थः एतत्पर्यनुयोगापातात् = अदृष्टचरत्वप्रश्नप्रसङ्गादिति ।
अथ द्वित्वावच्छित्रस्य यस्य कस्यचित् पक्षत्वं तत्सामान्यस्य वा ? इत्येवं विकल्पयुगलमत्र समजम्भत इत्याशयेन परः शकते नन्विति । चेदित्यनेनाऽस्यान्वयः । प्रथमविकणे आह- 'द्वयं न विरुद्धमि त्यत्र सिद्धसाधनमिति । कुतः । इत्याह - रूपरसादिद्वयाऽविरोधे परस्य = प्रतिवादिनः अप्यविवादात = विप्रतिपत्त्यभावात । सिषाधयिषाविरहविशिष्टसिद्धेः सत्त्वेन पश्नताविरहान्न यत्किञ्चिद्वये विरुद्धभेदलक्षणसाव्यप्रकारकानुमितेः सम्भव इति पराशयः । द्वितीयविकल्पे आह-द्वयसामान्ये = द्वित्वावच्छिन्ने विरुद्धभेदः = अविरोधः पुनरसम्भरी, कुतः ? इत्याह- गोत्वाश्वत्वयोरेव तदभावात् = विरुद्भभिन्नत्वविरहात, एवकारोच्योगव्यवच्छेदार्थः । न हि गोत्वाधिकरणेऽश्वत्वं तदधिकरणे गोत्वं वा वर्तमानं कदापि केनाऽपि दृष्टमिष्टं वा । द्वित्वञ्चाऽत्राऽपेक्षाबुद्भिविशेषविषयत्वरूपं बोध्यं न तु सङ्ख्यागुणात्मकं, तेन रूपरसादी गोत्वाश्वत्वादी च गुणत्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाल्यन्ताभावसत्त्वेऽपि न अतिः । विकल्पद्यविधुरितत्वेन न प्रकृतानुमितिसम्भव इति पराभिप्रायः ।।
प्रकरणकारस्तमपहस्तयति- नेति । अत्र = अनुमानप्रयोगे द्वयपदस्य पक्षप्रतिपादकस्य नित्यानित्यत्वादियुग्मतात्पर्य - कत्वात् = नित्यत्वाऽनित्यत्य-भेदाभेद सत्त्वासत्त्वादियुगलपरत्वात् । तथा च न परस्य सिद्धसाधनं, पक्षतावच्छेदकावच्छंदन तत्सामानाधिकरण्येन वा विरुद्धभेदस्य 'परेणाऽनङ्गीकृतत्वात् । न बाऽसम्भवः गोत्वाश्चत्वादियुग्मस्य पक्षानन्तर्भावात् । पक्षताबच्छेदकच प्रकृतविचारानुकूलविवादविषयत्वमित्यादिकं स्वयमहनीयम् ।
का अन्वय हो सकता है। यहाँ यह शंका करना कि -> 'आपने जो अन्वय बताया है, वह अन्यत्र इस रीति से नहीं देखा गया है, अतः उपदर्शित अन्वय कैसे मान्य किया जायेगा ?' -भी नामुनासिब है, क्योंकि अन्वयबोध तो तात्पर्य = वक्ता की इच्छा के अनुसार ही होता है। यहाँ पर 'विरोधविषयक प्रमाण प्रसिद्ध न होने से ऐसा मूलकार का तात्पर्य होने से उसके अनुसार ही अर्थघटन करना चाहिए । अन्यत्र तथाविध अन्वयबोध न होने से क्या ? तात्पर्य हो तो तथाविध अन्वयबोध हो सकता है। अन्यथा 'नामूढस्य इतरोत्पत्तेः' यहाँ भी यह समस्या तो होगी कि 'पंचमी विभक्ति के अर्थ का स्वप्रकृतिभिन्न 'न पद के अर्थ से अन्चित हो कर भान कैसे हो सकेगा ?' । इसलिए मानना चाहिए कि अन्यत्र अप्रसिद्ध भी अन्चयबोध नात्पर्य के बल से हो सकता है । अतः उपदर्शित व्याख्यान युक्त ही है - यह फलिन होता है ।
0 सि.साधनदोष का परिहार ननु दू. इति । यहाँ यह शंका हो कि -> "दो धर्म अविरुद्ध है यानी दो धर्म में अविरुद्धत्वात्मक साध्य को सिद्ध करने के लिए आपने उपर्युक्त अनुमान का प्रदर्शन किया है। मगर यहाँ तो सिद्धसाधन दोष होगा, क्योंकि रूप और रस आदि दो धर्म एक घट आदि अधिकरण में अविरुद्ध होते हैं, यह तो प्रतिवादी भी मानते हैं। अतः सिद्ध का ही साधन करने से उक्त अनुमानप्रयोग निरर्थक है, पिष्टषेपणतुल्य है। यदि सभी दो दो धर्म में अविरोध को साध्य बनाया जाय तो यह असंभव ही हो जायेगा, क्योंकि गोत्व-अश्रस्व आदि दो धर्म में ही अविरुद्धत्व = विरुद्धभेद = एकाधिकरणवृत्तित्व बाधित होता है । गोत्व गाय में रहता है और अबत्व अश्व में रहता है, न कि दोनों एक अधिकरण में रहते हैं । अतः न तो द्वित्वसामानाधिकरण्येन अनुमिति हो सकती है और न तो द्वित्वावच्छेदेन अनुमिति हो सकती है" -'तो यह नामुनासिब है, क्योंकि यहाँ 'द्वयं' शब्द से नित्यत्व-नित्यत्व, भेद-अभेद आदि युगल का ग्रहण करने का तात्पर्य है । अतः यहाँ प्रतिवादी नैयायिक आदि की ओर से सिद्धसाधन दोप का उद्भावन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके मतानुसार एक धर्मी में नित्यत्व अनित्यत्व आदि पुगल धर्म का समावेश असिद्ध है । एवं असंभव दोष भी अप्रसक्त है, क्योंकि गोत्वअश्वत्व आदि धर्म में अविरुद्धत्व को सिद्ध करने का तात्पर्य ही नहीं है। अतः विवादास्पदीभूत नित्यत्व-अनित्यत्व आदि