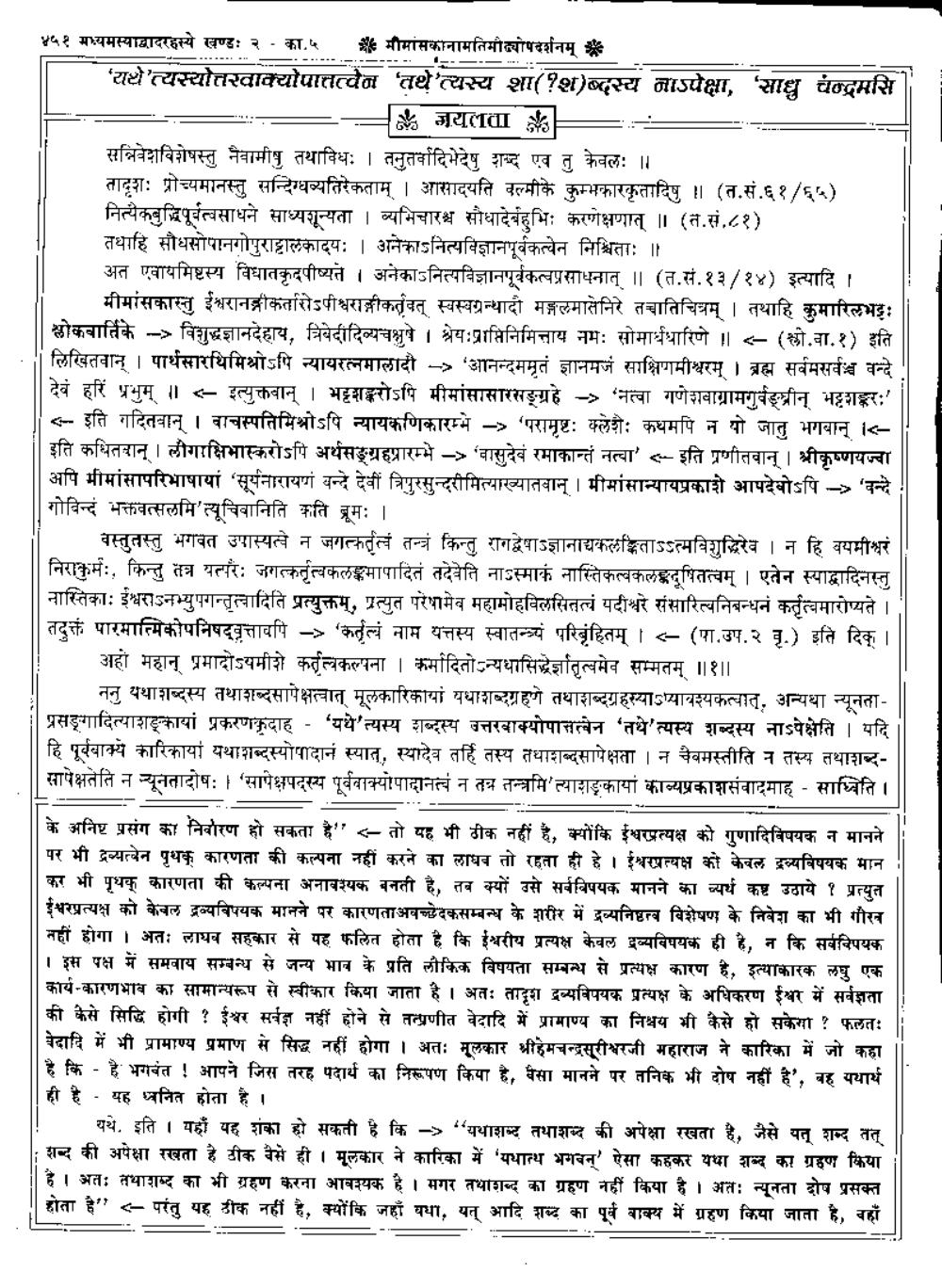________________
४५१ मध्यमस्याद्वादरहस्ये खण्डः २ - का.५ * मीमांसकानामतिमोत्योपदर्शनम् * 'राधे'त्यस्योत्तरवाक्योपात्तत्वेन 'तथे त्यस्य शा(?)ब्दस्य नाऽपेक्षा, 'साधु चन्द्रमसि]
--..-== =* जयलता * = = सन्निवेशविशेषस्तु नैवामीषु तथाविधः । तनुतर्वादिभेदेषु शब्द एव तु केवलः ।। तादृशः प्रोच्यमानस्तु सन्दिग्धव्यतिरेकताम् । आसादयति इल्मीके कुम्भकारकृतादिषु ।। (त.सं.६१/६५) नित्यैकबद्भिपूर्वत्वसाधने साध्यशन्यता । व्यभिचारश्च सौधादेर्बहुभिः करणेक्षणात || (त.सं.८१) तथाहि सौधसोपानगोपुराट्टालकादयः । अनेकाऽनित्यविज्ञानपूर्वकत्वेन निश्चिताः ॥ अत एवायमिष्टस्य विधातकृदपीष्यते । अनेकाऽनित्यविज्ञानपूर्वकत्वप्रसाधनात् ।। (त.सं.१३/१४) इत्यादि ।
मीमांसकास्तु ईश्वरानङ्गीकर्तारोऽपीश्वराङ्गीकर्तृवत् स्वस्वग्रन्थादौ मङ्गलमासेनिरे तच्चातिचित्रम् । तथाहि कुमारिलभट्टः श्लोकवार्तिके --> विशुद्धज्ञानदेहाय, त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे । श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे || - (श्लो.वा.१) इति लिखितवान् । पार्थसारथिमिश्रोऽपि न्यायरत्नमालादौ --> 'आनन्दममृतं ज्ञानमजं साक्षिणमीश्वरम् । ब्रह्म सर्वमसर्वञ्च वन्दे ! देवं हरिं प्रभुम् ॥ - इत्युक्तवान् । भट्टशङ्करोऽपि मीमांसासारसङ्ग्रहे → 'नत्वा गणेशवाग्रामगुर्वङ्क्रीन् भट्टशङ्करः'
- इति गदितवान् । वाचस्पतिमिश्रोऽपि न्यायकणिकारम्भे -> 'परामृष्टः क्लेशः कथमपि न यो जातु भगवान् ।<इति कधितरान् । लौगाक्षिभास्करोऽपि अर्थसङ्ग्रहप्रारम्भे -> 'वासुदेवं रमाकान्तं नत्वा' - इति प्रणीतवान् । श्रीकृष्णयज्वा अपि मीमांसापरिभाषायां 'सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीमित्याख्यातवान् । मीमांसान्यायप्रकाशे आपदेवोऽपि -> 'वन्दे ! गोबिन्दं भक्तवत्सलमि'त्यूचिवानिति कति ब्रूमः ।
वस्तुतस्तु भगवत उपास्यत्वे न जगत्कर्तृत्वं तन्त्रं किन्तु रागद्वेषाऽज्ञानाद्यकविताऽऽत्मविशुद्धिरेव । न हि वयमीश्वरं निराकुर्मः, किन्तु तत्र यत्परः जगत्कर्तृत्वकलङ्कमापादितं तदेवेति नाऽस्माकं नास्तिकत्वकलङ्कदूषितत्वम् । एतेन स्पाद्वादिनस्तु नास्तिकाः ईश्वराऽनभ्युपगन्तृत्वादिति प्रत्युक्तम्, प्रत्युत परेषामेव महामोहविलसितत्वं यदीश्वरे संसारित्वनिबन्धनं कर्तृत्वमारोप्यते । तदुक्तं पारमात्मिकोपनिषवृत्तावपि -> 'कर्तृत्वं नाम यत्तस्य स्वातन्त्र्यं परिबृंहितम् । ८- (पा.उप.२ वृ.) इति दिक् ।
अहो महान् प्रमादोऽयमीशे कर्तृत्वकल्पना । कर्मादितोऽन्यथासिद्धेातृत्वमेव सम्मतम् ||१||
ननु यथाशब्दस्य तथाशब्दसापेक्षत्वात् मूलकारिकायां यधाशब्दग्रहणे तथाशब्दग्रहस्याऽण्यावश्यकत्वात्, अन्यथा न्यूनताप्रसङ्गादित्याशङ्कायां प्रकरणकृदाह - 'यथे' त्यस्य शब्दस्य उत्तरवाक्योपात्तत्त्वेन 'तथे' त्यस्य शब्दस्य नाऽपेक्षेति । यदि हि पूर्ववाक्ये कारिकायां यथाशब्दस्योपादानं स्यात्, स्यादेव तर्हि तस्य तधाशब्दसापेक्षता । न चैवमस्तीति न तस्य तथाशब्दसापेक्षतेति न न्यूनतादोषः । 'सापेक्षपदस्य पूर्ववाक्योपादानत्वं न तत्र तन्त्रमि'त्याशङ्कायां काव्यप्रकाशसंवादमाह - साध्विति ।
के अनिष्ट प्रसंग का निवारण हो सकता है" - तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ईश्वरप्रत्यक्ष को गुणादिविषयक न मानने पर भी द्रव्यत्वेन पृथक् कारणता की कल्पना नहीं करने का लाधब तो रहता ही है। ईश्वरप्रत्यक्ष को केवल द्रव्यविषयक मान कर भी पृथक् कारणता की कल्पना अनावश्यक बनती है, तब क्यों उसे सर्व विषयक मानने का व्यर्थ कष्ट उठाये १ प्रत्युत ईश्वरप्रत्यक्ष को केवल द्रव्यविषयक मानने पर कारणताअवच्छेदकसम्बन्ध के शरीर में द्रव्यनिष्ठत्व विशेषण के निवेश का भी गौरव नहीं होगा । अतः लायव सहकार से यह फलित होता है कि ईश्वरीय प्रत्यक्ष केवल द्रव्यविषयक ही है, न कि सर्वविषयक । इस पक्ष में समवाय सम्बन्ध से जन्य भाव के प्रति लौकिक विषयता सम्बन्ध से प्रत्यक्ष कारण है, इत्याकारक लघु एक कार्य-कारणभाव का सामान्यरूप से स्वीकार किया जाता है। अतः तादृश द्रव्यविषयक प्रत्यक्ष के अधिकरण ईश्वर में सर्वज्ञता की कैसे सिद्धि होगी ? ईश्वर सर्वज्ञ नहीं होने से तत्प्रणीत वेदादि में प्रामाण्य का निश्चय भी कैसे हो सकेगा ? फलतः वेदादि में भी प्रामाण्य प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा । अतः मूलकार श्रीहेमचन्द्रसूरीश्वरजी महाराज ने कारिका में जो कहा है कि - है भगवंत ! आपने जिस तरह पदार्थ का निरूपण किया है, वैसा मानने पर तनिक भी दोष नहीं है', वह यथार्थ ही है . यह वनित होता है।
यथे. इति । यहाँ यह शंका हो सकती है कि -> "यथाशब्द तथाशब्द की अपेक्षा रखता है, जैसे यत् शब्द तत् । शब्द की अपेक्षा रखता है ठीक वैसे ही । मूलकार ने कारिका में 'यथात्थ भगवन्' ऐसा कहकर यथा शब्द का ग्रहण किया
है । अतः तथाशब्द का भी ग्रहण करना आवश्यक है। मगर तथाशब्द का ग्रहण नहीं किया है । अतः न्यूनता दोष प्रसक्त | होता है" - परंतु यह ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ यथा, यत् आदि शब्द का पूर्व वाक्य में ग्रहण किया जाता है, वहाँ