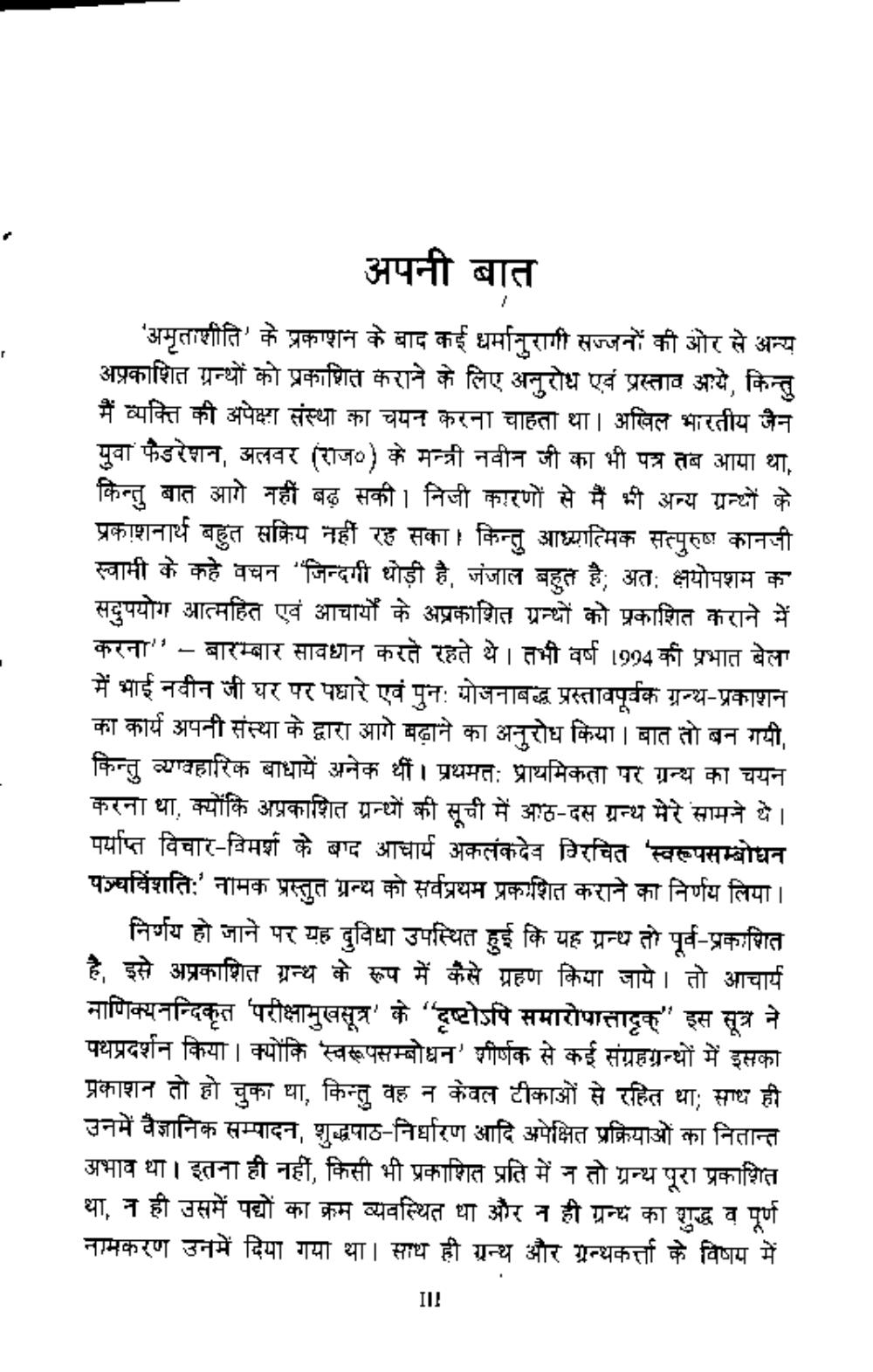________________
अपनी बात 'अमृताशीति' के प्रकाशन के बाद कई धर्मानुरागी सज्जनों की ओर से अन्य अप्रकाशित ग्रन्थों को प्रकाशित कराने के लिए अनुरोध एवं प्रस्ताव आये, किन्तु मैं व्यक्ति की अपेक्षा संस्था का चयन करना चाहता था। अखिल भारतीय जैन युवा फैडरेशन, अलवर (राज.) के मन्त्री नवीन जी का भी पत्र तब आया था, किन्तु बात आगे नहीं बढ़ सकी। निजी कारणों से मैं भी अन्य ग्रन्थों के प्रकाशनार्थ बहुत सक्रिय नहीं रह सका। किन्तु आध्यात्मिक सत्पुरुष्ा कानजी स्वामी के कहे वचन "जिन्दगी थोड़ी है, जंजाल बहुत है; अत: लयोपशम क सदुपयोग आत्महित एवं आचार्यों के अप्रकाशित ग्रन्थों को प्रकाशित कराने में करना'' - बारम्बार सावधान करते रहते थे। तभी वर्ष 1994 की प्रभात बेला में भाई नवीन जी घर पर पधारे एवं पुन: योजनाबद्ध प्रस्तावपूर्वक ग्रन्थ-प्रकाशन का कार्य अपनी संस्था के द्वारा आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। बात तो बन गयी, किन्तु व्यावहारिक बाधायें अनेक थीं। प्रथमतः प्राथमिकता पर ग्रन्थ का चयन करना था, क्योंकि अप्रकाशित ग्रन्थों की सूची में आठ-दस ग्रन्थ मेरे सामने थे। पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद आचार्य अकलंकदेव गिरचित 'स्वरूपसम्बोधन पञ्चविंशति:' नामक प्रस्तुत ग्रन्थ को सर्वप्रथम प्रकाशित कराने का निर्णय लिया।
निर्णय हो जाने पर यह दुविधा उपस्थित हुई कि यह ग्रन्थ तो पूर्व-प्रकाशित है, इसे अप्रकाशित ग्रन्थ के रूप में कैसे ग्रहण किया जाये। तो आचार्य माणिक्यनन्दिकृत परीक्षामुखसूत्र' के “दृष्टोऽपि समारोपासादृक्” इस सूत्र ने पथप्रदर्शन किया। क्योंकि 'स्वरूपसम्बोधन' शीर्षक से कई संग्रहग्रन्थों में इसका प्रकाशन तो हो चुका था, किन्तु वह न केवल टीकाओं से रहित था। साथ ही उनमें वैज्ञानिक सम्पादन, शुद्धपाठ-निर्धारण आदि अपेक्षित प्रक्रियाओं का नितान्त अभाव था। इतना ही नहीं, किसी भी प्रकाशित प्रति में न तो ग्रन्थ पूरा प्रकाशित था, न ही उसमें पद्यों का क्रम व्यवस्थित था और न ही ग्रन्थ का शुद्ध व पूर्ण नामकरण उनमें दिया गया था। साथ ही ग्रन्थ और ग्रन्थकर्ता के विषय में
II!