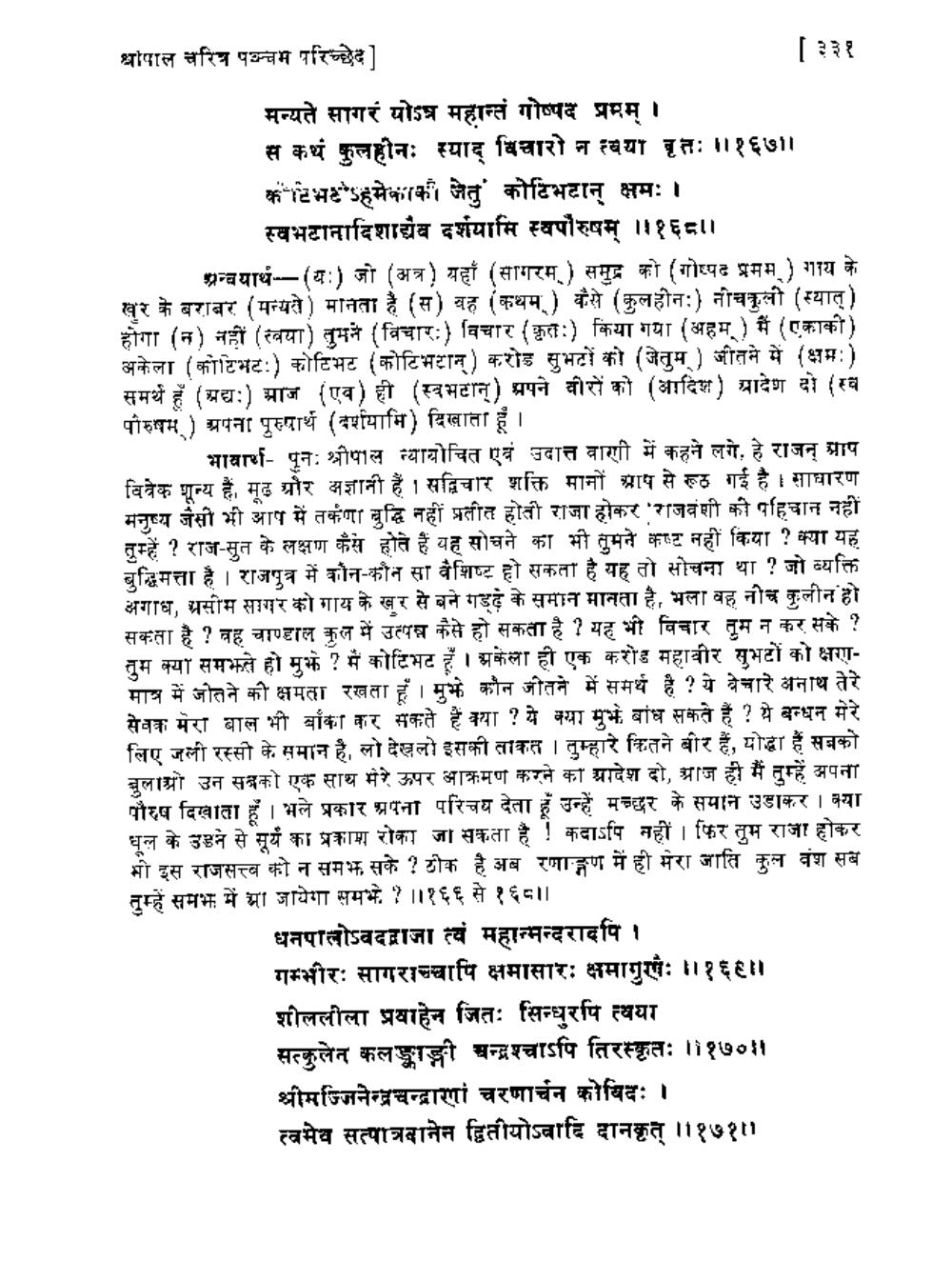________________
श्रीपाल चरित्र पञ्चम परिच्छेद ]
[ ३३१
मन्यते सागरं योऽत्र महान्तं गोष्पद प्रमम् । स कथं कुलहीनः स्याद् विचारो न त्वया वृतः ।।१६७॥ के टिभटेऽहमेकाकी जेतु कोटिभटान् क्षमः ।
स्वभटानादिशाद्यैव दर्शयामि स्वपौरुषम् ॥१६८।।
अन्वयार्थ-- (यः) जो (अत्र) यहाँ (सागरम ) समुद्र को (गोष्पद प्रमम ) गाय के खुर के बराबर (मन्यते) मानता है (स) वह (कथम ) कैसे (कुलहीन;) नीचकूली (स्यात्) होगा (न) नहीं (स्वया) तुमने (विचार:) विचार (कृतः) किया गया (अहम ) मैं (एकाकी) अकेला (कोटिभटः) कोटिभट (कोटिभटान्) करोड सुभटों को (जेतुम ) जीतने में (क्षम:) समर्थ हुँ (अद्यः) आज (एव) ही (स्वभटान्) अपने वीरों को (आदिश) यादेश दो (स्व पौरुषम ) अपना पुरुषार्थ (दर्शयामि) दिखाता हूँ।
भावार्थ- पुनः श्रीपाल न्यायोचित एवं उदात्त वाणी में कहने लगे. हे राजन् पाप विवेक शून्य हैं, मूढ़ और अज्ञानी हैं । सद्विचार शक्ति मानों पाप से रूठ गई है। साधारण मनुष्य जैसी भी आप में तकणा बुद्धि नहीं प्रतीत होती राजा होकर राजवंशी को पहिचान नहीं तुम्हें ? राज-सुत के लक्षण कैसे होते हैं यह सोचने का भी तुमने कष्ट नहीं किया ? क्या यह बुद्धिमत्ता है । राजपुत्र में कौन-कौन सा वैशिष्ट्र हो सकता है यह तो सोचना था ? जो व्यक्ति अगाध, असीम सागर को गाय के खर से बने गडढे के समान मानता है, भला वह नीच कुलीन हो सकता है ? वह चाण्डाल कुल में उत्पन्न कैसे हो सकता है ? यह भी विचार तुम न कर सके ? तुम क्या समझते हो मुझे ? मैं कोटिभट हूँ । अकेला ही एक करोड महावीर सुभटों को क्षणमात्र में जोतने की क्षमता रखता हूँ। मुझे कौन जीतने में समर्थ है ? ये बेचारे अनाथ तेरे सेवक मेरा बाल भी बांका कर सकते हैं क्या ? ये क्या मुझे बांध सकते हैं ? ये बन्धन मेरे लिए जली रस्सी के समान है, लो देख लो इसकी ताकत । तुम्हारे कितने बीर हैं, योद्धा हैं सबको बुलाओ उन सबको एक साथ मेरे ऊपर आक्रमण करने का आदेश दो, आज ही मैं तुम्हें अपना पौरुष दिखाता हूँ। भले प्रकार अपना परिचय देता हूँ उन्हें मच्छर के समान उडाकर । क्या धूल के उडने से सूर्य का प्रकाश रोका जा सकता है ! कदापि नहीं । फिर तुम राजा होकर भी इस राजसत्त्व को न समझ सके ? ठीक है अब रणाङ्गण में ही मेरा जाति कुल वंश सब तुम्हें समझ में भा जायेगा समझे. १ ।।१६६ से १६८।।
धनपालोऽवदद्वाजा त्वं महान्मन्दरादपि । गम्भीरः सागराच्चापि क्षमासारः क्षमागुरपः ।।१६६॥ शीललीला प्रवाहेन जितः सिन्धुरपि त्वया सत्कुलेन कलङ्काङ्गी चन्द्रश्चाऽपि तिरस्कृतः ।। १७०॥ श्रीमज्जिनेन्द्रचन्द्राणां चरणार्चन कोविदः । त्वमेव सत्पात्रदानेन द्वितीयोऽवादि दानकृत् ।।१७१।।