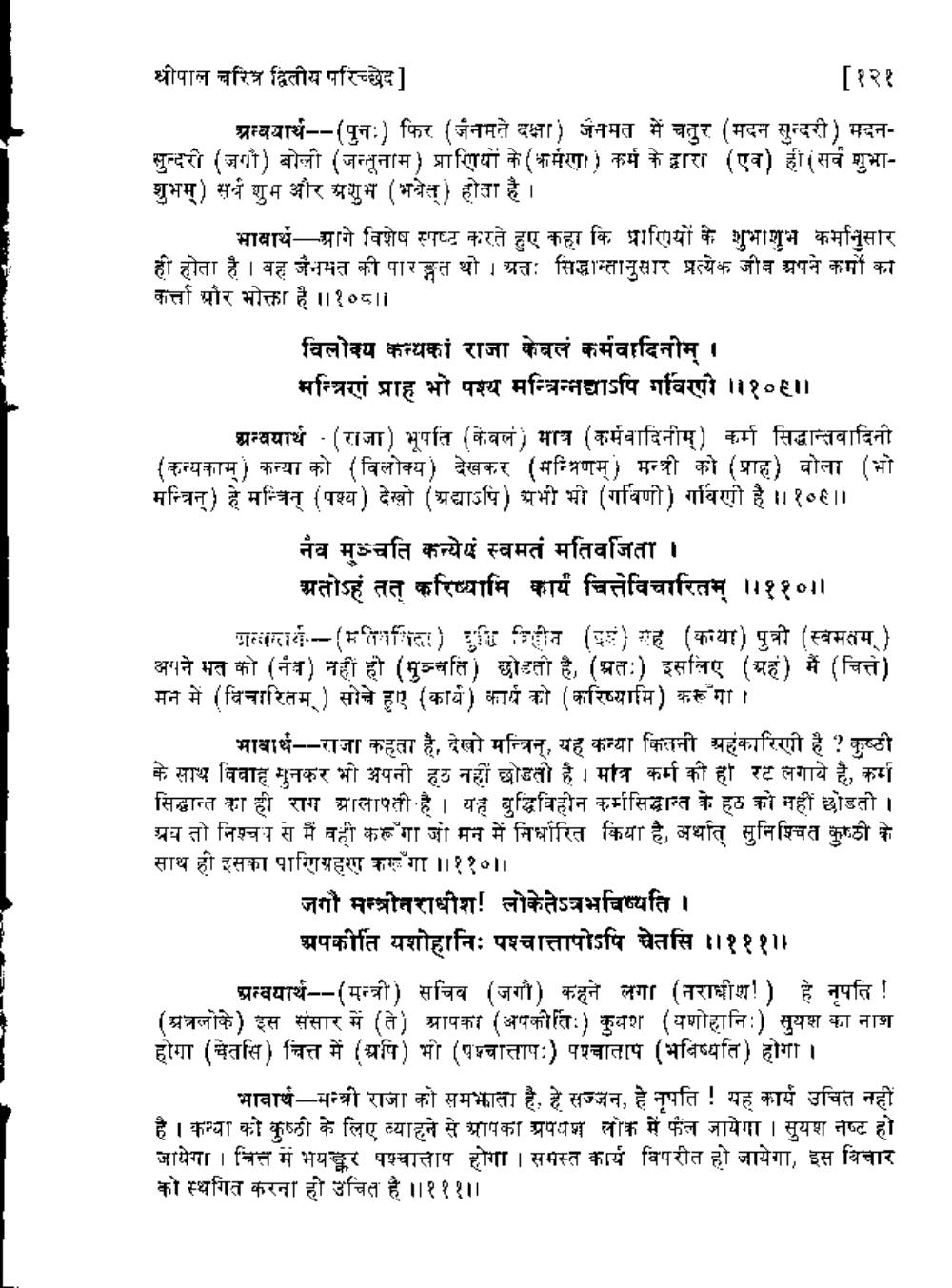________________
श्रीपाल चरित्र द्वितीय परिच्छेद ]
[१२१
श्रन्वयार्थ - - (पुनः) फिर ( जनमते दक्षा) जनमत में चतुर ( मदन सुन्दरी) मदनसुन्दरी (जग) बोली ( जन्तूनाम ) प्राणियों के ( कर्मणा ) कर्म के द्वारा (एव) ही ( सर्व शुभाशुभम् ) सर्व शुभ और अशुभ ( भवेत् ) होता है ।
भावार्थ – आगे विशेष स्पष्ट करते हुए कहा कि प्राणियों के शुभाशुभ कर्मानुसार ही होता है । वह जैनमत की पारङ्गत थी । अतः सिद्धान्तानुसार प्रत्येक जीव अपने कर्मों का कर्त्ता और भोक्ता है ।। १०८ ।।
विलोक्य कन्यका राजा केवलं कर्मवादिनीम् ।
मन्त्रिणं प्राह भो पश्य मन्त्रिन्नद्याऽपि गवरी ॥१०६ ॥
अन्वयार्थ (राजा) भूपति ( केवल ) मात्र ( कर्मवादिनीम् ) कर्म सिद्धान्तवादिनी ( कन्यकाम् ) कन्या को ( विलोक्य) देखकर (मन्त्रिणम् ) मन्त्री को ( प्राह ) बोला ( भो मन्त्रिन्) हे मन्त्रिन् (पश्य) देखो (अद्यापि ) अभी भी (गर्विणी) गर्विपी है ।। १०६ ।।
नैव मुञ्चति कन्येयं स्वमतं मतिवजिता ।
अतोऽहं तत् करिष्यामि कार्यं चित्तविचारितम् ॥ ११०॥
बर्थ -- (विधि) धिविहीन ( ) यह (कन्या) पुत्री (स्वमतम् ) अपने मत को (नेत्र) नहीं हो ( मुञ्चति ) छोडती है, ( श्रतः ) इसलिए (अहं) मैं ( चित्तं ) मन में (विचारितम् ) सोचे हुए ( कार्य ) कार्य को ( करिष्यामि) करूंगा।
भावार्थ -- राजा कहता है, देखो मन्त्रिन्, यह कन्या कितनी अहंकारिणी है ? कुष्ठी के साथ विवाह सुनकर भी अपनी हर नहीं छोडती है। मांत्र कर्म की हा रट लगाये है, कर्म सिद्धान्त का ही राग अलापती है। यह बुद्धिविहीन कर्मसिद्धान्त के हठ को नहीं छोडती । अब तो निश्चय से मैं वहीं करूँगा जो मन में निर्धारित किया है, अर्थात् सुनिश्चित कुष्ठी के साथ ही इसका पाणिग्रहण करूँगा ।। ११० ।
जगौ मन्त्रीतराधीश ! लोकेतेऽत्रभविष्यति ।
अपकीर्ति यशोहानिः पश्चात्तापोऽपि चेतसि ।। १११ ॥
अन्वयार्थ - - (मन्त्री) सचिव ( जगी) कहने लगा ( नराधीश ! )
हे नृपति ! ( अत्रलोके) इस संसार में (ते) आपका ( अपकीर्तिः) कुश ( यशोहानिः ) सुयश का नाश होगा ( चेतसि ) चित्त में (अपि) भी (पश्चात्तापः ) पश्चाताप ( भविष्यति ) होगा ।
भावार्थ - मन्त्री राजा को समझाता है, है सज्जन, हे नृपति ! यह कार्य उचित नहीं है | कन्या को कुष्ठी के लिए व्याहने से आपका अपयश लोक में फैल जायेगा । सुयश नष्ट हो जायेगा । वित्त में भयङ्कर पश्चात्ताप होगा । समस्त कार्य विपरीत हो जायेगा, इस विचार को स्थगित करना ही उचित है ।। १११ ॥