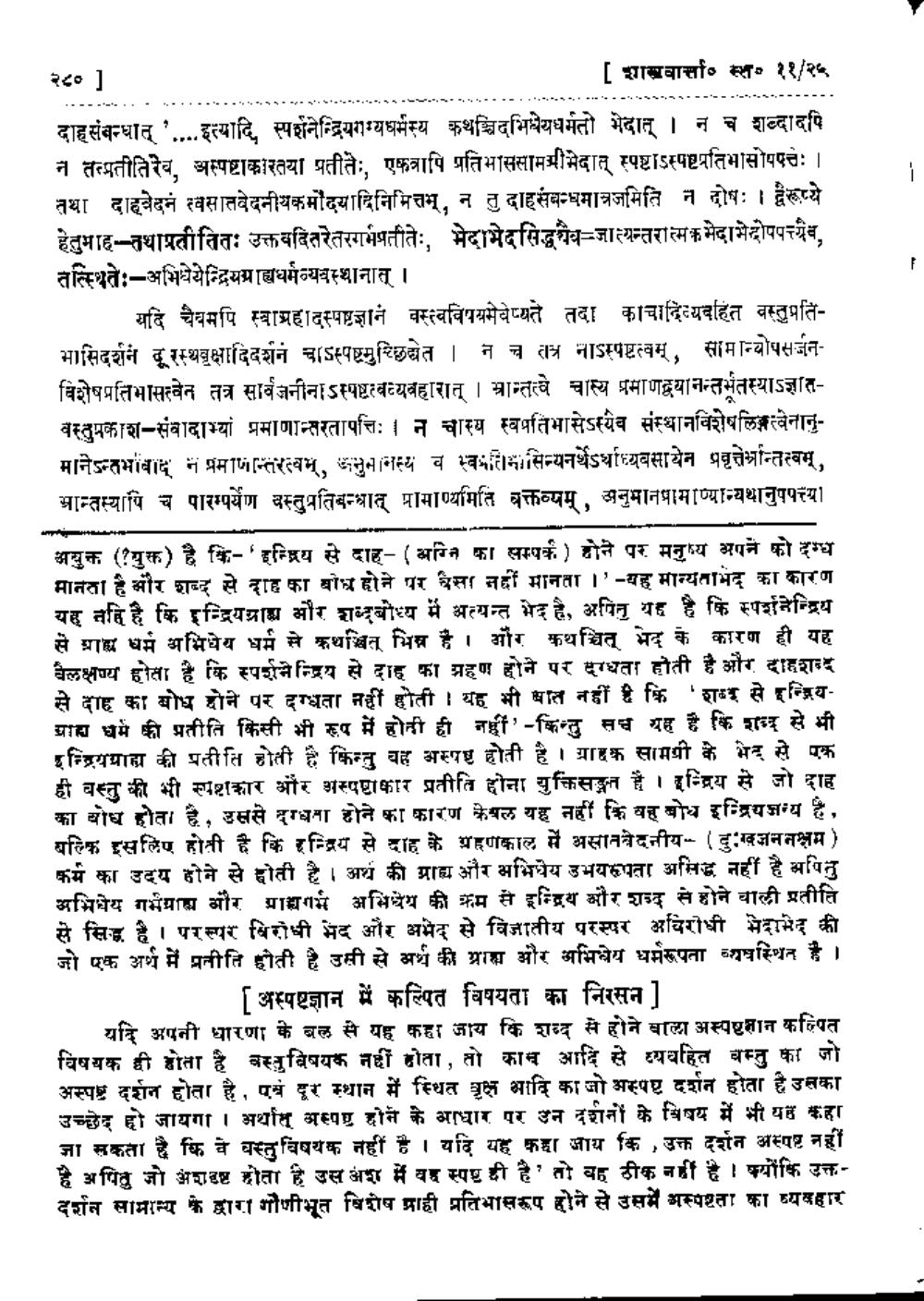________________
२८० ]
[शास्वार्सा० स्तर ११/२५ दाहसंबन्धात् '....इत्यादि, स्पर्शनेन्द्रियगम्यधर्मस्य कथञ्चिदभिधेयधर्मतो भेदात् । न च शब्दादपि न तत्पतीतिरेव, अस्पष्टाकारतया प्रतीतेः, एकत्रापि प्रतिभाससामग्रीभेदात् स्पष्टाऽस्पष्टप्रतिभासोपपत्तेः । तथा दावेदनं वसातवेदनीयकमोदयादिनिमित्तम् , न तु दाहसंबन्धमात्रजमिति न दोषः । द्वैरूप्ये हेतुमाह-तथाप्रतीतितः उक्तवदितरेतरगर्भपतीतेः, भेदाभेदसिद्धथैव-जात्यन्तरात्मक भेदाभेदोपपत्त्यैव, तस्थिते:-अभिधेयेन्द्रियग्राह्यधर्मव्यवस्थानात् ।
यदि चैवमपि स्वाग्रहादस्पष्टज्ञानं वस्त्वविषयमेवेप्यते तदा काचादिव्यदहित वस्तुपतिभासिदर्शन दूरस्थवृक्षादिदर्शनं चाऽस्पष्टमुच्छिद्येत । न च तत्र नाऽस्पष्टत्वम् , सामान्योपसर्जनविशेषप्रतिभासत्वेन तत्र सार्वजनीनाऽस्पष्टत्वव्यवहारात् । श्रान्तत्वे चास्य प्रमाणद्वयानन्त तस्याऽज्ञातवस्तुमकाश-संवादाभ्यां प्रमाणान्तरतापत्तिः । न चास्य स्वप्रतिभासेऽस्येव संस्थानविशेषलिङ्गत्वेनानमानेऽन्तभावा न प्रमाणान्तरत्वम्, अनुमानस्य व स्वातिमासिन्यनर्थेऽर्थाध्यबसायेन प्रवृत्तेन्तिस्वम्, प्रान्तस्यापि च पारम्पर्येण वस्तुप्रतिबन्धात् प्रामाण्यमिति वक्तव्यम् , अनुमानप्रामाण्यान्यथानुपपत्त्या अयुक्त (?युक्त) है कि-' इन्द्रिय से दाह- ( अग्नि का सम्पर्क ) होने पर मनुष्य अपने को दग्ध मानता है और शब्द से दाह का बोध होने पर पैसा नहीं मानता ।' -यह मान्यताभेद का कारण यह नहि है कि इन्द्रियग्राम और शब्दबोध्य में अत्यन्त भेद है, अपितु यह है कि स्पर्शनेन्द्रिय से ग्राह्य धर्म अभिधेय धर्म से कश्चित् भिन्न है। और कथञ्चित् भेद के कारण ही यह बैलक्षण्य होता है कि स्पर्शनेन्द्रिय से दाह का ग्रहण होने पर दग्धता होती है और दाहशब्द से दाह का बोध होने पर दग्धता नहीं होती। यह भी बात नहीं है कि 'शब्द से इन्द्रियग्राह्य धर्म की प्रतीति किसी भी रूप में होती ही नहीं' -किन्तु सच यह है कि शन्द्र से भी इन्द्रियग्राह्य की प्रतीति होती है किन्तु वह अस्पष्ट होती है। ग्राहक सामग्री के भेद से एक ही वस्तु की भी स्पष्टाकार और अस्पष्टाकार प्रतीति होना युक्तिसङ्गत है । इन्द्रिय से जो दाह का बोध होता है, उससे दग्धता होने का कारण केवल यह नहीं कि वह बोध इन्द्रियजन्य है, बल्कि इसलिए होती है कि इन्द्रिय से दाह के ग्रहणकाल में असातवेदनीय- (दुःजननक्षम ) कर्म का उदय होने से होती है। अर्थ की ग्राह्य और अभिधेय उभयरूपता असिद्ध नहीं है अपितु अभिधेय गर्भग्राह्य और ग्राश्चगर्भ अभिधेय की क्रम से इन्द्रिय और शब्द से होने वाली प्रतीति से सिद्ध है । परस्पर विरोधी भेद और अभेद से विजातीय परस्पर अविरोधी भेदाभेद की जो एक अर्थ में प्रतीति होती है उसी से अर्थ की ग्राम और अभिधेय धर्मरूपता व्यवस्थित है।
[अस्पष्टज्ञान में कल्पित विषयता का निरसन] यदि अपनी धारणा के बल से यह कहा जाय कि शब्द से होने वाला अस्पष्टज्ञान कल्पित विषयक ही होता है वस्तुविषयक नहीं होता , तो काम आदि से व्यवहित वस्तु का जो अस्पष्ट दर्शन होता है , पर्व दूर स्थान में स्थित वृक्ष आदि का जो अस्पष्ट दर्शन होता है उसका उच्छेद हो जायगा । अर्थात् अस्पष्ट होने के आधार पर उन दर्शनों के विषय में भी यह कहा जा सकता है कि वे वस्तविषयक नहीं है। यदि यह कहा जाय कि उक्त दर्शन अस्प है अपितु जो अंशदृष्ट होता है उस अंश में वह स्पष्ट ही है तो वह ठीक नहीं है। क्योंकि उक्तदर्शन सामान्य के द्वारा गौणीभूत विशेष प्राही प्रतिभासरूप होने से उसमें अस्पश्ता का ध्यवहार