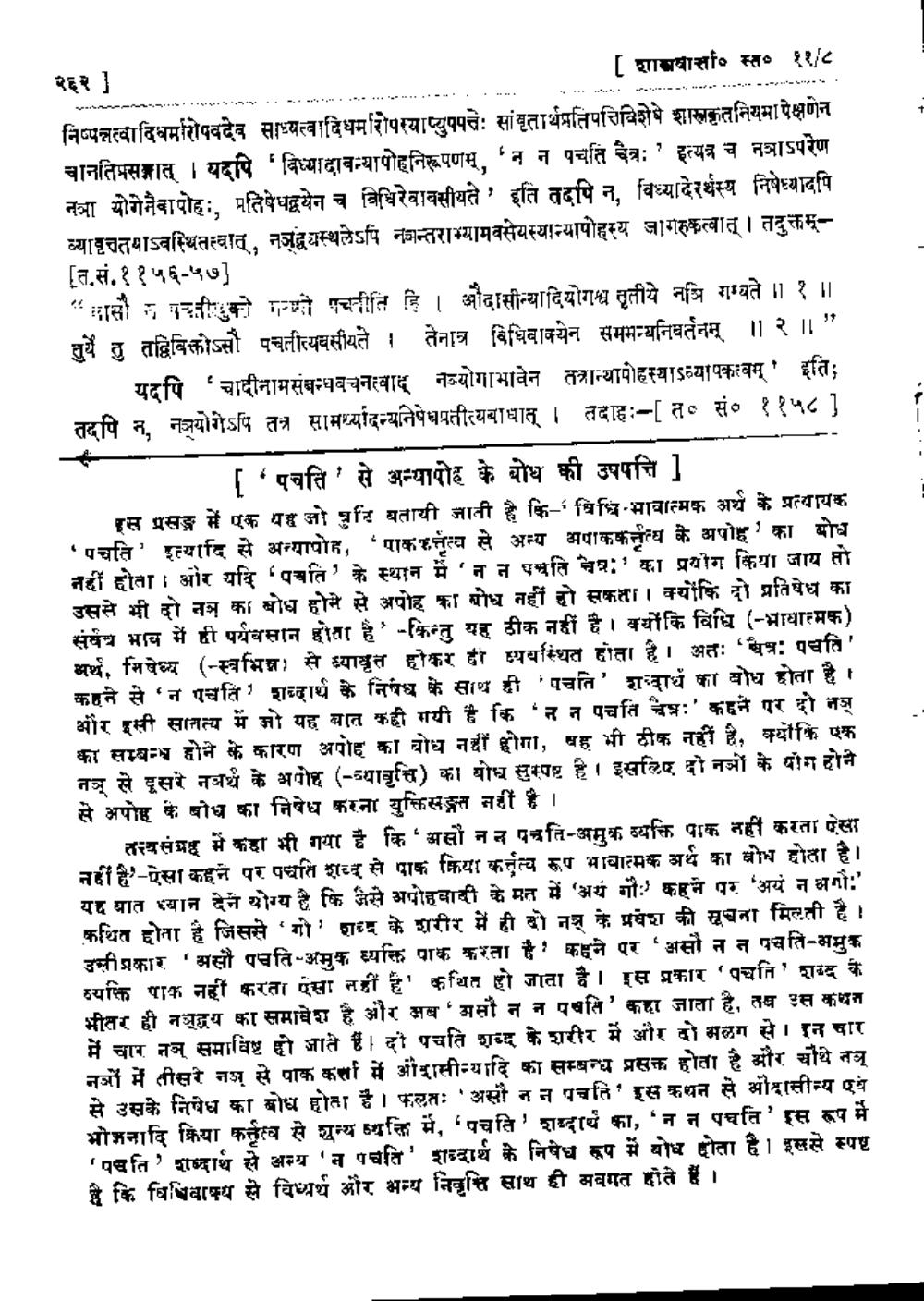________________
[ शासवा० स्त० ११८ निष्पन्नत्वादिधर्मारोपवदेव साध्यत्वादिधर्मारोपस्याप्युपपत्तेः सांवृतार्थप्रतिपत्तिविशेधे शास्त्रकृतनियमा पेक्षणेन चानतिप्रसङ्गात् । यदपि 'विध्यादावन्यापोहनिरूपणम्, 'न न पचति चैत्रः' इत्यत्र च नाऽपरेण नत्रा योगेनैकापोहः, प्रतिषेधद्वयेन च विधिरेवावसीयते' इति तदपि न, विध्यादेरर्थस्य निषेध्यादपि व्यावृत्ततयाऽवस्थितत्वात् , नद्वयस्थलेऽपि नअन्तराभ्यामवसेयस्यान्यापोहस्य जागरुकत्वात् । तदुक्तम्[त.सं.११५६-५७] " मासौ , मशीको नमो पचतीति हि । औदासीन्यादियोगश्च तृतीये नञि गम्यते ॥ १ ॥ तुर्थे तु तद्विविक्तोऽसौ पचतीत्यवीयते । तेनात्र विधिवाक्येन सममन्यनिवर्तनम् ॥२॥"
यदपि 'चादीनामसंबन्धवचनत्वाद् नब्योगाभावेन तत्रान्यापोहस्याऽव्यापकत्वम् ' इति; तदपि न, नयोगेऽपि तत्र सामर्थ्यादन्यनिषेधपतीत्यबाधात् । तदाहः-[ त० सं० ११५८ ]
[ 'पचति' से अन्यापोह के बोध की उपपत्ति ] इस प्रसङ्ग में एक यह जो दि बतायी जाती है कि-'विधि भावात्मक अर्थ के प्रत्यायक 'पति' इत्यादि से अन्यापोह, 'पाककर्तृत्व से अन्य अपाककर्नत्य के अपोह' का बोध नहीं होता। और यदि 'पति' के स्थान में न न पचति चन:' का प्रयोग किया जाय तो उससे भी दो नत्र का बोध होने से अपोह का बोध नहीं हो सकता। क्योंकि दो प्रतिषेध का संबंध भाव में ही पर्यवसान होता है किन्त यत ठीक नहीं है। क्योंकि विधि (-भायात्मक) अर्थ, मिषेय (-स्वभिन्न से ध्यावत होकर ही ध्ययस्थित होता है। अतः
मत: : पति ' कहने से 'न पचति' शब्दार्थ के निषेध के साथ ही 'पचति' शदा) का बोध होता है। और इसी सातत्य में जो यह बात कही गयी है कि 'न न पचति चत्रः' कहने पर दो नञ् का सम्बन्ध होने के कारण अपोह का बोध नहीं होगा, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक नञ् से दूसरे नार्थ के अपोह (-व्यावृत्ति) का बोध सुस्पष्ट है। इसलिए दो नत्रों के योग होने से अपोह के बोध का निषेध करना युक्तिसङ्गत नहीं है।
तत्यसंग्रह में कहा भी गया है कि 'असौ न न पचति-अमुक व्यक्ति पाक नहीं करता ऐसा नहीं है-ऐसा कहने पर पति शब्द से पाक क्रिया कर्तुत्य रूप भावात्मक अर्थ का बोध होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जैसे अपोहवादी के मत में 'अयं गौः' कहने पर 'अयं न अगो:' कथित होता है जिससे 'गो' शब्द के शरीर में ही दो नत्र के प्रवेश की सूचना मिलती है। उनी असौ पचति-अमक ध्यक्ति पाक करता है. कहने पर 'असौ न न पचति-अमक व्यक्ति पाक नहीं करता एसा नहीं है' कथित हो जाता है। इस प्रकार 'पति' शब्द के भीतर ही नद्धय का समावेश है और अब 'असौ न न पति' कहा जाता है, तब इस कथन में चार नञ् समाविष्ट हो जाते हैं। दो पचति शब्द के शरीर में और दो अलग से। इन चार नों में तीसरे न से पाक का में औसीन्यादि का सम्बन्ध प्रसक्त होता है और चौथे नञ् से उसके निषेध का बोध होता है। फलतः ' असौ न न पचति' इस कथन से औदासीन्य एवं भोजनादि क्रिया कर्तृत्व से शुन्य व्यक्ति में, 'पचति' शब्दार्थ का, 'न न पचति' इस रूप में 'पति' शब्दार्थ से अन्य न पचति' शब्दार्थ के निषेध रूप में बोध होता है। इससे स्पष्ट है कि विधिवाक्य से विध्यर्थ और अन्य निवृत्ति साथ ही अवगत होते है।
-