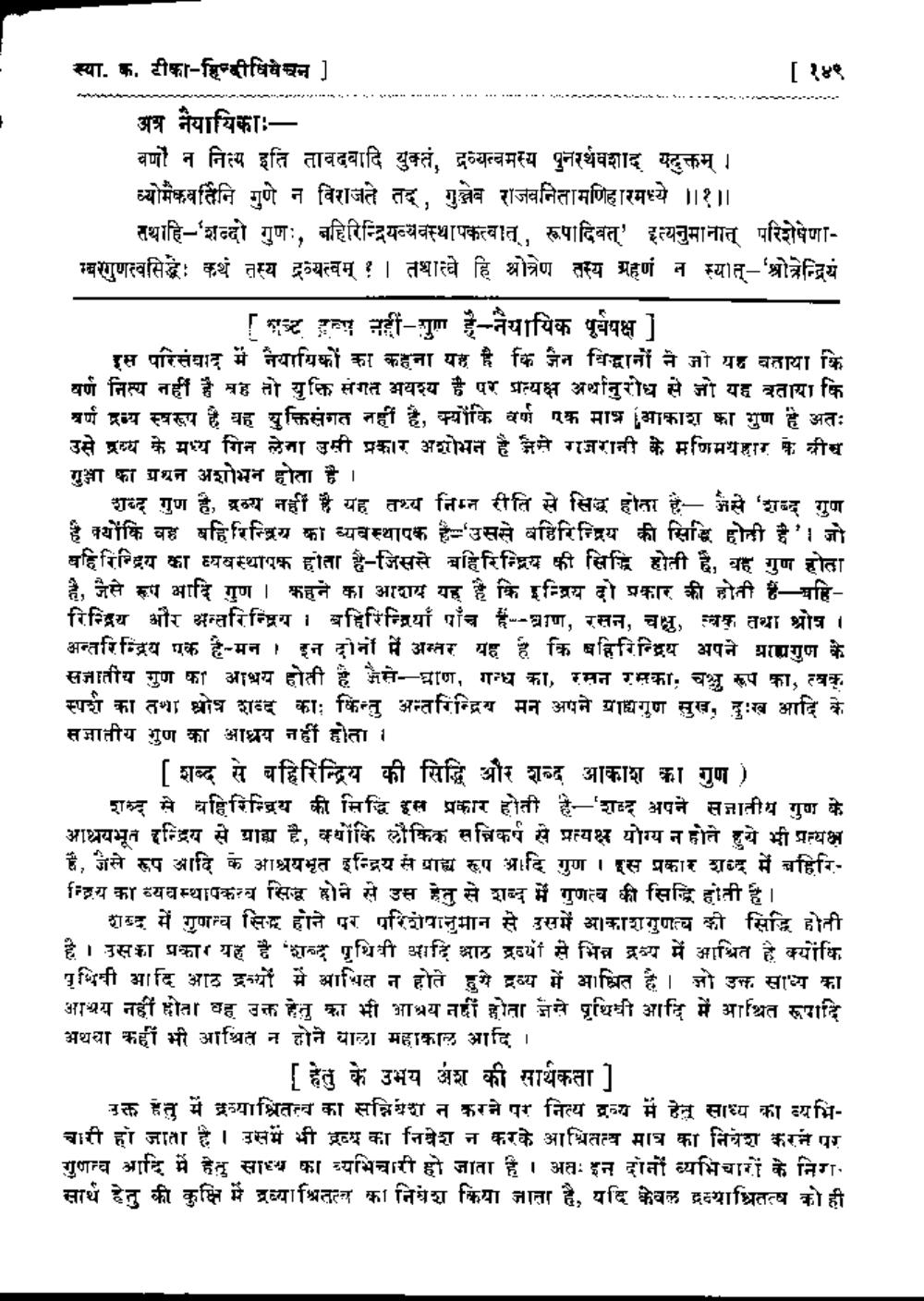________________
स्या. क. टीका-हिन्दीविवेचन ]
[ १४९ अत्र नैयायिकाःवो न नित्य इति ताबदबादि युक्तं, द्रव्यन्वमस्य पुनरर्थवशाद यदुक्तम् । व्योमैकवर्तिनि गुणे न विराजते तद् , गुल्लेब राजवनितामणिहारमध्ये ॥१॥
सथाहि-शब्दो गुणः, बहिरिन्द्रियव्यवस्थापकत्वात् , रूपादिवत्' इत्यनुमानात् परिशेषेणाम्वगुणस्वसिद्धः कथं तस्य द्रव्यत्वम् ? । तथात्वे हि श्रोत्रेण तस्य ग्रहणं न स्यात्- 'श्रोत्रेन्द्रिय
हप नहीं-गुण है-नैयायिक पूर्वपक्ष ] इस परिसंघाद में नैयायिकों का कहना यह है कि जैन विद्वानों ने जो यह बताया कि वर्ण निस्य नहीं है मह तो युक्ति संगत अवश्य है पर प्रत्यक्ष अर्थानुरोध से जो यह बताया कि वर्ण द्रव्य स्वरूप है यह युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि वर्ण एक मात्र आकाश का गुण है अतः उसे द्रव्य के मध्य गिन लेना उसी प्रकार अशोभन है जैसे गजरानी के मणिमयहार के बीच गुञ्जा का प्रथन अशोभन होता है।
शब्द गुण है, द्रव्य नहीं है यह तथ्य निम्न रीति से सिद्ध होता है:- जैसे 'शब्द गुण है क्योंकि वह बहिरिन्द्रिय का व्यवस्थापक है-'उससे बहिरिन्द्रिय की सिद्धि होती है। जो बहिरिन्द्रिय का व्यवस्थापक होता है-जिससे बहिरिन्द्रिय की सिद्धि होती है, यह गुण होता है, जैसे रूप आदि गुण | कहने का आशय यह है कि इन्द्रिय दो प्रकार की होती है यहिरिन्द्रिय और अन्तरिन्घ्यि । बहिरिन्द्रियाँ पाँच है. प्राण, रसन, चक्षु, स्वक तथा श्रोत्र । अन्तरिन्द्रिय एक है-मन । इन दोनों में अन्तर यह है कि बहिगिन्द्रिय अपने प्राणगुण के सजातीय गुण का आश्रय होती है जैसे-घाण, गन्ध का, रमन रमका, चक्षु रूप का, त्वक स्पर्श का तथा श्रोत्र शब्द काः किन्तु अन्तगिन्द्रिय मन अपने प्राधगुण सुख, दुःख आदि के सजातीय गुण का आश्रय नहीं होता ।।
[ शब्द से बहिरिन्द्रिय की सिद्धि और शब्द आकाश का गुण ) शब्द से बहिरिन्द्रिय की सिद्धि इस प्रकार होती है-'शब्द अपने सजातीय गुण के आश्रयभूत इन्द्रिय से ग्राम है, क्योंकि लौकिक सत्रिकर्ष से प्रत्यक्ष योग्य न होते हुये भी प्रत्यक्ष है, जिसे रूप आदि के आश्रयभूत इन्द्रिय संग्राह्य रूप आदि गुण । इस प्रकार शब्द में बहिरिन्द्रिय का व्यवस्थापकत्व सिद्ध होने से उस हेतु से शब्द में गुणत्व की सिद्धि होती है।
शब्द में गुणव सिन्द होने पर परिशेपानुमान से उसमें आकाशगुणात्य की सिद्धि होती है। उसका प्रकार यह है “शब्द पृथिवी आदि आठ द्रव्यों से भिन्न द्रव्य में आश्रित है क्योंकि पृथिवी आदि आठ द्रव्यों में आश्रित न होते हुये द्रव्य में आश्रित है। जो उस साध्य का आश्य नहीं होता वह उक्त हेतु का भी आश्रय नहीं होता जो पृथिवी आदि में आश्रित रूगदि अथवा कहीं भी आश्रित न होने वाला महाकाल आदि ।
हेतु के उभय अंश की सार्थकता ] उक्त हेतु में द्रव्याश्रितत्व का सन्निवेश न करने पर नित्य द्रव्य में हेतु साध्य का व्यभिचारी हो जाता है । इसमें भी द्रव्य का निवेश न करके आश्रितत्व मात्र का निवेश करने पर गुणव आदि में हेतु साध्य का व्यभिचारी हो जाता है । अतः इन दोनों व्यभिचारों के निग. सार्थ हेतु की कुक्षि में व्याश्रितत्व का निधेश किया जाता है, यदि केवल द्रक्ष्याभ्रितत्व को ही