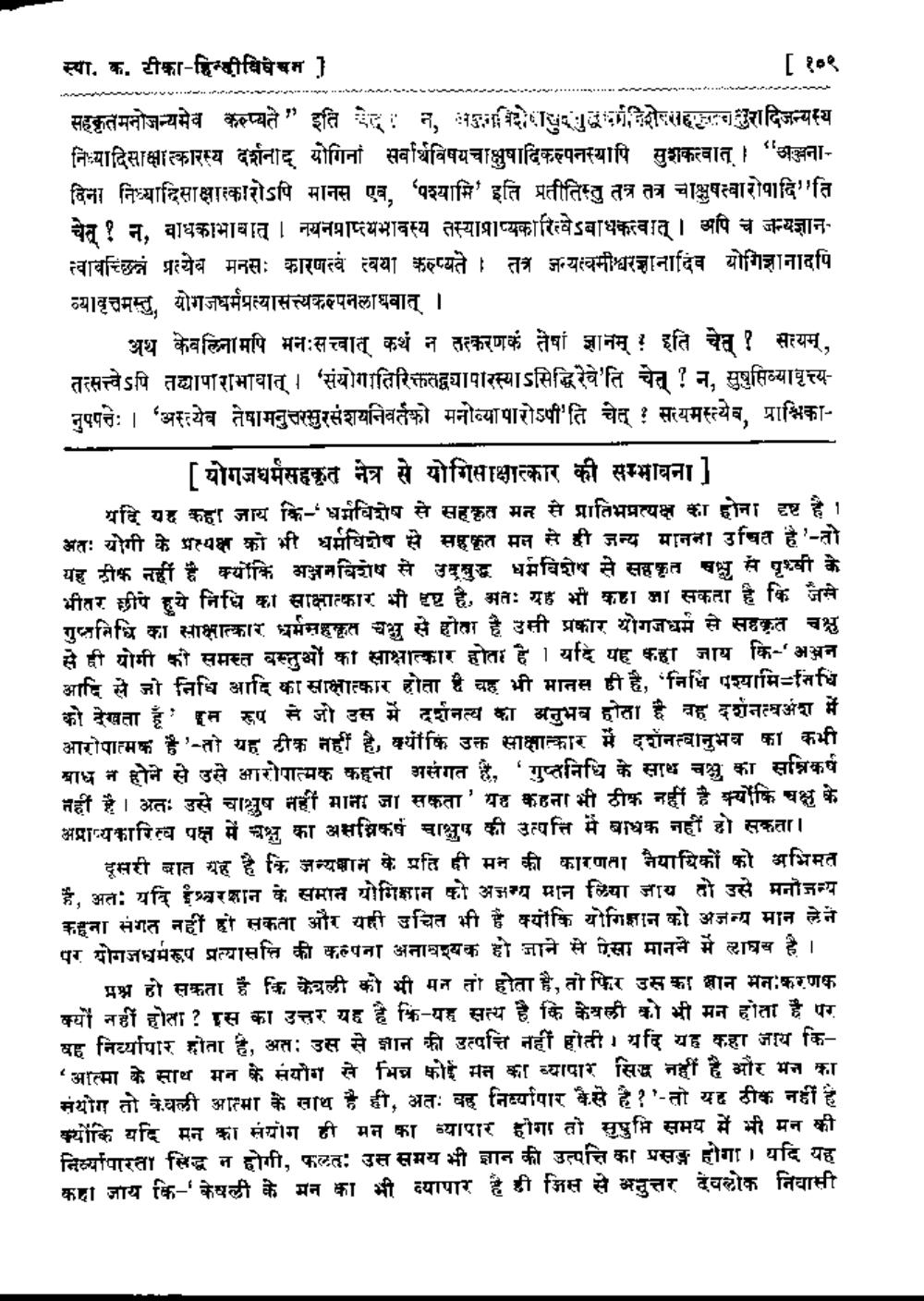________________
स्था. क. टीका-हिन्दीविषेचन ]
[ १०९
सहकृतमनोजन्यमेव करप्यते" इति वेद :: न, विदोषासुर मनिस्सहारा दिजन्यस्य निम्यादिसाक्षात्कारस्य दर्शनाद् योगिनां सर्वार्थविषयचाक्षुषादिकल्पनस्यापि सुशकत्वात् । “अञ्जनाविना निध्यादिसाक्षात्कारोऽपि मानस एव, 'पश्यामि' इति प्रतीतिस्तु तत्र तत्र चाक्षुषत्वारोपादि"ति चेत् ? न, बाधकाभावात् । नयनप्राप्त्यभावस्य तस्याप्राप्यकारित्वेऽबाधकत्वात् । अपि च जन्यज्ञानत्वावच्छिन्नं प्रत्येक मनसः कारणत्वं त्वया करप्यते । तत्र जन्यस्वमीश्वरज्ञानादिव योगिज्ञानादपि व्यावृत्तमस्तु, योगजधर्मप्रत्यासत्यकल्पनलाघवात् ।
अथ केबलिनामपि मनःसत्त्वात् कथं न तत्करणकं तेषां ज्ञानम् ! इति चेत् ? सत्यम् , तत्सत्त्वेऽपि तयापाराभावात् । 'संयोगातिरिक्ततद्वयापारस्याऽसिद्धि रेवेति चेत् ? न, सुषुप्तिव्यावृत्त्यनुपपत्तेः । 'अस्त्येव तेषामनुत्तरसुरसंशयनिवर्तको मनोव्यापारोऽपीति चेत् ? सत्यमस्त्येव, प्राभिका
[योगजधर्मसहकृत नेत्र से योगिसाक्षात्कार की सम्भावना] यदि यह कहा जाय कि-'धर्मविशेष से सहकृत मन से प्रातिभप्रत्यक्ष का होना दृष्ट है। अतः योगी के प्रत्यक्ष को भी धर्मविशेष से सहकत मन से ही जन्य मानना उचित है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि अञ्जमविशेष से उबुद्ध धर्मविशेष से सहकृत पक्ष से पृथ्वी के भीतर ये निधि का साक्षात्कार भी दृष्ट है, अतः यह भी कहा ना सकता है कि जैसे गुणनिधि का साक्षात्कार धर्ममहकत चच से होता है उसी प्रकार योगजधर्म से सहकृत चन से ही योगी की समस्त वस्तुओं का साक्षात्कार होता है । यदि यह कहा जाय कि-'अञ्जन आदि से जो निधि आदि का साक्षात्कार होता है वह भी मानस ही है, 'निधि पश्यामि निधि को देखता हूँ इस रूप से जो उस में दर्शनत्य का अनुभव होता है वह दर्शनत्वअंश में आरोपात्मक है'-तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त साक्षात्कार में दर्शनत्वानुभव का कभी बाध न होने से उसे आरोगत्मक कहना असंगत है, 'गुप्तनिधि के साथ चनु का सन्निकर्ष नहीं है। अतः उसे चाक्षुष नहीं माना जा सकता' यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि चक्ष के अप्राप्यकारिस्व पक्ष में चक्षु का असन्निकर्ष चाक्षुष की उत्पत्ति में बाधक नहीं हो सकता।
__ दूसरी बात यह है कि जन्यज्ञान के प्रति ही मन की कारणता नैयायिकों को अभिमत हैं, अत: यदि ईश्वर ज्ञान के समान योगिझान को अजय मान लिया जाय तो उसे मनोजन्य कहना संगत नहीं हो सकता और यही उचित भी है क्योंकि योगिज्ञान को अजन्य मान लेने पर योगजधर्मरूप प्रत्यासत्ति की कल्पना अनावश्यक हो जाने से ऐसा मानने में साघय है।
प्रश्न हो सकता है कि केवली को भी मन तो होता है, तो फिर उस का शान मनःकरणक क्यों नहीं होता?स का उत्तर यह है कि-यह सत्य है कि कैवल्ली को भी मन होता है पर यह निर्व्यापार होता है, अत: उस से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। यदि यह कहा जाय कि'आत्मा के साथ मन के संयोग से भिन्न कोई मन का व्यापार सिम्स नहीं है और मन का मयोग तो केवली आत्मा के साथ है ही, अतः वह निर्यापार कैसे है ?'-तो यह ठीक नहीं है क्योंकि यदि मन का संयोग ही मन का व्यापार होगा तो सुषुप्ति समय में भी मन की नियापारता सिद्ध न होगी, फलतः उस समय भी ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसङ्ग होगा। यदि यह कहा जाय कि-'केवली के मन का भी व्यापार है ही जिस से अनुत्तर देवलोक निवासी