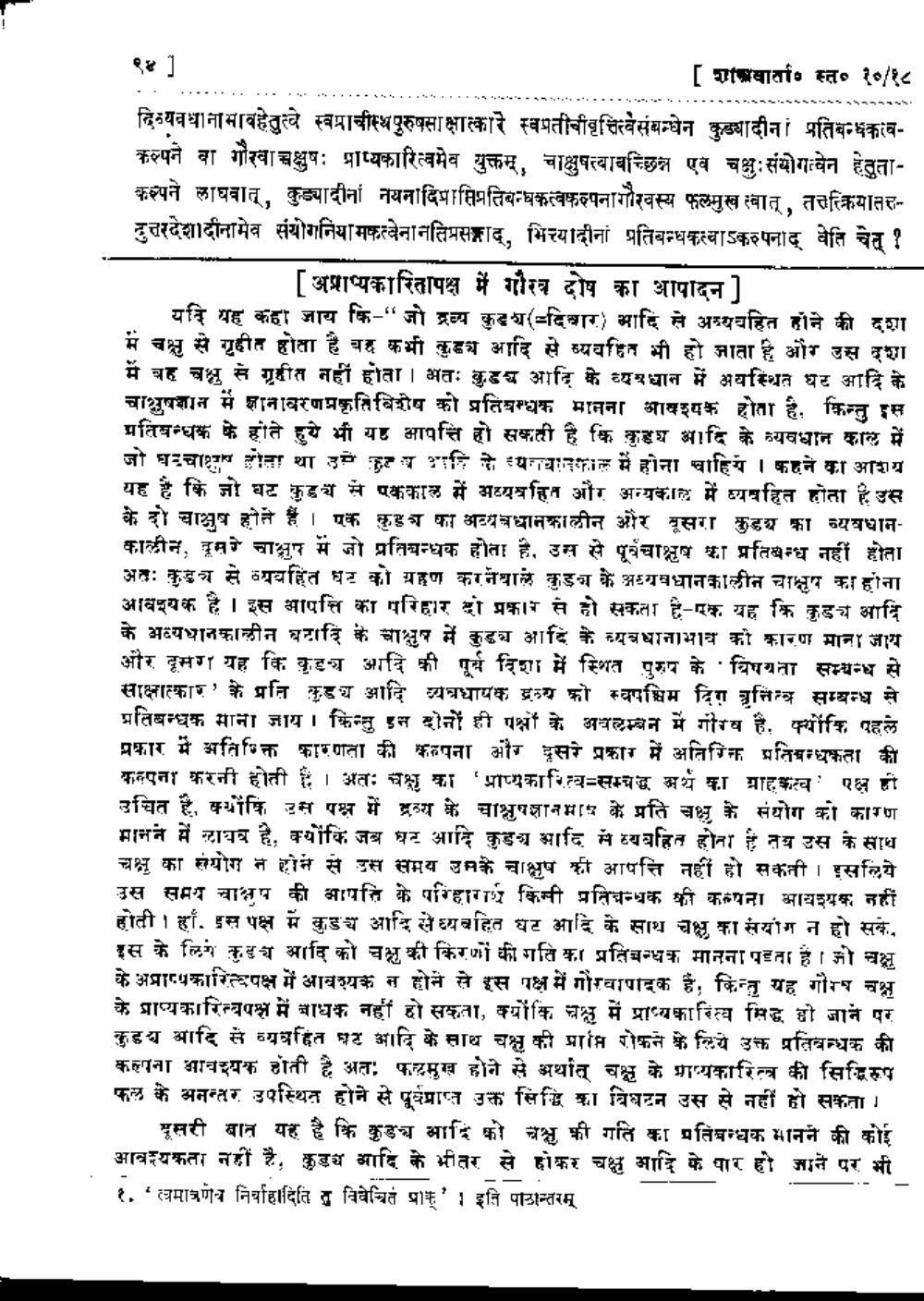________________
९४ ]
[ शासवार्ताः स्त० १०/१८ दिव्यवधानामावहेतुत्वे स्वप्राचीस्थपुरुषसाक्षात्कारे स्वपतीचीवृत्तित्वेसंबन्धेन कुड्यादीनां प्रतिबन्धकत्वकल्पने वा गौरवाचक्षुषः प्राप्यकारित्वमेव युक्तम्, चाक्षुषत्वावच्छिन्न एव चक्षुः संयोगत्वेन हेतुताकल्पने लाघवात् , कुड्यादीनां नयनादिप्राप्तिप्रतिबन्धकत्वकल्पनागौरवस्य फलमुख स्वात् , ततक्रियातत्तदुत्तरदेशादीनामेव संयोगनियामकत्वेनानतिप्रसकाद्, भित्यादीनां प्रतिबन्धकत्वाऽकरुपनाद् वेति चेत् ?
[अप्राप्यकारितापक्ष में गौरव दोष का आपादन] यदि यह कहा जाय कि-"जो द्रव्य कुदय(-दिशार भादि से अश्यरहित होने की दशा में चक्ष से गृहीत होता है वह कभी कुड्ध आदि से व्यवहित भी हो जाता है और उस दशा में वह चश्न गृहीत नहीं होता। अतः कुडच आदि के व्यवधान में अयस्थित घट आदि के चाशुषशान में ज्ञानावरणप्रकृतिविशेष को प्रतिबन्धक मानना आवश्यक होता है. किन्तु इस प्रतिबन्धक के होते हुये भी यह आपत्ति हो सकती है कि कुड्य आदि के व्यवधान काल में जो घरचाना होता था उमेद आदि से व्यायामाल में होना चाहिये । कहने का आशय यह है कि जो घट कुद्धच से पककाल में अध्यहित और अन्यकाल में व्यवहित होता है उस के दो चाक्षुष होते हैं। एक कुत्र का अव्यवधानकालीन और दूसग कुडय का व्यवधानकालीन, दुमरे चाक्षुप में जो प्रतिबन्धक होता है, उस से पूर्वचाक्षुष का प्रतिबन्ध नहीं होता अत: कुद्ध से व्यवहित घट को ग्रहण करनेवाले कुड़न के अध्यवधानकालीन चाक्षुष काहींना आवश्यक है । इस आपत्ति का परिहार दो प्रकार से हो सकता है-एक यह कि कृडय आदि के अव्यधानकालीन घटादि के चाक्षुष में कुडय आदि के व्यत्र धानाभाव को कारण माना जाय और दृमग यह कि कृढ-य आदि की पूर्व दिशा में स्थित पुरुष के विषयता सम्बन्ध से साक्षात्कार' के प्रति कुडय आदि व्यवधायक द्रव्य को स्वपश्चिम दिग वृत्तित्र सम्बन्ध मे प्रतिबन्धक माना जाय । किन्तु इन दोनों ही पक्षों के अवलम्बन में गौग्य है. क्योंकि पहले प्रकार में अतिरिक्त कारणता की कल्पना और दूसरे प्रकार में अतिरिक्त प्रतिबन्धकता की कल्पना करनी होती है। अतः चक्ष का 'प्राप्यकात्वि-सम्बद्ध अर्थ का ग्राहकत्व' एक्ष ही उचित है, क्योंकि उस पक्ष में द्रव्य के चाक्षुष ज्ञानमा के प्रति चक्षु के संयोग को कारण मानने में टायर है, क्योंकि जब घट आदि कुडय आदि में व्यवहित होता है तब उस के साथ चक्षु का संयोग न होने से उस समय उसके चानुष की आपत्ति नहीं हो सकती । इसलिये उस समय चाक्षप की आपत्ति के परिहागर्थ किमी प्रतिबन्धक की कल्पना आवश्यक नहीं होती। हाँ. इस पक्ष में कुडच आदि से ध्यवहित घट आदि के साथ चक्षु का संयोग न हो सके, इस के लिय कच आदि को चाकी किरणों की गति का प्रतिबन्धक मानना पडता है। मो चल के अप्राप्यकारिवपक्ष में आवश्यक न होने से इस पक्ष में गौरवाणादक हैं, किन्तु यह गौरव चश्न के प्राप्यकारिवपक्ष में बाधक नहीं हो सकता, क्योंकि चश्च में प्राध्यकारित्व सिद्ध हो जाने पर कुडव आदि से व्यवहित घट आदि के साथ चश्च की प्राप्ति रोकने के लिये उक्त प्रतिबन्धक की कल्पना आवश्यक होती है अतः फलमग्न होने से अर्थात् चश्च के प्राप्यकारित्र की सिद्धि रूप फल के अनन्तर उपस्थित होने से पूर्वप्राप्त उक्त सिद्धि का विघटन उस से नहीं हो सकता ! _दूसरी बात यह है कि कुडच आदि को चश्च की गति का प्रतिबन्धक मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुलथ आदि के भीतर से होकर चक्षु आदि के पार हो जाने पर भी १. 'स्वमात्रणेव निर्वाहादिति तु विवेचितं प्राक्' । इति पाठान्तरम्