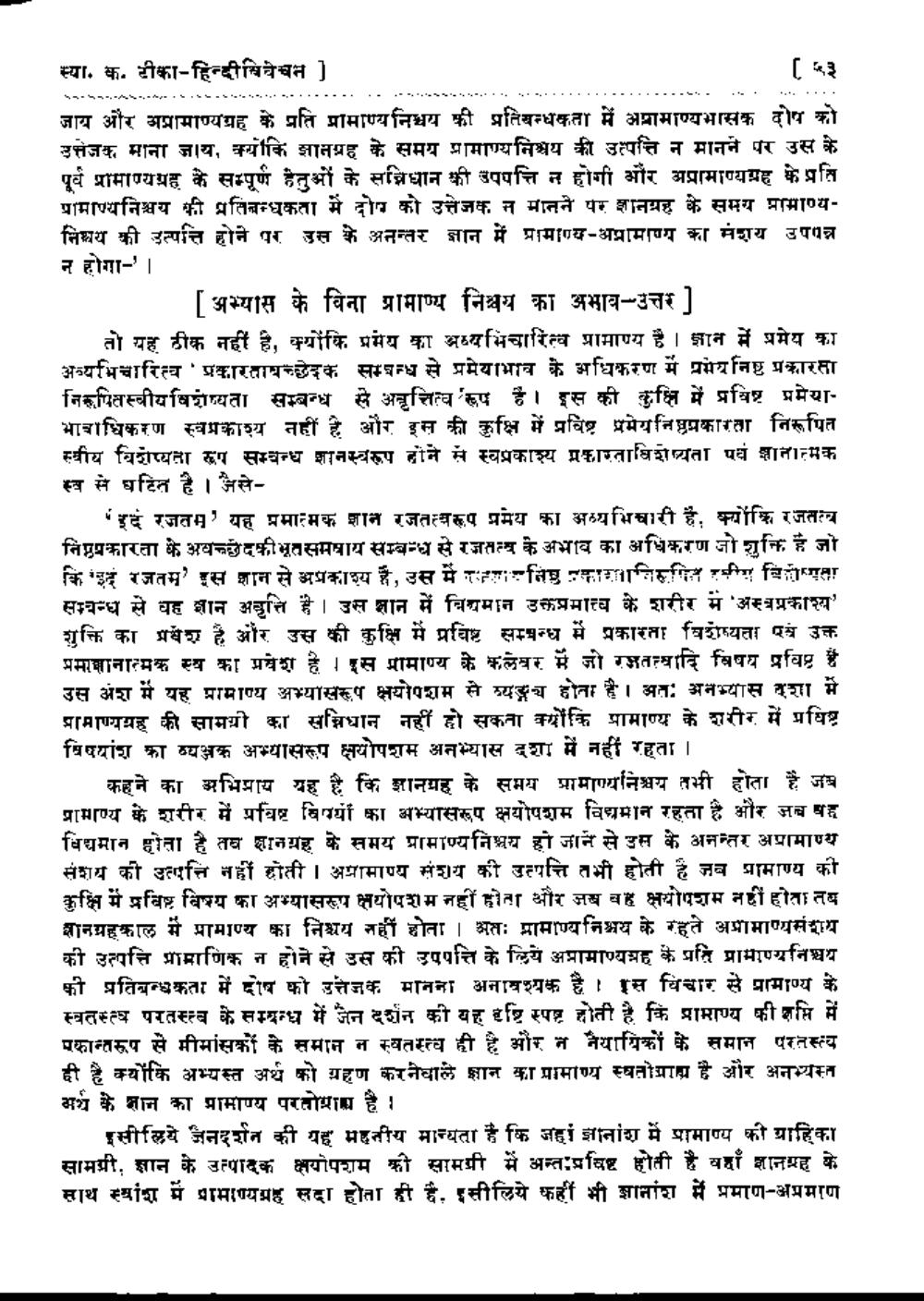________________
स्या. क. टीका-हिन्दी विवेचन ]
[ ५३
जाय और अप्रामाण्यग्रह के प्रति प्रामाण्यनिश्चय की प्रतिबन्धकता में अप्रामाण्यभासक दोष को उत्तेजक माना जाय, क्योंकि ज्ञानग्रह के समय प्रामाण्यनिश्चय की उत्पत्ति न मानने पर उस के पूर्व प्रामाण्यग्रह के सम्पूर्ण हेतुओं के सन्निधान की उपपत्ति न होगी और अप्रामाण्यग्रह के प्रति प्रामाण्यनिश्चय की प्रतिबन्धकता में दोष को उत्तेजक न मानने पर ज्ञानग्रह के समय प्रामाण्यनिश्रय की उत्पत्ति होने पर उस के अनन्तर ज्ञान में प्रामाण्य- अप्रामाण्य का मंशय उपपन्न न होगा |
[ अभ्यास के विना ग्रामाण्य निश्चय का अभाव - उत्तर ]
तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमेय का अध्यभिचारित्व प्रामाण्य है। ज्ञान में प्रमेय का अव्यभिचारित्व प्रकारतायच्छेदक सम्बन्ध से प्रमेयाभाव के अधिकरण में प्रमेयनिष्ठ प्रकारता निरूपित स्वीय विशेष्यता सम्बन्ध से अवृत्तित्व रूप है। इस की कुक्षि में प्रविष्ट प्रमेयाभावाधिकरण स्वप्रकाश्य नहीं है और इस की कुक्षि में प्रविष्ट प्रमेयनिष्ठप्रकारता निरूपित स्त्रीय विशेष्यता रूप सम्बन्ध ज्ञानस्वरूप होने से स्वप्रकाश्य प्रकारताविशेष्यता पवं ज्ञानात्मक स्त्र से घटित है । जैसे
" इदं रजतम' यह प्रमात्मक शान रजतत्वरूप प्रमेय का अभ्यभिचारी है, क्योंकि रजतत्व निप्रकारता के अवच्छेद की भूतसमप्राय सम्बन्ध से रजसत्य के अभाव का अधिकरण जो शुति है जो किं इदं रजतम' इस ज्ञान से अप्रकाश्य है, उसमें पिता सम्बन्ध से वह ज्ञान अवृत्ति है । उस ज्ञान में विश्रमान उक्तप्रमात्व के शरीर में 'अस्त्रप्रकाश्य' शुक्ति का प्रवेश है और उस की कुक्षि में प्रविष्ट सम्बन्ध में प्रकारता विशेष्यता पत्र उक्त प्रमशानात्मक स्व का प्रवेश है। इस प्रामाण्य के कलेवर जो रजतत्वादि विषय प्रविष्ट हैं उस अंश में यह प्रामाण्य अभ्यासरूप क्षयोपशम से व्यय होता है । अतः अनभ्यास दशा में प्रामाण्यग्रह की सामग्री का सन्निधान नहीं हो सकता क्योंकि प्रामाण्य के शरीर में प्रविष्ट fueria का व्यञ्जक अभ्यासरूप क्षयोपशम अनभ्यास दशा में नहीं रहता ।
कहने का अभिप्राय यह है कि ज्ञानग्रह के समय प्रामाण्यनिश्चय तभी होता है जब प्रामाण्य के शरीर में प्रविष्ट विषयों का अभ्यासरूप क्षयोपशम विद्यमान रहता है और जब वह विद्यमान होता है तब ज्ञानग्रह के समय प्रामाण्यनिश्रय हो जाने से उस के अनन्तर अप्रामाण्य संशय की उत्पत्ति नहीं होती । अप्रामाण्य संशय की उत्पत्ति तभी होती हैं जब प्रामाण्य की कुक्षि में प्रविष्ट विषय का अभ्यासरूप क्षयोपशम नहीं होता और जब वह क्षयोपशम नहीं होता तब ज्ञानग्रहकाल में प्रामाण्य का निश्चय नहीं होता । अतः प्रामाण्यनिश्रय के रहते अप्रामाण्यसंशय की उत्पत्ति प्रामाणिक न होने से उस की उपपत्ति के लिये अप्रामाण्यग्रह के प्रति प्रामाण्यनिश्चय की प्रतिबन्धकता में दोष को उत्तेजक मानना अनावश्यक है। इस विचार से प्रामाण्य के स्वतस्तव परतस्त्व के सम्बन्ध में जैन दर्शन की यह दृष्टि स्पष्ट होती है कि प्रामाण्य की शप्ति में प्रकान्तरूप से मीमांसकों के समान न स्वतस्त्व ही है और न नैयायिकों के समान परतस्त्व दी है क्योंकि अभ्यस्त अर्थ को ग्रहण करनेवाले ज्ञान का प्रामाण्य स्वतोप्राय है और अनभ्यस्त अर्थ के ज्ञान का प्रामाण्य परतोग्राम है ।
इसीलिये जैनदर्शन की यह महनीय मान्यता है कि जहां ज्ञानांश में प्रामाण्य की ग्राहिका सामग्री, ज्ञान के उत्पादक क्षयोपशम की सामग्री में अन्तःप्रविष्ट होती है वहाँ ज्ञानग्रह के साथ स्थांश में प्रामाण्यग्रह सदा होता ही है. इसीलिये कहीं भी ज्ञानांश में प्रमाण- अप्रमाण