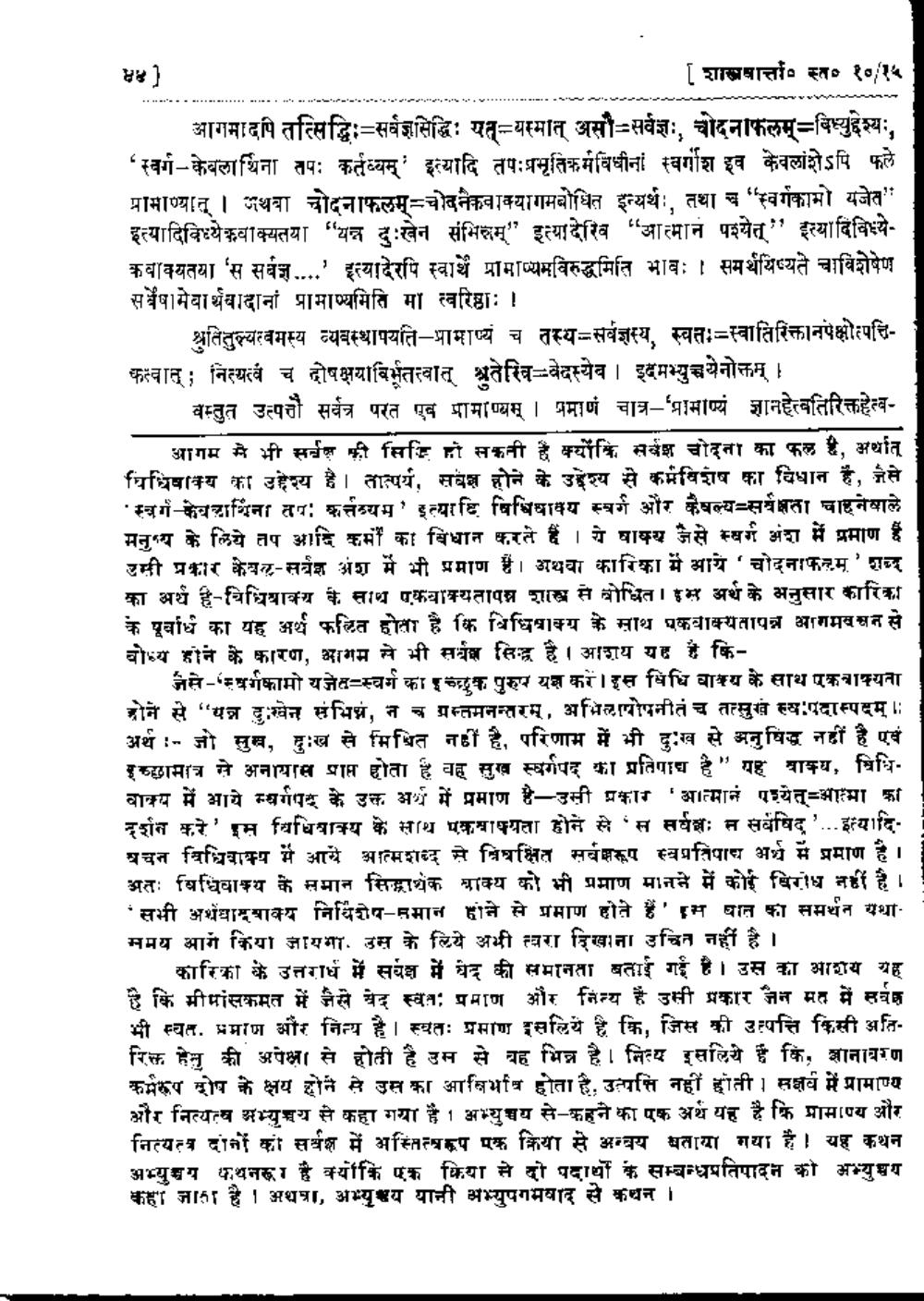________________
[ शास्त्रषार्त्ताः स्त० १०/१५
आगमादपि तत्सिद्धिः=सर्वज्ञसिद्धिः यत् = यस्मात् असौ = सर्वज्ञः, चोदना फलम् = विष्युद्देश्यः, 'स्वर्ग - केबलार्थिना तपः कर्तव्यम् इत्यादि तपःप्रभृतिकर्मविधीनां स्वर्गेश इव केवलांशेऽपि फले प्रामाण्यात् । अथवा चोदना फलम् = चोदनैकवाक्यागमबोधित इत्यर्थः तथा च "स्वर्गकामो यजेत" इत्यादिविध्येकवाक्यतया "यन्त्र दुःखेन संभिलम्" इत्यादेखि "आत्मानं पश्येत्" इत्यादिविध्येकवाक्यतया 'स सर्वज्ञ....' इत्यादेरपि स्वार्थे प्रामाप्यमविरुद्धमिति भावः । समर्थयिष्यते चाविशेषेण सर्वेषामेवार्थवादानां प्रामाण्यमिति मा त्वरिष्ठाः ।
श्रुतितुल्यत्वमस्य व्यवस्थापयति - प्रामाण्यं च तस्य सर्वज्ञस्य स्वतः = स्वातिरिक्तानपेक्षीत्पत्तिकत्वात् नित्यत्वं च दोषश्रयाविर्भूतत्वात् श्रुतेखि वेदस्येव । इदमभ्युच्चयेनोक्तम् ।
वस्तुत उत्पतौ सर्वत्र परत एव प्रामाण्यम् । प्रमाणं चात्र - 'प्रामाण्यं ज्ञानहेत्वतिरिक्तहेत्व
४४ ]
>
आगम से भी सर्व की सिद्धि हो सकती हैं क्योंकि सर्वेश चोदना का फल है, अर्थात् विधिवाक्य का उद्देश्य है। तात्पर्य, संदेश होने के उद्देश्य से कर्मविशेष का विधान है, जैसे 'स्वर्ग केवलार्थिना तपः कर्त्तव्यम' इत्यादि विधिवाक्य स्वर्ग और कैवल्य= सर्वेक्षता चाहनेवाले मनुष्य के लिये तप आदि कर्मों का विधान करते हैं। ये वाक्य जैसे स्वर्ग अंश में प्रमाण हैं। उसी प्रकार केवल- सर्वश अंश में भी प्रमाण है। अथवा कारिका में आयें ' चोदनाफल्म ' शब्द का अर्थ है - विधिवाक्य के साथ पकवाक्यतापत्र शाख से बोधित। इस अर्थ के अनुसार कारिका के पूर्वार्ध का यह अर्थ फलित होता है कि विधिवाक्य के साथ घकवाक्यतापत्र आगमवचन से बोध्य होने के कारण, आगम से भी सर्व सिद्ध है । आशय यह है कि
जैसे- 'स्वर्गकामो यजेत - स्वर्ग का इच्छुक पुरुष यश करें। इस विधि वाक्य के साथ पकवाक्यता होने से "पन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम् अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं रूपःपदास्पदम् ॥ अर्थ :- जो सुख, दुःख से मिश्रित नहीं है, परिणाम में भी दुःख से अनुषिद्ध नहीं है एवं इच्छामात्र से अनायास प्राप्त होता है वह सुख स्वर्गपद का प्रतिपाद्य है " यह वाक्य, विधिवाक्य में आये स्वर्गपद के उक्त अर्थ में प्रमाण है-उसी प्रकार 'आत्मानं पश्येत्=आत्मा का दर्शन करे इस विधिवाक्य के साथ पकवापता होने से 'स सर्वज्ञः स सर्वविद्' इत्यादि. वचन विधिवाक्य में आये आत्मशब्द से विवक्षित सर्वशरूप स्वप्रतिपाद्य अर्थ में प्रमाण है । अतः विधिवाक्य के समान सिद्धार्थक वाक्य को भी प्रमाण मानने में कोई विरोध नहीं है। • सभी अर्थवादवाक्य निर्विशेष-समान होने से प्रमाण होते हैं इस बात का समर्थन यथासमय आगे किया जायगा. उस के लिये अभी त्वरा दिखाना उचित नहीं है ।
कारिका उत्तरार्ध में सर्वश वेद की समानता बताई गई है। उस का आशय यह है कि मीमांसकमत में जैसे वेद स्वतः प्रमाण और नित्य है उसी प्रकार जैन मत में सर्वश भी स्वत प्रमाण और नित्य है । स्वतः प्रमाण इसलिये है कि, जिस की उत्पत्ति किसी अतिरिक हेतु की अपेक्षा से होती है उस से वह भिन्न है। नित्य इसलिये है कि, ज्ञानावरण कर्मरूप शेष के क्षय होने से उस का आविर्भाव होता है, उत्पत्ति नहीं होती । सशर्व में प्रामाण्य और नित्यत्व अभ्युच्चय से कहा गया है । अभ्युच्चय से कहने का एक अर्थ यह है कि प्रामाण्य और नित्यत्व दोनों को सर्वक्ष में अस्तित्वरूप एक क्रिया से अन्वय बताया गया है। यह कथन अभ्युच्चय कथन है क्योंकि एक क्रिया से दो पदार्थों के सम्बन्धपतिपादन को अभ्युच्चय कहा जाता है । अथत्रा, अभ्युश्चय यानी अभ्युपगमवाद से कथन |